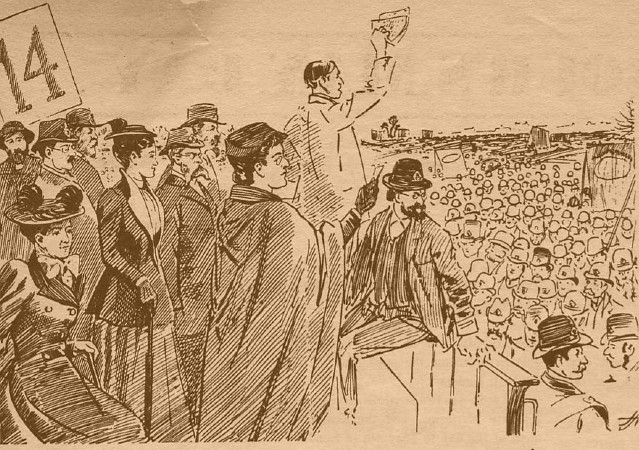पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस- 5) के आंकड़े पिछले दिसंबर में जारी हुए, तो उनसे एक बेहद चिंताजनक तथ्य सामने आया। 2015 से 2019 के बीच दशकों में ऐसा पहली बार ऐसा हुआ कि देश में शारीरिक रूप से अविकसित बच्चों की संख्या बढ़ गई। यानी सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि बाल कुपोषण बढ़ गया। ये ट्रेंड 17 (जिन राज्यों में ये सर्वे हुआ) में से 11 राज्यों में देखा गया। जिन राज्यों में ये हालत बिगड़ी, उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, और केरल जैसे राज्य भी हैं, जिन्हें आम तौर पर अधिक विकसित माना जाता है।
ये स्थिति क्यों हुई? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पूर्व प्रमुख आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने अपने एक विश्लेषण में इसके लिए मोदी सरकार की ‘न्यू वेल्फेयरिज्म’ नीति को जिम्मेदार ठहराया। ये नीति बिल्कुल नई है या नहीं, यह बहस का विषय है। लेकिन ये नीति देश को कहां ले जा रही है, अब इसमें कोई शक नहीं बचा है। तो आखिर क्या है ये ‘न्यू वेल्फेयरिज्म’ की नीति? अरविंद सुब्रह्मण्यम के मुताबिक पुनर्वितरण (redistribution) और समावेशन (inclusion) के प्रति यह एक बिल्कुल खास नजरिया है। इसके तहत बुनियादी स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा जैसे सार्वजनिक कल्याण के क्षेत्रों को अहमियत नहीं दी जाती, जैसाकि पहले किया जाता था। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा के तंत्र को मजबूत करने में सरकार दिलचस्पी नहीं लेती। इसके बदले इसमें वस्तुओं और सेवाओं को सीधे लाभार्थी को दे दिया जाता है। मसलन, पहले जो सब्सिडी कृषि इनपुट के उत्पादन के लिए दी जाती थी, वह अब सीधे किसानों के बैंक खाते में डाल दी जाती है। इसी तरह रसोई गैस, बिजली, मकान, शौचालय आदि लोगों को सीधे उपलब्ध करवाए जाते हैँ।
सुब्रह्मण्यम ने लिखा- न्यू वेल्फेयरिज्म के पीछे गणना यह है कि मतदाताओं को सीधे वस्तु या सेवाएं देने से उच्च राजनीतिक लाभ प्राप्त होता है। इसके तहत मिला लाभ सामने होता है, जिसे लोग देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा जैसी जो सेवाएं सरकारें परंपरागत रूप से देती थीं, वह साकार रूप में व्यक्ति के सामने मौजूद नहीं दिखती थीं। उन्हें परिभाषित करना और उन्हें मापना आसान नहीं था। लेकिन अगर सरकार शौचालय देने का वादा कर रही है, तो उसे आप देख सकते हैं कि वह बन रहा है या नहीं। सुब्रह्मण्यम ने कहा कि ये नया वेल्फेयरिज्म एक साथ दक्षिणपंथ की अस्मिता की राजनीति को संतुलित करता है, मध्य मार्ग के बाजार सुधार को गले लगाता दिखता है, और वामपंथ की पुनर्वितरण (redistributive) अर्थव्यवस्था का नुमाइंदा बना दिखता है।
जाहिर है, न्यू वेल्फेयरिज्म से वोट मिलते हैं। लेकिन ये सियासी कामयाबी देश में सामाजिक सुरक्षा के तंत्र के कमजोर होने और दीर्घकालिक विकास के लिए जरूरी निवेश के धीरे-धीरे खत्म होते जाने की शर्त पर होता है। अगर परिवारों की अपनी आमदनी नहीं बढ़ेगी, बुनियादी स्वास्थ्य में निवेश नहीं होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) को क्रमिक ढंग से खत्म किया जाएगा, आंगनबाड़ी जैसी योजनाएं कमजोर होंगी, मिड-डे मील का सिस्टम प्राथमिकता में नहीं रहेगा, तो कुपोषण बढ़ना उसका स्वाभाविक परिणाम है। लेकिन ये मुमकिन है कि जिनके बच्चे कुपोषण से नए सिरे से ग्रस्त हुए, उनके हाथ में कोई प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ पहुंचा हो। और इसलिए ये संभव है वे उसी पार्टी को फिर से वोट दें, जिसकी नीतियों की वजह से कुपोषण बढ़ रहा है। इसी तरह संभव है कि कृषि का पूरा तंत्र बर्बाद होने और उर्वरक एवं डीजल जैसे अहम कृषि इनपुट की लगातार महंगाई के बावजूद बहुत से किसानों को अपने खाते में पहुंची ‘सम्मान निधि’ की रकम ज्यादा लुभावनी लगे।
बेशक, न्यू वेल्फेयरिज्म की ये नीति मोदी सरकार के दौर में सर्व-प्रमुख बन गई है। इसलिए इसके नतीजे अब और तेजी से सामने आ रहे हैं। फिर भी ये सवाल अपनी जगह प्रासंगिक है कि क्या सचमुच इस नीति के लिए पूरी तरह मोदी सरकार ही जिम्मेदार है? पिछले तीन दशकों से देश जिस दिशा में चला और उस दौरान बुनियादी ढांचा जिस तरह सरकारों की प्राथमिकता से हटता गया, उससे वाकिफ लोगों के लिए पूरी जवाबदेही मोदी सरकार पर डालना शायद संभव नहीं होगा। पीडीएस, सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से सरकारों के हटाने का क्रम 1991 में अपनाई गई नव-उदारवादी नीति के साथ शुरू हो गया था। ‘government has no business to be in business’ (कारोबार में दखल सरकारों का काम नहीं है) जैसे जुमले भी नरेंद्र मोदी का आविष्कार नहीं हैं। अब सिर्फ इतनी बात है कि मोदी सरकार ने ऐसे जुमलों को खुलेआम कार्यरूप देना शुरू कर दिया है। वह पहले अपनाई गई दिशा पर बेहिचक अब बेहद तेज रफ्तार से दौड़ रही है।
क्या यह हैरतअंगेज नहीं है कि इस नीति के दुष्परिणाम सामने होने के बावजूद भारत के पूरे सियासी फलक में इसकी ठोस आलोचना और उचित विकल्प पेश करने की कोई कोशिश होती नहीं दिखती। बल्कि प्रत्यक्ष लाभ देकर से वोट पाने का लालच ऐसा है कि उस दिशा में ही लगभग तमाम पार्टियां दौड़ती नजर आ रही हैँ।
केरल को भारत का सबसे प्रगतिशील राज्य कहा जाता है। कभी यहां अपनाए गए विकास मॉडल की खूब तारीफ होती थी। मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के विमर्श में अक्सर आई ‘केरल मॉडल’ की चर्चा ने इसे दुनिया भर में चर्चित किया था। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख मोर्चों- लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के चुनाव घोषणापत्रों में समाज के अलग- अलग तबकों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ पहुंचाने के वायदों की होड़ लगी दिखती है। इस ‘मॉडल’ के टिकाऊ होने पर शक जताते हुए हाल में मशहूर अर्थशास्त्री पुलापरे बालाकृष्णन ने ध्यान दिलाया कि देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति सार्वजनिक कर्ज केरल पर ही है। जाहिर है, इन वादों को पूरा करने पर केरल के ऊपर पहले से ही चढ़े कर्ज के बोझ और बढ़ जाएगा।
बालाकृष्णन ने लिखा है- ‘वास्तविक कल्याणकारी राज्य और मौजूदा केरल मॉडल के बीच फर्क यह है कि वास्तविक कल्याणकारी में जो लाभ दिए जाते हैं, उसके लिए धन टैक्स के जरिए जुटाया जाता है। कल्याणकारी राज्य के ढांचे में दो बातें अहम हैं। पहला मुद्दा वित्तीय रूप से संभव होने का है। दूसरा कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर लोगों में स्वामित्व का भाव उत्पन्न करना है (यानी उन्हें लगना चाहिए कि ये कार्यक्रम खुद उनके हैं)। भाव यह नहीं होना चाहिए कि कल्याणकारी राज्य खैरात बांटने वाला संस्थान है, बल्कि यह होना चाहिए कि इसे खुद लोगों ने अपने लिए खड़ा किया है।’ बालाकृष्णन ने वास्तविक कल्याण कार्यक्रम के रूप में ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) का जिक्र किया। एनएचएस की स्थापना 1950 के दशक में तत्कालीन लेबर पार्टी सरकार ने की थी। इसे चलाने के लिए नागरिकों पर टैक्स लगाया गया। बालाकृष्णन ने ध्यान दिलाया है कि ब्रिटेन आज भी उन देशों में है, जहां इनकम टैक्स रेट सबसे ज्यादा है।
तो एक बात जो यहां अहम है, वो ये है कि सरकारों का सिर्फ वही सामाजिक निवेश टिकाऊ हो सकता है, जिनसे भविष्य में संसाधन उत्पन्न होने और सरकार की कर आमदनी बढ़ने की संभावना हो। जबकि सीधे नकदी दी गई सहायता अक्सर ऐसे उपभोग में खर्च होती है, जिससे सामाजिक संपत्ति तो दूर खुद लाभान्वित परिवारों के लिए भी कोई दीर्घकालिक संपत्ति खड़ी नहीं हो पाती। सरकारों की आमदनी का स्रोत मुख्य रूप से टैक्स और कर्ज ही हैं। न्यू वेल्फेरियज्म का नतीजा यह हुआ है कि राज्यों और अब केंद्र पर भी कर्ज का बोझ बेहद बढ़ गया है। ये ऐसा कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए वेल्फेयरिज्म पर खर्च हुए धन से भविष्य में कोई संसाधन नहीं आएगा। टैक्स आमदनी के एक न्यूनतम स्तर को बरकरार रखने के लिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर भी पेट्रोलियम पदार्थों पर अनुचित कर लगाए गए हैँ। इसके अलावा राज्य सरकारें शराब, लॉटरी आदि जैसे धंधों पर कर लगाकर पैसा जुटा रही हैं। चूंकि उस धन से सामाजिक सुरक्षा के तंत्र नहीं खड़े किए जा रहे हैं, अतः उसका नतीजा यह है कि अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ और कुशल कर्मी तैयार नहीं हो रहे हैं।
ध्यान देने की बात है कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अधिक से अधिक प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, तो उनका महंगा होना लाजिमी है। ऐसे में इन दोनों उद्देश्यों के लिए परिवारों के कर्ज में डूबने की स्थिति लगातार मजबूत होती है। दूसरी तरफ कर्ज लेकर की गई पढ़ाई के बाद अगर नौकरी मिल भी जाए, लेकिन इलाज की सार्वजनिक गारंटी ना हो, तो फिर नौकरीशुदा व्यक्ति के परिवार के पास उपभोग पर खर्च करने के सीमित संसाधन ही बचते हैँ। इससे बाजार में मांग नहीं बढ़ती। तो निजी क्षेत्र के निवेश के लिए अनुकूल माहौल नहीं बनता है। असर यह होता है कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था निम्न वृद्धि दर का शिकार बनी रहती है। इसका परिणाम एक बार फिर सरकार की आमदनी घटने के रूप में सामने आता है। यानी कुल मिला कर यह एक दुश्चक्र है।
यहां ये तथ्य उल्लेखनीय है कि भारत (दरअसल, नव-उदारवाद की अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले अन्य देशों में भी) आर्थिक विकास दर की जो दर दिखती है, उसमें आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा वह है, जो जायदाद, शेयर बाजार, बॉन्ड आदि में निवेश से कमाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक हिस्सा जायदाद से प्राप्त होने वाले रेंट का है। ये तमाम आमदनियां जीडीपी में झलकती हैं, लेकिन इनसे असल अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं होता। इसी ट्रेंड के कारण हाल के वर्षों में दलाल स्ट्रीट (अमेरिका में वॉल स्ट्रीट) बनाम मेन स्ट्रीट की बहस खड़ी हुई है। इसका परिणाम समाज में लगातार आर्थिक गैर-बराबरी बढ़ने के रूप में सामने आ रहा है। दलाल स्ट्रीट से जुड़े लोगों की संपत्ति घातीय (exponential) ढंग से बढ़ रही है, जबकि आम इनसान के लिए रोजमर्रा की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी देश के धनी लोगों की संपत्ति और बढ़ जाने का भी यही राज है। असल में उपरोक्त स्थितियों के रहते सरकार बाजार में नकदी बढ़ाने के जो भी उपाय घोषित करेगी, उसका परिणाम यही होगा। ये बात पहले भी देखने को मिली थी, जब यूपीए की सरकार के दौरान देश ने उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल की थी। लेकिन तब भी उस वृद्धि दर से उसी अनुपात में रोजगार के अवसर पैदा नही हुए। इसलिए तब जॉबलेस ग्रोथ की अवधारणा सामने आई थी।
इस समस्या का समाधान क्या है? फिलहाल, हम दीर्घकालिक और पूर्ण समाधान की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हालात बिल्कुल ही उलटे हों, तो उस समय ऐसी बातों को दिवास्वप्न के अलावा कुछ और नहीं कहा जाएगा। लेकिन बात जहां से शुरू हो सकती है, वो यह है कि अर्थव्यवस्था में सरकार की वापसी को एक मूलभूत एजेंडा बनाया जाए। पिछले पांच साल में अगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में चली बहस पर गौर करें, तो वहां ऐसा होने की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर है, बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन अब वहां बने ताजा हालात के बीच ‘government has no business to be in business’ जैसी बातों को वो नेता भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो अतीत में इस सोच के वाहक रहे हैँ।
इस अंतर्विरोध पर गौर कीजिए। 1980 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ‘Minimum Government’ के नारे पर विजयी हुए रोनॉल्ड रेगन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में एक और जुमला उछाला। उन्होंने कहा था- “आज के संकट के बीच, सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि सरकार ही समस्या है।”
आज के अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन तब अमेरिकी सीनेट के सदस्य थे। रेगन ने उस समय जो कहा, आगे चल कर वह न सिर्फ अमेरिका, बल्कि पूरी गैर-कम्युनिस्ट दुनिया का आर्थिक दर्शन बन गया। रेगन प्रशासन ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए बजट में कटौती, धनी तबकों के लिए टैक्स दरें घटाने और धीरे- धीरे राज्य के अंगों और एजेंसियों के निजीकरण की जो शुरुआत की, वो उस आर्थिक सोच की बुनियाद बनी, जिसे ‘वॉशिगंटन कॉन्सेंसस’ यानी वॉशिंगटन आम-सहमति के नाम से जाना गया। अमेरिका में उसके बाद सत्ता में चाहे रिपब्लिकन पार्टी रही हो, या डेमोक्रेटिक पार्टी- उसकी सरकार उसी आर्थिक दर्शन पर चली। जो बाइडेन इसी दौर की व्यवस्था से (ऐस्टैबलिशमेंट) नियंत्रित राजनेता रहे हैं।
लेकिन रेगन की सोच का असर यह हुआ कि अमेरिका में गैर-बराबरी बढ़ी, मध्य वर्ग संकुचित हुआ, और कुल मिलाकर ऐसे आर्थिक हालात बने जिससे 2010 का दशक आते- आते अपनी सरकार संचालित अर्थव्यवस्था की बदौलत चीन उससे आगे निकल जाने को तैयार हो गया। डॉनल्ड ट्रंप की परिघटना को भी इसी का नतीजा समझा जाता है, जिससे अमेरिकी लोकतंत्र आज खतरे में बताया जा रहा है। इसकी प्रतिक्रिया बर्नी सैंडर्स परिघटना के उदय के रूप में भी देखने को मिली है। ट्रंप और सैंडर्स की परिघटनाओं ने वहां के विमर्श को काफी हद तक बदल दिया है।
इसकी झलक देखनी हो, राष्ट्रपति बाइडेन की एक हालिया टिप्पणी पर गौर करना चाहिए। बाइडेन ने कहा- ‘हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि सरकार किसी दूर राजधानी में बैठी कोई विदेश ताकत नहीं है। हम ही, हम सब, हम अमेरिका के लोग ही असल में सरकार हैं।’ और इसी सोच के तहत हाल में बाइडेन प्रशासन ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर का कोरोना राहत पैकेज पारित किया, जिसमें 80 फीसदी रकम 20 फीसदी सबसे गरीब आबादी को नकद और स्वास्थ्य सहायता के रूप में मुहैया कराई गई है। उसके बाद अब बाइडेन तीन ट्रिलियन डॉलर का इन्फ्रास्ट्रक्चर और फैमिली हेल्फ पैकेज घोषित करने वाले हैं, जिससे मुफ्त शिक्षा देने वाले कॉलेजों का निर्माण, सभी बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह के साथ अवकाश और बच्चों के पालन-पोषण की सार्वजनिक व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए धन कॉरपोरेट सेक्टर और धनी लोगों पर नए टैक्स लगाकर जुटाया जाएगा।
तो ये साफ है कि भारत 1991 में जिस ‘आम सहमति’ का हिस्सा बना था, वह बुरे अनुभवों के बाद अब अपने गढ़ में ही टूट चुकी है। बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। कोरोना महामारी के दौर में ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने भी राजकोष से जितनी उदारता से बड़े पैमाने पर खर्च किया है, उसके बाद राजकोषीय अनुशासन और किफायत (ऑस्टेरिटी) की नीतियां फिलहाल तो कहीं पीछे छूट गई हैँ। इसके मद्देनजर इसे विडंबना ही कहेंगे, जिस समय ये ‘आम सहमति’ टूटी है, उसी समय भारत में मोदी सरकार ने उसे लागू करने की गति और तेज कर दी है। इसके आधार पर यह तो बेहिचक कहा जा सकता है कि ये सरकार या तो अर्थ नीति को समझने में बिल्कुल नाकाबिल है, या फिर उसे भारत के आम जन के हितों की कोई परवाह नहीं है। बहरहाल, चूंकि अभी तक उसका सांप्रदायिक- क्रोनी पूंजीवाद मॉडल चुनावी रूप से कारगर है, इसलिए उससे इस मामले में किसी बहस की संभावना नहीं है।
मगर जो पार्टियां इस कम्युनल- क्रोनी पॉलिटिकल इकॉनोमी का विकल्प खड़ा करना चाहती हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था में सरकार की वापसी को जरूर अपने एजेंडे पर लाना चाहिए। पिछले 30 साल में न्यू वेल्फेरियज्म की नीति से हुए नुकसान अब दुनिया के सामने हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी अगर वोट के फौरी फायदे के लिए इस नीति के तहत बढ़-चढ़ के वादे करती रहीं, तो उससे मुमकिन है कि उन्हें भी कभी लाभ हो जाए। लेकिन उससे देश की जनता का कोई दीर्घकालिक फायदा नहीं होगा। हालांकि जिस तरह मोदी सरकार ने न्यू वेल्फेयरिज्म को हड़प लिया है, उसके बाद बाकी पार्टियां इस होड़ में भी टिक सकेंगी, इसकी संभावना कम ही है। इसलिए उनके अपने भविष्य के लिए भी जरूरी है कि वे नई शुरुआत करें। वे अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका, नियोजित विकास, पब्लिक सेक्टर केंद्रित अर्थ नीति में अपनी आस्था और मौका मिलने पर उस दिशा में देश को ले जाने का संकल्प जताएं। वरना, वे आरएसएस-बीजेपी के पिच पर खेलने और उस पर लगातार पराजित होने के लिए अभिशप्त बनी रहेंगी।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।