
 जब उम्मीद डूबने लगती है तभी कोई हाथ ग़ैब से सहारा बन जाता है और देश जी जाता है.
जब उम्मीद डूबने लगती है तभी कोई हाथ ग़ैब से सहारा बन जाता है और देश जी जाता है.
पिछले हफ्ते लोकसभा टीवी पर मदरसों के निसाब पर एक डिस्कशन में मैंने एंकर मनोज जी को जवाब देते हुए कहा था की “उर्दू ज़बान का सवाल मदरसों से नत्थी न कीजिये. बल्कि मदरसों को उर्दू का मुहाफ़िज़ न बनने दीजिये. क्यूंकि उर्दू उस अदब के लिए जानी जाती है जिसने बड़े आस्तानों से बग़ावत करने का फ़लसफ़ा और एक्सप्रेशन दिया, चाहे ख़ुदा की ज़ात हो या ख़ुदा के ठेकेदारों की, चाहें हुकूमत का आस्ताना हो या समाज के ठेकेदारों का, उर्दू ने सबसे बग़ावत को इज़हार की ताक़त दी है. उर्दू में इक़बाल ने अल्लाह से शिकवा किया है और ग़ालिब ने ज़ाहिद को किनारे लगाया है, अँगरेज़ से लेकर देसी हुक्मरानो से जवाब तलब करने के लिए उर्दू ने सबसे अच्छे अशआर और नारे दिए हैं. सरमायादारी से दो दो हाथ करने के लिए भारत में उर्दू पहली देसी ज़बान थी जिसने दौर-ए -जंग-ए-आज़ादी एक पूरी तहरीक को संभाला. 1857 की बग़ावत का तसव्वुर उर्दू के बिना किया ही नहीं जा सकता था.
ये अफ़सोस की बात है की भारत में आज इदारे के तौर पर मज़हबी मदरसे ही उर्दू के मुहाफ़िज़ बन के रह गए हैं क्यूंकि हुकूमत-ए-वक़्त ने उर्दू को लावारिस कर दिया. इसलिए सेक्युलर स्कूलों से उर्दू को विषय के तौर पर बेदख़ल किया गया तो तालीम के माध्यम के तौर पर उर्दू मदरसों में क़ैद हो गयी. लेकिन अंग्रेज़ी स्कूलों से पढ़ के, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी, और लॉ से रोज़गार पाने के बाद उर्दू के आशिक़ीन अब उर्दू पर खर्च कर रहे हैं. हुकूमत की साज़िश को नाकाम करते हुए भारत के ग़ैर मुस्लिम नौजवान अपने सांझा विरसे की हिफ़ाज़त कर रहे हैं.
ग़ालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढा कर ग़ालिब पे करम क्यों है’

लेकिन अब हालात वो नहीं रहे जो साहिर के वक़्त में थे, भले ही सरकार और सियासत कहती रहे की ‘उर्दू आतंकवादियों की ज़बान है’, लेकिन इस देश का नौजवान आईटी, लॉ, मैनेजमेंट में कमा रहा है और उर्दू पर लगा रहा है. किसी भी उर्दूदां को अब उर्दू की फ़िक्र करने की ज़रुरत नहीं है क्यूंकि उर्दू के परस्तारों ने अब हाथ लगा दिया है और इस खूबसूरत असासे को संभल लिया है. बंटवारे और नफरत की सियासत ने तमाम कोशिश की कि उर्दू की पहचान ‘मुसलमानो की और पाकिस्तान की ज़बान’ बना दी जाए लेकिन उर्दू अपनी लसानी ताक़त से नौजवानो के दिलों में हुकूमत कर रही है. सलामत रहें मेरे देश के अदब परवरदा जिन्होंने बिना शोर किये अपने जंगा-जमुनी खूबसूरत विरसे पर हक़ का दावा कर दिया.
इस वक़्त देश के बड़े बड़े शहरों में तमाम महफ़िलें, जश्न, दास्तानगोई और दीगर तक़रीबात मुरत्तब की जा रही हैं जो उर्दू में महफूज़ सांझी विरासत का जश्न मना रही हैं. दास्तानगोई जैसी लापता सिन्फ़ को दोबारा ज़िंदा कर दिया गया है. तमाम शोरा- पंकज परवेज़, अशोक कुमार पांडेय, अभिषेक शुक्ल, संदीप शजर, विपुल कुमार, हिमांशु वाजपेयी, मीनाक्षी जिजीविषा, सौम्या कुलश्रेष्ठ, दास्तानगो- राणा प्रताप सेंगर, राजेश कुमार, अंकित चढ्ढा, सुनील मेहरा, पूनम गिरधानी, मयंक यादव वगैरह अपने अदबी विरसे में चार चाँद लगा रहे हैं. उधर फ़िल्मी दुनिया में भी नए गीतकार उम्दा लिख रहे हैं और उर्दू को मॉडर्न सेटअप में फैशनएबेल बनाए हैं. इनके अलावा ‘उर्दू कलचर’ जिसमे ज़बान के साथ साथ उर्दू दुनिया के आदाब, गायकी, पहनावे, खाने, इमारतें, और मुसव्विरि शामिल है अब अख़बारों, न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया और टूरिस्म की दुनिया के अटूट हिस्से हैं. उत्तर भारत में उर्दू हेरिटेज एक नया बाज़ार बन चुका है.

मेरी नज़र में इंटरनेट के तमाम फायदों में सबसे बड़ा सामाजिक फ़ायदा आज की तारीख़ में यही होगा की देश बेहिचक जुड़ रहा है. फेसबुक का मजमा अब इंडिया गेट, लोधी गार्डन, आई आई सी, हैबिटैट सेंटर और आईजीएनसीए, लामकान, रविंद्र भवन के आँगन में उतर आया है. जश्न-ए-रेख़्ता, जश्न-ए-इश्क़ा, जश्न-ए-विरासत, गुफ़्तुगू, महफ़िल, सुख़नवर-ए-शायरी, लफ़्ज़ों का सफ़र, पोएट्स कलेक्टिव, आफ़रीन, महफ़िल-ए-अज़ादारी जैसे आयोजन दस साल पहले कहाँ थे? आज जॉन एलिया नौजवानों की ज़ुबान पर रवां-दवां हैं. फैज़ तो ख़ैर इस सदी के शायर तय पाए गए हैं. आज तमाम इदारे उर्दू स्क्रिप्ट सिखाने का कोर्स चला रहे हैं क्यूंकि हुकूमत ने उनको अपने प्राइमरी के निसाब में उर्दू से महरूम कर दिया।
पिछले दौर में उर्दू उन पर मनहसर थी जो इसी की कमाई खाते थे. अब उर्दू उनके पास पहुंची है जो अपनी कमाई उर्दू पर लगाते हैं. हिन्द के नौजवानों आपकी कोशिशों को सलाम, उर्दू का दौर-ए-आफ़रीँ आप सबको मुबारक।
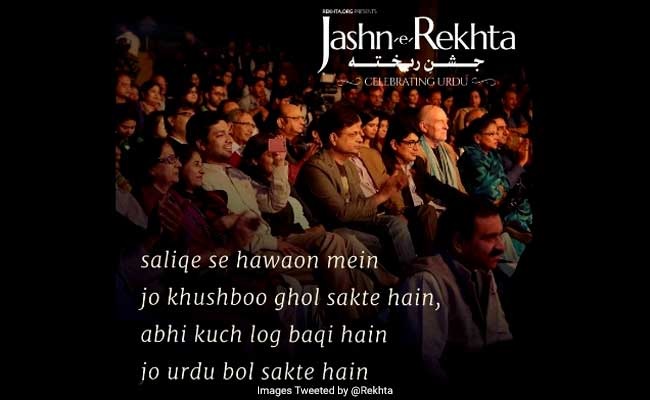
पुनश्च : साहिर लुधियानवी की वो मशहूर नज़्म पेश है जिसकी रौशनी में आपको गुज़रे वक़्त के अंधेरों का अंदाज़ा हो जाएगा
तब जाके कहीं हम को ग़ालिब का ख़्याल आया ।
तुर्बत है कहाँ उसकी, मसकन था कहाँ उसका,
अब अपने सुख़न परवर ज़हनों में सवाल आया ।
-
- सौ साल से जो तुर्बत चादर को तरसती थी,
-
- अब उस पे अक़ीदत के फूलों की नुमाइश है ।
-
- उर्दू के ताल्लुक से कुछ भेद नहीं खुलता,
-
- यह जश्न, यह हंगामा, ख़िदमत है कि साज़िश है ।
जिन शहरों में गुज़री थी, ग़ालिब की नवा बरसों,
उन शहरों में अब उर्दू बे नाम-ओ-निशां ठहरी ।
आज़ादी-ए-कामिल का ऎलान हुआ जिस दिन,
मातूब ज़ुबां ठहरी, गद्दार ज़ुबां ठहरी ।
-
- जिस अहद-ए-सियासत ने यह ज़िन्दा ज़ुबां कुचली,
-
- उस अहद-ए-सियासत को मरहूमों का ग़म क्यों है ।
-
- ग़ालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था,
-
- उर्दू पे सितम ढा कर ग़ालिब पे करम क्यों है ।
ये जश्न ये हंगामे, दिलचस्प खिलौने हैं,
कुछ लोगों की कोशिश है, कुछ लोग बहल जाएँ ।
जो वादा-ए-फ़रदा, पर अब टल नहीं सकते हैं,
मुमकिन है कि कुछ अर्सा, इस जश्न पर टल जाएँ ।
-
- यह जश्न मुबारक हो, पर यह भी सदाकत है,
-
- हम लोग हक़ीकत के अहसास से आरी हैं ।
-
- गांधी हो कि ग़ालिब हो, इन्साफ़ की नज़रों में,
-
- हम दोनों के क़ातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं ।
-
–साहिर लुधियानवी
































