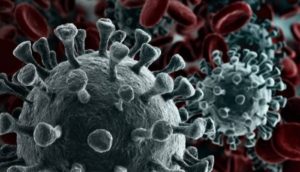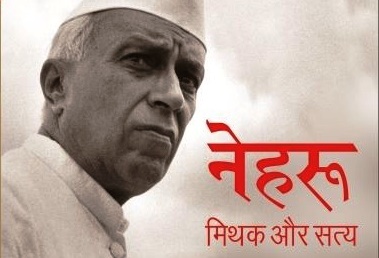
‘‘सीमा पार के हमारे विरोधी कह रहे हैं कि यह हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है. हम कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की मदद करने के लिए वहां गए हैं, कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी हमारे साथ नहीं है. इससे ज्यादा सफेद झूठ और क्या हो सकता है. हम वहां कश्मीर के महाराजा के न्योते पर भी नहीं जाते, अगर उस न्योते को वहां की जनता के नेताओं की सहमति हासिल नहीं होती. मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सेनाओं ने वहां अदम्य बहादुरी का परिचय दिया है, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी सेनाओं को कामयाबी नहीं मिली होती,अगर उन्हें कश्मीर के लोगों की मदद और सहयोग न मिलता.’’
जवाहरलाल नेहरू, मार्च 1948, संविधान सभा में
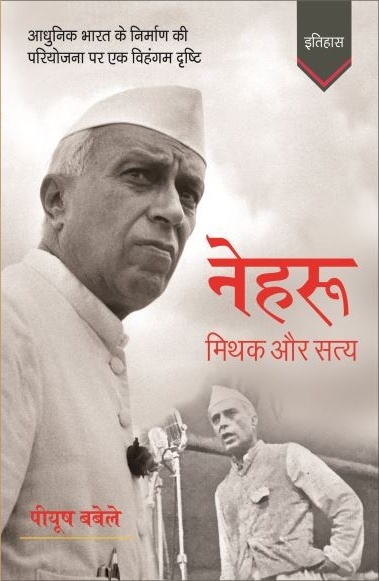
कश्मीर की भौगोलिक परिस्थिति और शेख अब्दुल्ला से दोस्ती
कश्मीर. एक ऐसा मुद्दा, जिसका जिक्र छिड़ते ही नेहरू पर आरोपों की बौछार शुरू हो जाती है. पहला आरोप लगता है कि जब देसी रियासतों के भारत संघ में विलय का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे, तो नेहरू ने कश्मीर का मामला अपने हाथ में क्यों लिया. आरोप के समर्थन में दलील दी जाएगी कि वे कश्मीरी पंडित थे, इसलिए उन्हें कश्मीर से भावनात्मक लगाव था. इसी चक्कर में उन्होंने यह मुद्दा अपने हाथ में लिया और सब गुड़ गोबर कर दिया.
दूसरा आरोप लगता है कि चलो, मुद्दा अपने हाथ में ले भी लिया था तो मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की क्या जरूरत थी. और जनमत संग्रह की बात कहां से ले आए.
तीसरा आरोप लगेगा कि इतना सब करके ही नेहरू को चैन न मिला जो कश्मीर के लिए धारा 370 बना गए.
वैसे सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन नेहरू के आलोचक मुख्यरूप से इन्हीं तीन सवालों के इर्द-गिर्द उन्हें घेरते हैं और बहस के अंत में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कश्मीर की मौजूदा समस्या के लिए संपूर्णरूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार हैं.
इन आरोपों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता. लेकिन इन्हें समझने के लिए बात को शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा. तो बात यहां से शुरू होगी कि आखिर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इस आधार पर हुआ था कि हिंदू बहुल इलाके भारत में रहेंगे और मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो फिर मुस्लिम बहुल कश्मीर आखिर किस तरह भारत में आया होगा. उस समय जबरन किसी राज्य पर कब्जे का सवाल नहीं था, क्योंकि विभाजन की भूमिका अंग्रेजीराज में ही तय हो रही थी और दोनों ही पक्षों को नियम कायदों से बंधना था. भारतीय पक्ष पर नियम कायदों का बंधन इसलिए भी ज्यादा होना था, क्योंकि उसके नेता महात्मा गांधी थे. महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी पूरी लड़ाई नैतिकता के बल पर लड़ी थी, इसलिए भारतीय नेतृत्व के लिए अनैतिकता के साथ खड़ा होना मुश्किल के साथ शर्मनाक भी हो सकता था.
तो मुस्लिमबहुल कश्मीर किस सिद्धांत के तहत भारत में आया. क्या वह इसलिए आया कि वहां के हिंदू राजा हरि सिंह भारत में आना चाहते थे. कुछ लोगों को लगता है कि हां. लेकिन हरि सिंह तो कबायली हमला होने से पहले तक आजादी पर ही अड़े हुए थे. और मान लीजिए कि वे आना चाहते भी तो उन्हें कैसे इसका हक मिल जाता,जबकि उसी समय जूनागढ़ और हैदराबाद के मुस्लिम शासकों की पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा को खारिज कर दिया गया था.
हैदराबाद और जूनागढ़ के शाषकों की मांग इसी आधार पर खारिज की गई थी कि वहां की बहुसंख्यक हिंदू आबादी भारत के साथ रहना चाहती थी. ऐसे में राजा की जगह प्रजा के विचार को ज्यादा महत्व दिया जाना था.
दूसरी तरफ बंगाल और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य थे. इन राज्यों को हिंदू और मुस्लिम आबादी के वजन के हिसाब से दो-दो हिस्सों में बांट दिया गया. मुस्लिम बहुल हिस्सा पाकिस्तान बना और हिंदू बहुल हिस्सा भारत में शामिल हो गया.
तो क्या यह बात कश्मीर में नहीं हो सकती थी. कश्मीर भी तो दोनों देशों के बीच था. यहां भी यह हो सकता था कि हिंदू बहुल जम्मू और बौद्ध बहुल लद्दाख भारत में आ जाते और कश्मीर का इलाका मुस्लिम बहुल होने के कारण पाकिस्तान में चला जाता.
लेकिन विभाजन के समय अपनाए गए ये दोनों नियम जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं हुए. न तो वह पूरा ही पाकिस्तान में गया और न ही उसका मुस्लिम बहुल हिस्सा. और यह सब तब हुआ जब कश्मीर का भारतीय भूभाग से सड़क और रेल संपर्क न के बराबर था, जबकि पाकिस्तानी भूभाग से संपर्क कहीं बेहतर था.
इसके बावजूद पूरा का पूरा कश्मीर भारत के साथ आया, यह बात अलग है कि बाद में पाकिस्तान ने कबायली हमला किया और जबरन कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया. जिसे भारत आज तक मान्यता नहीं देता. लेकिन जम्मू कश्मीर का मुख्य हिस्सा खासकर कश्मीर घाटी भारत में ही बनी रही.
यह कड़वी भूमिका इसलिए सामने रखनी पड़ी, ताकि समझा जा सके कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कश्मीर भारत में ऐसे ही नहीं आ गया, उसे शामिल करने के लिए लंबी कूटनीतिक लड़ाई, लड़ी गई. एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत के विभाजन के दोनों मूल सिद्धांतों को कश्मीर के मामले में बेअसर कर दिया और कश्मीर का भारत में विलय हो गया.
इस कूटनीतिक लड़ाई के चाणक्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के नेतृत्व को पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ खड़ा कर दिखाया. इसीलिए जब कबायली हमले के समय राजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय का समझौता किया, तो ठीक उसी समय कश्मीर की जनता के लोकप्रिय नेता की हैसियत से शेख अब्दुल्ला ने भी भारत में विलय स्वीकार किया और वे कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने. जो काम सांप्रदायिकता के चरम उभार और भौगोलिक परिस्थितियों के चलते सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में नहीं कर सके, यानी वहां के सेकुलर ताने-बाने को नहीं बचा सके, उस काम को कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती ने कर दिखाया.
29 सितंबर 1947 को नेहरू के प्रयासों से कश्मीर के राजा हरि सिंह की जेल से आजाद होने के बाद शेख अब्दुल्ला ने एक भाषण में कहा: “पाकिस्तान के नारे में कभी मेरा विश्वास नहीं रहा. फिर भी आज पाकिस्तान एक वास्तविकता है. मैं भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का अध्यक्ष हूं और उसकी नीति स्पष्ट है. पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे उत्तम मित्र हैं और मुझे गांधीजी के प्रति सच्चा पूज्य भाव है. यह भी सत्य है कि कांग्रेस ने (कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में) हमारे आंदोलन की बड़ी मदद की है, परंतु इन सब बातों के बावजूद मेरा निजी विश्वास दोनों में से किसी एक देश के पक्ष में स्वतंत्र निर्णय करने के मार्ग में बाधक नहीं बनेगा. भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का हमारा चुनाव जम्मू और कश्मीर में रहने वाले 40 लाख लोगों की भलाई पर आधारित होगा और यदि हम पाकिस्तान में मिल गए तो भी हम दो राष्ट्रों के सिद्धांत को नहीं मानेंगे. जिसने इतना अधिक जहर फैलाया है.”
शेख अब्दुल्ला का यह बयान महीन कूटनीति से भरा है. वे यह तो मान रहे हैं कि कश्मीर की जनता को भारत या पाक में से एक को चुनने का अधिकार है. लेकिन साथ ही जाहिर कर रहे हैं कि वे गांधी और नेहरू के साथ हैं. इससे बढ़कर वे कह रहे हैं कि दो राष्ट्रों के सिद्धांत में यकीन नहीं है. जिस आदमी को दो राष्ट्र के सिद्धांत में यकीन ही नहीं है, वह इसी सिद्धांत पर बने पाकिस्तान के साथ कैसे जा सकता है.
कश्मीर को लेकर नेहरू क्या सोच रहे थे
इधर, नेहरू के दिमाग में एक गहरी शतरंज चल रही थी. सरदार पटेल अक्सर कहा करते थे कि नेहरू को देसी मामलों के साथ ही विदेशी मामलों की भी गंभीर समझ है. उनका पूरी दुनिया में मान है. दोनों विषयों पर अच्छी पकड़ के कारण देश का प्रधानमंत्री नेहरू को ही होना चाहिए.
जाहिर है कि पटेल गलत नहीं थे. 1930 के दशक में ही नेहरू की आत्मकथा पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर हो गई थी. उनकी छवि एक ऐसे राजकुमार की बन गई थी, जो गांधी की अहिंसा की लड़ाई में सब कुछ त्यागकर शामिल हुआ था. दुनिया के लगभग सभी प्रमुख नेताओं से उनका सीधा संपर्क था. जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर से उन्हें मिलना नहीं था और इटली के तानाशाह मुसोलिनी के लाख चाहने के बावजूद नेहरू ने उन्हें मिलने के लिए वक्त नहीं दिया था.
नेहरू जिस तरह पूरी दुनिया को समझ रहे थे, उसी तरह उस दुनिया में भारत की भावी स्थिति को भी समझ रहे थे. उन्हें अच्छी तरह पता था कि दुनिया की महाशक्तियों के बीच बिछी बिसात में पाकिस्तान किस तरह का मोहरा हो सकता है. इस बाजी को पलटने के लिए भारत को हर हाल में कश्मीर अपने पास रखना होगा. नेहरू के लिए कश्मीर एक खूबसूरत वादी तो थी ही, लेकिन उससे कहीं बढ़कर दुनिया का महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थल था, जो आगे चलकर दुनिया की राजनीति पर खासा असर डालने वाला था.
इस बात को एक बार उन्होंने संसद में भी समझाया कि कश्मीर उनके लिए भावनात्मक नहीं, रणनीतिक मुद्दा है. 7 अगस्त 1952 को संसद में दिए एक भाषण में उन्होंने कहा:
“मुझे इस संदर्भ में कश्मीरी कहा जाता है कि दस पीढ़ी पहले मेरे पुरखे कश्मीर से उतरकर भारत आ गए थे. लेकिन यह वह बंधन नहीं है, जिसके कारण कश्मीर मेरे दिमाग में आता है. वे दूसरे ही बंधन है, जिन्होंने हमें एक-दूसरे बांध दिया है.”
कश्मीर का यह बंधन अगर भावनात्मक नहीं था तो और क्या था. इसे जानने के लिए जरा उस कहानी को देखते हैं जो 1947 से शुरू हुई. कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसकी सीमा उस उस समय सोवियत संघ, चीन, अफगानिस्तान,पाकिस्तान और भारत जैसे पांच देशों को छूती थी. इसके अलावा सिंक्यांग और तिब्बत से होकर गुजरने वाली 900 मील की सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित नहीं थी. यह रूस और चीन से हिमालय और पामीर के पर्दे से ढका था. कश्मीर कितना महत्वपूर्ण था, इसे दिसंबर 1955 में भारत की यात्रा पर आए सोवियत संघ के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव की इस बात से समझा जा सकता है. ख्रुश्चेव ने कहा था, “आप पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाएं तो आवाज लगाकर हमें बुला सकते हैं.”
यही नहीं कश्मीर घाटी के उत्तर में बाल्टिस्तान है और उसके बाद हुंजा और नागिर के क्षेत्र हैं, जो गिलगित को छूते हैं. इसके दक्षिण में जम्मू है और पूर्व में लद्दाख. इसके पश्चिम में मुजफ्फराबाद, रायसी, पुंछ और मीरपुर जिले हैं.
इसलिए नेहरू के लिए कश्मीर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला नहीं था. कश्मीर की सरहद का रूस,चीन और अफगानिस्तान की सीमाओं को छूना, नेहरू के दिमाग में बराबर चलता रहता था. कश्मीर पर कबायली हमले के एक हफ्ते बाद 2 नवंबर 1947 को राष्ट्र के नाम संदेश में नेहरू ने कहा,
“कश्मीर एक ऐसा ऐसा भूभाग है, जिसकी सीमाएं बड़े देशों को छूती हैं. इसलिए वहां हो रही गतिविधियों में हमें दिलचस्पी दिखानी ही होगी.”
इसके 3 हफ्ते बाद उन्होंने इसी बात को संविधान सभा में दिए गए बयान में और स्पष्टता से रखा. नेहरू ने कहा,
“अपनी भौगोलिक स्थिति और सीमाओं के कारण, जो कि तीन देशों सोवियत संघ, चीन और अफगानिस्तान को छूती हैं, कश्मीर ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत से जुड़ा हुआ है.”
‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ के लेखक को यह भी याद था कि कुछ हफ्ते पहले जिस रास्ते से बर्बर कबायली हमलावर कश्मीर में घुसे थे, सदियों पहले उसी रास्ते से पैदल चलते हुए सीथियन्स भी आए थे. कहा तो यह भी जाता है कि यूनान का सिकंदर भी इसी रास्ते से भारत आया था. वह काबुल नदी और उसके बाद सिंध नदी को पार करके तक्षशिला में घुसा था. यह बात 325 ईसापूर्व की है.
इन ऐतिहासिक और भौगोलिक सच्चाइयों को नेहरू बहुत पहले से समझ रहे थे. वह जानते थे कि अगर कश्मीर भारत में नहीं रहा और पाकिस्तान में चला गया या आजाद फिर हो गया, तो दुनिया की शक्तियां कश्मीर के बहाने भारत के सिर पर नाचेंगीं. यह भारत की सुरक्षा के लिए एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय खतरा बना जाएगा. इस खतरे की अन्य अंतरराष्ट्रीय बातों को दूसरे अध्याय में शामिल करेंगे.
इस रणनीतिक विचार के साथ नेहरू के जेहन में एक सैद्धांतिक हलचल भी मची हुई थी. यह थी महात्मा गांधी और पंडितजी की धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी नीति. भारत की आजादी के समय महात्मा गांधी लगातार एक बात कह रहे थे कि अगर कश्मीर की जनता भारत के साथ आ जाती है और वह निहत्थे ही अपनी लड़ाई लड़ती है, तो दुनिया के सामने यह अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता की अद्भुत लड़ाई होगी. वह बार-बार कह रहे थे कि अगर हमने कश्मीर में सिद्धांतों की जीत हासिल कर ली, तो पूरा भारत फतह कर लेंगे. बापू का इशारा इस तरफ था कि अगर मुस्लिम बहुल कश्मीर मानवता के सिद्धांतों पर चलकर भारत के साथ आता है, तो हिंदू-मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा करने की थ्योरी ही झूठी साबित हो जाएगी. यही नहीं, देश में फैले भयंकर सांप्रदायिक विद्वेष को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी. जो बापू सोच रहे थे, वही उनके जवाहर की भी सोच थी.
मार्च 1948 में संविधान सभा में दिए भाषण में नेहरू कहते हैं:
“दुर्भाग्य से भारत में हम हर समस्या के बारे में अत्यधिक सांप्रदायिक दृष्टिकोण से सोचने के आदी हो गए हैं. हम ज्यादातर हिंदू बनाम मुसलमान या हिंदू बनाम सिख या मुस्लिम बनाम अन्य कोई, इसी तरह सोचते हैं. सांप्रदायिक विवादों के इस संदर्भ के बीच कश्मीर का मामला सबसे जुदा है, क्योंकि कश्मीर सांप्रदायिक विवाद का मुद्दा नहीं है. हां, यह राजनैतिक विवाद का मुद्दा हो सकता है. अगर आपको लगता है तो यह दूसरे किसी भी विवाद का मुद्दा हो सकता है. लेकिन, आवश्यक रूप से यह सांप्रदायिक विवाद का मुद्दा नहीं है. इसलिए कश्मीर का संघर्ष, जैसा की जाहिर है कि इसने कश्मीर के लोगों को बहुत कष्ट दिया है और इसने भारत सरकार और भारत के लोगों पर भी बोझ डाला है, इसके बावजूद हम इसे संभावना और आशा की तरह देखते हैं. हम इसे कई तत्वों हिंदू और मुसलमान और सिखों के बीच सहयोग के तौर पर देखते हैं. हम देखते हैं कि यह सब लोग मिलकर अपनी राजनैतिक आजादी की लड़ाई लड़ें. मैं यह बातें इसलिए जोर देकर कह रहा हूं, क्योंकि सीमा के पार हमारे विरोधी कह रहे हैं कि यह हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है. हम कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की मदद करने के लिए वहां गए हैं,कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी हमारे साथ नहीं है. इससे ज्यादा सफेद झूठ और क्या हो सकता है. हम वहां कश्मीर के महाराजा के न्योते पर भी नहीं जाते, अगर उस न्योते को वहां की जनता के नेताओं की सहमति हासिल नहीं होती. मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सेनाओं ने वहां अदम्य बहादुरी का परिचय दिया है, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी सेनाओं को कामयाबी नहीं मिली होती, अगर उन्हें कश्मीर के लोगों की मदद और सहयोग न मिलता.’’
यहां तक, अंदाजा लग गया होगा कि नेहरू कश्मीर को इसलिए ही नहीं चाहते थे कि वह स्वयं कश्मीरी पंडित थे,बल्कि वह इसलिए चाहते थे क्योंकि वह सही मायनों में पंडित थे, जो जानता था कि कश्मीर का क्षेत्रीय राजनीति में और व्यापक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आगे किस-किस तरह इस्तेमाल हो सकता है. क्यों पश्चिम की ताकतें इसे अपने इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान को देना चाहेंगी.
इसके अलावा नेहरू यह तो बताना चाहते ही थे कि भले ही पूरे भारत में महात्मा गांधी की सांप्रदायिकता विरोधी नीति पूरी तरह कामयाब न हो पाई हो, लेकिन कश्मीर में तो ऐसा माहौल बने, जहां गांधी की बहुलतावादी नीति जीते.
गांधीजी ने यह बात कही भी थी. कश्मीर की रक्षा के लिए भारतीय सेना भेजे जाने के फैसले की महात्मा गांधी ने तारीफ की थी. अपने एक प्रार्थना प्रवचन में गांधी जी ने कहा था: “यदि थर्मापली के स्पार्टनों की तरह छोटी सी संघ सेना बहादुरी से कश्मीर की रक्षा करते हुए मर मिटे, तो मैं एक आंसू नहीं बहाऊंगा. अगर शेख अब्दुल्ला और उनके मुसलमान, हिंदू और सिख साथी कश्मीर को बचाने में अपने-अपने कर्तव्य के स्थान पर मर जाएं, तो उसकी भी मैं परवाह नहीं करूंगा. यह शेष भारत के लिए एक गौरव पूर्ण उदाहरण होगा. इससे भारत के लोग यह भूल जाएंगे कि हिंदू, मुसलमान और सिख कभी एक-दूसरे के शत्रु थे.”
नेहरू यह सब कैसे कर रहे थे
लेकिन यह सब किया कैसे जाए. यह कैसे संभव हो कि मुस्लिम बहुल आबादी वाले कश्मीर के जननेता मुस्लिम लीग के बजाय कांग्रेस के साथ खड़े हों.
अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस पार्टी की घोषित नीति थी कि कांग्रेस अंग्रेजी राज के खिलाफ तो अभियान चलाएगी, लेकिन देसी राजाओं की रियासतों के जन आंदोलन से सीधे नहीं जुड़ेगी. एक तरह से देसी रियासतों में कांग्रेस होगी ही नहीं. बाद में कांग्रेस ने अपने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में यह स्पष्ट किया कि भले ही राजाओं के खिलाफ कांग्रेस सीधे कोई आंदोलन नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस के नेता अपनी निजी हैसियत में वहां चल रहे, आजादी के आंदोलनों को मदद दे सकते हैं. इस काम के लिए कांग्रेस ने अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन किया था, जो रियासतों में चलने वाले आंदोलनों से जुड़ी रहती थी. तब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संस्था के अध्यक्ष थे.
इस पहलू को समझने के बाद, अब वापस कश्मीर के घटनाक्रम पर लौटते हैं. 15 अगस्त 1947 के पहले के कश्मीर के निजाम का वर्णन सरदार पटेल के सचिव वी शंकर ने ‘सरदार पटेल के चुने हुए पत्र व्यवहार खंड-1’ में कुछ इस तरह किया है:
“महाराजा हरि सिंह का प्रशासन कार्यकुशल होते हुए भी प्रबुद्ध निरंकुश शासन था, जो महाराजा द्वारा पसंद किए गए प्रसिद्ध और प्रतिभावान लोगों द्वारा चलाया जाता था. राज्य की आबादी के पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग का राज्य की सरकार में कोई हाथ नहीं था.”
इन हालात में कश्मीर में आजादी का आंदोलन कैसे पनपा. इसका जिक्र नेहरू की बायोग्राफी में फ्रैंक मोरिस कुछ इस तरह करते हैं: “1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन से पहले अशिक्षित और दबे-कुचले कश्मीर के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक नहीं थे. नेहरू की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना का लक्ष्य बताया था. यह पहला मौका था जब कश्मीर में राजनैतिक जागरूकता ने जोर पकड़ा. उस समय 25 साल के बेरोजगार अध्यापक शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में आजादी के आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया. 6 फुट 4 इंच लंबे अब्दुल्ला जल्द ही शेर-ए-कश्मीर के नाम से जाने जाने लगे. वह निडर थे, सीधा और साफ बोलने वाले थे,हालांकि उनके भीतर कहीं एक गहरी कुटिलता और छल था.
1931 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर में एक छोटा सा प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद अब्दुल्ला को कई हफ्तों के लिए जेल में डाल दिया गया. उसके बाद अक्टूबर 1932 में बने अब्दुल्ला के संगठन ‘ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस’ ने कई विरोध और विद्रोह किए.
अब्दुल्ला शुरू से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति से प्रभावित थे और वह विशेष रूप से नेहरू के करीब आते चले गए. बदले में नेहरू ने भी उनकी राष्ट्रीय सोच की तारीफ की और उसे स्वीकार किया. धीरे-धीरे दोनों व्यक्ति करीबी दोस्त हो गए. नेहरू के इसी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर अब्दुल्ला ने जून 1939 में ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कान्फ्रेंस को अपना नाम बदलकर ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस करने के लिए मना लिया. जब अब्दुल्ला अपने संगठन में धर्म विशेष की जगह राष्ट्रवादी बदलाव कर रहे थे, तो उनके संगठन का एक छोटा धड़ा चौधरी गुलाम अब्बास के नेतृत्व में अलग हो गया. और खुद को मुस्लिम कांफ्रेंस ही कहता रहा. इस धड़े ने बाद में पाकिस्तान की हिमायत की, वहीं शेख अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस के और करीब आ गई.’’
इस पूरे घटनाक्रम से इतना तो समझा ही जा सकता है कि नेहरू बहुत पहले से कश्मीर को भारत में लाने की तैयारी कर रहे थे. एक तो वह प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते राज्यों के आंदोलनों से जुड़े हुए थे, दूसरे यह कि उन्होंने बहुत सावधानी से मुस्लिम कांफ्रेंस का नाम और नीतियां समय रहते बदलवाकर इसे नेशनल कांफ्रेंस करा लिया और उसे धर्मनिरपेक्ष नीतियों के साथ ले आए. यही नहीं, शेख अब्दुल्ला के साथ उनका जो निजी दोस्ताना था और शेख अब्दुल्ला पर उनका जो असर था, उसके कारण मुस्लिम आबादी के नेता होते हुए भी शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान या मुस्लिम लीग की तुलना में खुद को भारत के ज्यादा करीब पाने लगे.
इस दोस्ती का आलम यह था कि 1946 में शेख अब्दुल्ला के राजा के खिलाफ चलाए जा रहे, कश्मीर छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए नेहरू कश्मीर पहुंच गए और वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, भारत के दबाव में कुछ घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया. यही नहीं, नेहरू जेल में बंद शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भी एक वकील की हैसियत से कश्मीर गए.
शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते की एक बानगी रामचंद्र गुहा ने अपनी चर्चित पुस्तक इंडया आफ्टर गांधी में पेश की है:
‘‘शेख अब्दुल्ला की पहली गिरफ्तारी के दो महीने बाद नेहरू ने लिखा था कि वास्तव में शेख की गिरफ्तारी एक ऐसी बात है जो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है. धीरे-धीरे महीने साल में बदल गए और उनकी तकलीफ आत्मिक दुख का कारण बनती गई. इस तकलीफ को कम करने का एक तरीका था कि नेहरू ने अपने मित्र के बेटे की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना शुरू किया. कुछ विवरणों के मुताबिक उन्होंने इसका खर्चा भी वहन किया. जुलाई 1955 में अब्दुल्ला के बड़े बेटे फारूक ने नेहरू से मुलाकात की जो उस समय जयपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे. फारूक ने प्रधानमंत्री से कहा कि उसके सहपाठी लगातार उसके पिता को गद्दार कहते रहते हैं. नेहरू ने इसके बाद राजस्थान के एक मंत्री को लिखा कि फारुख के रहने-सहने की उचित व्यवस्था करें और उनके लिए कुछ अच्छे दोस्तों की तलाश करें, ताकि वह किसी तरह की हीन भावना में न पड़ें. जैसा कि नेहरू ने खुद लिखा है कि कुछ लोग बड़े बेवकूफाना ढंग से सोचते हैं कि चूंकि शेख अब्दुल्ला के साथ हमारा कुछ मतभेद है इसलिए हमें उनकी बेटे और उनके परिवार की तरफ झुकाव नहीं रखना चाहिए. यह बात सिर्फ बकवास ही नहीं है, बल्कि मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा सोचता हूं. शेख अब्दुल्ला जेल में हैं इसलिए यह मेरा विशेष दायित्व है कि मुझे उनके बेटे और परिवार का ध्यान रखना चाहिए.
इस निजी किस्म की कहानी को यहां छेपक के रूप में लाना इसलिए जरूरी था कि पता चले कि नेहरू ने कश्मीर के मुस्लिम नेतृत्व को न सिर्फ राजनीति और कूटनीति से भारत के पक्ष में किया, बल्कि असल में अपना दिल कश्मीर को देकर कश्मीरियों का दिल भारत के पक्ष में किया. इसीलिए जब हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए तो उसे स्वीकृति देने के लिए कश्मीर की जनता की तरफ से शेख अब्दुल्ला खड़े थे, अगर शेख अब्दुल्ला की सहमति न होती यानी कश्मीर की जनता की सहमति न होती तो हैदराबाद या जूनागढ़ के नवाबों की तरह कश्मीर के राजा की बात भी नहीं मानी जाती. और कोई मान भी लेता तो भारत के सर्वोच्च नेता महात्मा गांधी नहीं मानते.
कश्मीर के भारत में विलय के बाद गांधी जी ने अपने एक प्रार्थना प्रवचन में कहा:
मेरी सदा यह राय रही है कि सारे ही राज्यों के सच्चे शासक वहां के लोग हैं. कश्मीर के लोगों को किसी बाहरी या भीतरी दबाव अथवा बल प्रदर्शन के बिना इस प्रश्न का निर्णय स्वयं करना होगा. पाकिस्तान सरकार कश्मीर को पाकिस्तान में मिलने के लिए दबाती रही है. इसलिए जब महाराजा ने संकट में फंसकर शेख अब्दुल्ला के समर्थन से संघ में शामिल होना चाहा तो भारतीय गवर्नर जनरल इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सके. यदि महाराजा अकेले ही भारत के साथ मिलना चाहते, तो मैं उसका समर्थन नहीं कर पाता. परंतु हुआ यह कि महाराजा और शेख अब्दुल्ला दोनों ने जम्मू और कश्मीर के लोगों की तरफ से बोलते हुए ऐसा चाहा था. शेख अब्दुल्ला इसलिए मैदान में आए क्योंकि उनका दावा मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि सारे कश्मीर के लोगों का प्रतिनिध होने का है.”
इस तरह भारत के असली चाणक्य नेहरू ने हर हाल में पाकिस्तान के साथ जाते दिख रहे कश्मीर को अपनी कूटनीति और राजनीति से भारत का अभिन्न अंग बना दिया.