
पिछले करीब सात वर्ष से देश में ‘पोस्ट ट्रुथ मीडिया’ का दौर चल रहा है। इस दौर में मीडिया जितना विवादास्पद बना है,उतना पहले कभी नहीं रहा। पोस्ट ट्रुथ मीडिया ने मीडिया की सार्थकता, प्रामाणिकता और छवि पर कई प्रश्न लगा दिए हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम मीडिया के चरित्र को सही परिप्रेक्ष्य में समझें और लोकतंत्र की सेहत के लिए इसे प्रभावशाली बनाएं। पोस्ट ट्रुथ मीडिया या सत्योत्तर मीडिया का सीधा अर्थ है- ‘सत्य का असत्य में, असत्य का सत्य में’ सुविधानुकूल रूपांतरण। वर्तमान सत्ताधीश और मीडियापति इस शस्त्र का बर्बरतापूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर प्रॉक्सी वार के रूप में देखे जा रहे हैं। इन छाया युद्धों का सीधा संबंध देश के लोकतंत्र और संविधान से है, क्योंकि वर्तमान पॉलिटिकल क्लास पोस्ट ट्रुथ मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र और संविधान का चरित्र ही बदल देना चाहती है। जहां वह भारत को एकलतावादी बना देना चाहती है वहीं मीडिया को भी एकरंगी सांचे में ढाल देना चाहती है। गोदी मीडिया इसका जीवंत परिणाम है।
नि:संदेह नेहरू युग के मीडिया और साल 2020 के मोदी युग के मीडिया की तुलना करना नितांत अव्यावहारिक होगा। दोनों में किसी भी प्रकार की बुनियादी समानताएं नहीं हैं, सिवाय अभिव्यक्ति के। मैं नेहरू युग को क्यों याद कर रहा हूं, इसकी वजह यह है कि प्रेस को सही दिशा में रखने के लिए पहले प्रेस आयोग का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उस जमाने में मीडिया को प्रेस से संबोधित किया जाता था। उस दौर में लोक अभिव्यक्ति के मूलत: दो माध्यम हुआ करते थे, अखबार और सरकार द्वारा संचालित आकाशवाणी। यह वह दौर था जब प्रेस को राज्य का चौथा स्तंभ कहा जाता था और राज्य भी इसकी प्रासंगिकता की रक्षा करता था। इसकी गरिमा, इसकी महत्ता जरूरी समझी जाती थी क्योंकि इसके माध्यम से ही राज्य और जनता के बीच स्वस्थ संवाद को बनाये रखा जा सकता है। चूंकि नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लोकतांत्रिक थे और आधुनिकतावादी भी। वैज्ञानिक मानस से लैस थे। इसलिए वे प्रेस से यह अपेक्षा रखते थे कि यह आधुनिक लोकतंत्र को सार्थक बनाए रखने में एक हस्तक्षेपकर्मी की भूमिका निभाए और जनता का वैज्ञानिक मानस के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दे। वह यह भी चाहते थे कि प्रेस पूरी तौर पर ‘प्रोफेशनल’ बने। यहां प्रोफेशनल से मेरा तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यवसाय की बुनियादी आचार संहिता होती है। नैतिकता होती है, जिसका परिपालन बेहद जरूरी है। मैं मिशनवादी और प्रोफेशनवादी पत्रकारिता में अंतर करता हूं। शुद्ध व्यवसाय पर आधारित पत्रकारिता में लाभ-अर्जन की इच्छा तो रहती है, लेकिन किसी भी व्यवसाय के मूल्यों को केन्द्र में रखकर ही उसे चलाया जाता है। नेहरू जी यही चाहते थे कि प्रेस निडर, स्वतंत्र रहे और व्यावसायिक मूल्यों का पालन करे। इसलिए उन्होंने पांचवें दशक के मध्य में प्रेस आयोग का गठन किया।
इस आयोग पर यह जिम्मेदारी थी कि वह प्रेस की स्वतंत्रता और उसके स्वस्थ संचालन के लिए क्या-क्या कसौटियां होनी चाहिए, इसकी सिफारिश भारत सरकार से करे। नेहरूजी उस समय अंग्रेजी प्रेस को मूलतः जूट प्रेस के नाम से संबोधित किया करते थे। यानी डालमिया जैसे एकाधिकार पतियों के हाथों में टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी महत्वपूर्ण प्रेस हुआ करती थी। जूट से अर्जित पूंजी भारत के अंग्रेजी प्रेस पर छाई हुई थी, जबकि भाषाई प्रेस पर मंझोली और महाजनी पूंजी का दबदबा था। उस दौर में महानगरीय प्रेस प्रदेश और राजधानी स्तर से निकलने वाले दैनिक और संभागीय स्तर से निकलने वाले संस्करण त्रिस्तरीय प्रेस हुआ करती थी। हालांकि उसमें कई प्रकार के भटकाव थे।
प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशें आने के बाद निजी क्षेत्र के प्रेस संचालन में कई प्रकार के सुधार किए गए। इसी दौर में प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसे हम प्रेस कॉउंसिल आफ इण्डिया भी कहते हैं। तमाम समाचार पत्रों को संतुलित विज्ञापन सरकार के मिलें, इसके लिए डीएवीपी का गठन किया गया। सिफारिश यह भी की गई कि प्रेस का स्वामित्व मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केन्द्रित न रहे। नेहरूजी यह जरूरी समझते थे कि प्रेस और उद्योग दोनों में किसी प्रकार का संबंध न रहे। दोनों स्वतंत्र रहें। यदि उद्योगपति के हाथों में अखबार रहेंगे तो वे जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। वह सिर्फ अपने मालिकों के स्वार्थों की पूर्ति के माध्यम बन जाएंगे।
वेज बोर्ड के माध्यम से पत्रकार और कर्मचारियों की सेवाएं शुरू की गईं। मालिकों से कहा गया कि वे वेज बोर्ड के अनुसार अपने कर्मचारियों और पत्रकारों को वेतनमान की विभिन्न श्रेणियों में रखें। इस तरह की कई अनुशंसाएं की गईं, जिससे कि प्रेस न सरकार पर निर्भर रहे न ही पूंजी पर। समाचार, विचार और विज्ञापन के बीच संतुलन बना रहे। 30-40 प्रतिशत से अधिक विज्ञापन न छापे जाएं, इसकी भी सिफारिश की गई। नि:संदेह प्रथम प्रेस आयोग की अधिकांश सिफारिशों को लागू किया गया और मालिकों ने इसका परिपालन भी किया। लेकिन उत्तर नेहरू कालीन सरकारों के दौरान विभिन्न पूंजीगत व राजनीतिक दबावों के कारण प्रेस प्रबंधकों पर जितना प्रभावशाली अंकुश रहना चाहिए था, नहीं रह सका।
प्रेस का उत्तरोत्तर व्यापारीकरण होता चला गया। प्रेस की आचार संहिता हाशिए पर खिसकती गई और मुनाफा केन्द्रीय भूमिका निभाने लगा। साल 1975 के आपातकाल में प्रेस पर सेन्सरशिप लाद दी गई और इंदिरा गांधी सरकार के दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पहला कुठाराघात हुआ। साल 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। तत्पश्चात मांग उठी कि दूसरे प्रेस आयोग का गठन हो, क्योंकि उस समय तक प्रेस का चरित्र तेजी से बदलने लगा था। देश राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। प्रेस प्रिंटिग टेक्नोलाजी में परिवर्तन हो रहा था। बड़ी पूंजी का प्रवेश भाषाई प्रेस में भी होने लगा। विज्ञापन की संस्कृति का विस्तार तेजी से होने लगा। यहां मुझे आधुनिक पत्रकारिता के वैचारिक पितामह बाबूराव विष्णु पराड़कर का कथन याद आ रहा है। पराड़कर जी ने 1925 में संपादकों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘आने वाले समय में अखबार चिकने-चुपड़े कागज पर निकलेंगे, अच्छी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी रहेगी, लेकिन अखबारों में आत्मा नहीं रहेगी और प्रेस पर विज्ञापन का कारोबार छाया रहेगा।’ उनकी यह चेतावनी 21वीं सदी में कितनी स्वयं सिद्ध है, हम स्वयं इसे देख सकते हैं।
अत: इस पृष्ठभूमि में दूसरे प्रेस आयोग की स्थापना की मांग तेजी से जोर पकड़ने लगी। इसके गठन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई। लेकिन जनता पार्टी और मोरारजी देसाई सरकार के बिखराव के कारण दूसरा प्रेस आयोग काम नहीं कर सका। वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में पुनः वापसी के पश्चात इस आयोग के गठन पर फिर से कार्य शुरू हुआ। इसमें भी कई प्रकार की ऐसी सिफारिशें की गईं, जिससे प्रेस की आजादी सुरक्षित रहे। लेकिन आयोग के कतिपय सदस्यों ने इस बात का विरोध किया था कि प्रेस को उद्योग से अलग किया जाए। दूसरे अर्थों में कतिपय संपादक सदस्य नहीं चाहते थे कि प्रेस से उद्योगपतियों का नियंत्रण समाप्त हो। फिर भी अधिकांश सदस्य यह चाहते थे कि प्रेस के मालिकान सिर्फ प्रेस का व्यवसाय करें न कि अन्य उद्योगों का। यह सर्वविदित है कि हिंदुस्तान टाइम्स समूह पर बिड़ला, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह पर साहू शांति प्रसाद जैन और स्टेट्समैन पर टाटा जैसे बड़े उद्योगपतियों का नियंत्रण शुरू से रहा है। जब उद्योगपति अख़बार चलाएंगे तो जाहिर है कि उनके समक्ष अपने औद्योगिक हितों के संरक्षण, प्रोत्साहन और विस्तार का लक्ष्य पहली प्राथमिकता पर रहेगा। इसमें समाचार और विचार दोयम दर्जे के रहेंगे।
पूंजीपतियों की इसी मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर दूसरे प्रेस आयोग ने भी इस सिफारिश को पुन: रेखांकित किया और यह तय भी किया कि समाचार, विचार और विज्ञापन में संतुलन रहना चाहिए। अखबार समाचार के लिए हैं न कि विज्ञापन के लिए। दुर्भाग्य से दोनों प्रेस आयोगों की सिफारिशों को शत-प्रतिशत ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। फलस्वरूप प्रेस का स्वरूप बेडौल बनता चला गया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के शासन काल में प्रेस का मीडिया में रूपांतरण हो गया, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रवेश हो चुका था। निजी क्षेत्र के चैनल तेजी से अस्तित्व में आने लगे। कुछ समय बाद साइबर पत्रकारिता का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया भी अस्तित्व में आ गया। लोगों के ब्लॉग बनने लगे। हर एक अखबार का नेट संस्करण प्रकाशित होने लगा। अब मुद्रित अखबार भी कई स्तरीय हो गए। जहां पहले केवल तीन स्तरीय थे वहीं अब चार-पांच स्तरीय बन गए। महानगरीय, राज्यों की राजधानी, संभागीय स्तर, जिला स्तर और ताल्लुका स्तर तक से संस्करण निकलने लगे। ऐसे में यह और भी जरूरी हो गया कि अब प्रेस आयोग के स्थान पर एक तीसरे बहुआयामी मीडिया आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि आज मीडिया का तेजी से एकाधिकारकरण हो गया है। एक-एक औद्दोगिक घरानों के हाथों में 20-20 चैनल्स हैं। इसके साथ-साथ अखबार भी हैं। क्रॉस ऑनरशिप का विस्तार तेजी से हो रहा है।
क्रॉस ऑनरशिप का मतलब है कि एक पूंजीपति अखबार भी निकाल सकता है और चैनल भी चला सकता है। वह दूसरे उद्योग भी चला सकता है। जबकि होना यह चाहिए कि एक मालिक को केवल एक ही स्वामित्व की इजाजत दी जानी चाहिए। यदि वह अखबारपति है तो सिर्फ अखबारपति ही रहे, वह चैनलपति न बने। यदि वह चैनल चलाना चाहता है तो अखबार न निकाले। आज देखने में यह आता है कि एक पूंजीपति अखबार के साथ-साथ चैनल चला रहा है। गन्ना मिलें चला रहा है। सीमेंट फैक्ट्री संचालित कर रहा है। कोयला खानों का ठेका ले रहा है। रियल स्टेट का कारोबार कर रहा है। चिटफंडी पूंजी में हाथ आजमा रहा है। संचार और मोबाइल की दुनिया की ठेकेदारी कर रहा है। उदाहरण के लिए इसमें टाइम्स समूह, हिन्दुस्तान टाइम्स समूह, दैनिक भास्कर समूह, लोकमत समूह, सकाल ग्रुप, प्रभात खबर, जागरण समूह, सहारा समूह, टीवी टुडे ग्रुप, नेटवर्क 18 ग्रुप, ए.बी.पी. ग्रुप आदि का नाम लिया जा सकता है। इससे अभिव्यक्ति की गतिशीलता व स्वतंत्रता प्राय: संकटग्रस्त रहती है। सत्ता प्रतिष्ठान मालिक की बाहें मरोड़ कर सभी माध्यमों पर रोब-शोब से अपना कब्जा जमा लेता है। यही आज हो रहा है। इसी कारण आज फेक न्यूज का बोलबाला है। जब अभिव्यक्ति के माध्यम विपथगामी बन जाते हैं। वाचाल हो जाते हैं तब न राजधर्म का पालन होता है न लोकधर्म का। राजधर्म और लोकधर्म दोनों की अभिव्यक्ति के लिए पूंजी के एकछत्र नियंत्रण से मुक्त रहना जरूरी है। इसलिए क्रॉस ऑनरशिप को समाप्त किया जाना लोकतंत्र की रक्षा के लिए बेहद आवश्यक है।
दूसरे अर्थों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निरंतर संकुचितकरण होता जा रहा है। इतना ही नहीं नेहरू युग से चलने वाली वेज बोर्ड की सेवा शर्तें भी अब लगभग मृत हैं। उसके स्थान पर मीडिया में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इससे पत्रकारों और कर्मचारियों की सेवाएं अस्थिर बन चुकी हैं। वह निरंतर संकटग्रस्त रहती हैं और अनुबंध से बंधी होती हैं। प्रबंधन, ब्राण्ड मैनेजर और संपादक की स्वेछाचारिता पर अनुबंध का विस्तार आश्रित रहता है। ऐसी स्थिति में कोई भी पत्रकार स्वतंत्र होकर सेवा नहीं कर पाता। उस पर अस्थाई सेवा की तलवार लटकी रहती है। वह त्रिशंकु बना रहता है और प्रबंधकों के समक्ष लगभग नतमस्तक रहता है। यहां यह भी याद दिलाना जरूरी है कि आज मीडिया में संपादक संस्था लगभग कोमा में है। उसका स्थान ब्राण्ड मैनेजर ने ले लिया है। ब्राण्ड मैनेजर या विज्ञापन प्रबंधक तय करता है कि अख़बार या चैनल का कंटेन्ट क्या होना चाहिए। सामग्री को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए यानी प्रस्तुतीकरण का निर्णय भी अब ब्राण्ड मैनेजर तय करने लगे हैं। समाचार और संपादकीय दोनों ही दोयम दर्जे पर हैं। यहां यह कहना गैर जरूरी नहीं होगा कि अब मीडिया में विदेशी पूंजी नियोजन का रास्ता साफ कर दिया गया है। अटल बिहारी बाजपेयी सरकार ने विदेशी पूंजी नियोजन की अनुमति दी थी और तय किया था कि 24 प्रतिशत तक का विदेशी नियोजन अखबारों में हो सकता है। तत्पश्चात मनमोहन सिंह सरकार ने यह प्रतिशत 50 से भी ज्यादा कर दिया। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी द्वार खोल दिए गए हैं। जाहिर है कि जब विदेशी पूंजी नियोजक मीडिया में आएंगे तो वे अपने राष्ट्रीय अथवा पूंजीगत हितों को ध्यान में रखकर ही जनमत तैयार करने की कोशिश करेंगे। उनके समक्ष भारत के जनमुद्दे, जन समस्याएं या जनसरोकार प्रथम प्राथमिकता में नहीं रहेंगे।
यहां टाइम्स समूह के प्रबंधकों के इस कथन की याद दिलाना मौजू रहेगा कि ‘हम समाचारों का नहीं विज्ञापनों का व्यापार करते हैं। हमारे लिए अखबार सिर्फ एक ‘उत्पाद’ यानी प्रोडक्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।’ यहीं मैं यह सवाल उठाता हूं कि यदि अखबार या मीडिया को सिर्फ प्रोडक्ट ही मान लिया जाएगा तो इसकी चतुर्थ स्तंभ की भूमिका का हमेशा के लिए पटाक्षेप हो जाएगा। दरअसल मीडिया प्रोडक्ट होते हुए भी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसका चरित्र मूलत: हस्तक्षेपधर्मी होता है। अखबार या चैनल अपने संचार के माध्यम से जनता और राज्य दोनों के बीच जहां सेतु बनते हैं वहीं दोनों को परस्पर एक-दूसरे के अधिकार, कर्तव्य और सरोकारों से अवगत भी कराते हैं। उदाहरण के लिए साबुन, कार, हवाई जहाज आदि भी तकनीकी दृष्टि से प्रोडक्ट हैं। लेकिन इनमें हस्तक्षेप और संवाद की प्रवृत्ति नहीं रहती है। इनका मिजाज मूल उत्पाद स्रोत से लेकर अंतिम क्षय तक यथावत रहता है। इसके विपरीत मीडिया आरंभ से अंत तक संवादधर्मी होता है और इतिहास में ये बड़े-बड़े युगांतकारी परिवर्तनों का वाहक भी रहा है। हम क्यों भूल जाते हैं कि मार्क्स, लेनिन, गांधी, अंबेडकर, मौलाना आजाद, नेहरू, डॉ. लोहिया जैसे लोक चितंक व लोक नायक मूलत: पत्रकार या कम्युनिकेटर रहे हैं। 1903 में गांधीजी ने ‘इंडियन ओपीनियन’ के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में परिर्वतन की चेतना पैदा की थी वहीं 1915 में भारत लौटकर ‘यंग इंडिया’, ‘हरिजन’ जैसे अखबार निकाले। 1825 में राजा राममोहन राय ने बंगला, उर्दू और हिंदुस्तानी में अखबार निकालकर क्रांतिकारी समाज सुधार किये थे। क्या मीडिया के इस योगदान को भुलाया जा सकता है? मेरे मन में अखबार रहे या चैनल या सोशल मीडिया, मूलत: बहुआयामी संवाद व परिवर्तन के माध्यम होते हैं।
अत: इस परिप्रेक्ष्य में बहुआयामी मीडिया आयोग और भी आवश्यक हो गया है या अपरिहार्य है। सरकार चाहे तो प्रेस के लिए अलग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग स्वतंत्र आयोग की स्थापना कर सकती है। चूंकि क्रॉस ऑनरशिप का समय है, इसलिए एक व्यापक समन्वयक मीडिया आयोग का गठन अधिक सार्थक रहेगा। इसमें सभी माध्यमों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। मीडिया विशेषज्ञों, समाज वैज्ञानिकों, समाज कर्मियों, उद्योगपतियों और सरकार के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाया जा सकता है। इस संस्था के माध्यम से हम मीडिया की स्वतंत्रता को सुरक्षित ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की सार्थकता को भी सुद्रढ़ बना सकते हैं। जिन देशों में मीडिया, गोदी मीडिया में रूपांतरित हो जाता है उन देशों में लोकतंत्र अपंग बन जाता है और अधिनायकवाद की शक्तियां समाज और राज्य पर हावी होने लगती हैं।
याद रखना चाहिए कि मीडिया आधुनिक समाज में केवल समाचार या विचार का ही माध्यम नहीं होता बल्कि वह नागरिकों को चेतनशील नागरिक बनाने की भूमिका भी निभाता है। आज जो लोग यह समझ रहे हैं कि मीडिया सिर्फ प्रोडक्ट है और विज्ञापन व्यापार है, वह मूलत: लोकतंत्र विरोधी और अधिनायकवादी हैं। अत: नए आयोग के गठन से हम उन तमाम आशंकाओं को काफी हद तक समाप्त कर सकते हैं, जिनकी वजह से मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र संकटग्रस्त है।
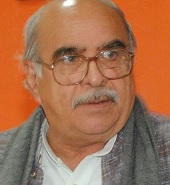
रामशऱण जोशी वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विजिल के सलाहकार मंडल के सम्मानित सदस्य हैं। यह लेख तद्भव पत्रिका के मीडिया विशेषांक में भी प्रकाशित हो रहा है।




















