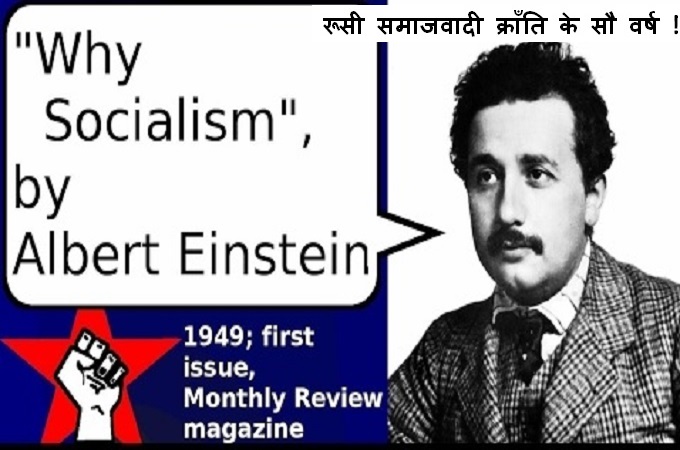
क्या ऐसे व्यक्ति का समाजवाद के बारे में विचार करना उचित है जो आर्थिक-सामाजिक मामलों का विशेषज्ञ नहीं है? कई कारणों से मेरा विश्वास है कि यह उचित है।
सबसे पहले वैज्ञानिक ज्ञान के दृष्टिकोण से इस सवाल पर विचार करें। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि खगोल विज्ञान और अर्थशास्त्र में कार्य-पद्धति का कोई मूलभूत फर्क नहीं है; दोनों ही क्षेत्रों में वैज्ञानिक किन्हीं परिघटनाओं के अन्तरसंबंधों को यथासम्भव स्पष्ट ढंग से समझने लायक बनाने के लिए उन परिघटनाओं के एक सीमित समूह के लिए सामान्य तौर पर स्वीकार्य नियमों को ढूँढने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तव में, इन दोनों विज्ञानों के बीच कार्य-पद्धति का फर्क मौजूद है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सामान्य नियमों की खोज इस बात से कठिन हो जाती है कि जिन आर्थिक परिघटनाओं का हम निरीक्षण करते हैं उन्हें बहुत-सी ऐसी बातें प्रभावित करती हैं जिनका मूल्यांकन अलग से कर पाना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि सभी जानते हैं, मानव इतिहास के तथाकथित सभ्यकाल के शुरू से ही संचित अनुभव ऐसे कारणों से बहुत ज्यादा प्रभावित और सीमित होते रहे हैं जो स्वभावत: किसी भी तरह महज आर्थिक नहीं होते। उदाहरण के लिए, इतिहास में अधिकतर बड़े राज्यों का अस्तित्व अन्य देशों को जीतने पर आधारित रहा है। विजेता लोगों ने कानूनी और आर्थिक तौर पर अपने को विजित देश के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के रूप में स्थापित किया। उन्होंने जमीन की मिल्कियत में अपना एकाधिकार कायम किया और अपने ही बीच के लोगों में से पुरोहित नियुक्त किये। शिक्षा पर नियन्त्रण रखने वाले पुरोहितों ने समाज के वर्ग-विभाजन को एक स्थायी संस्था का रूप दिया और मूल्यों के एक ढाँचे की रचना की, जिससे उसी समय से लोग काफी हद तक अचेतन रूप से, अपने सामाजिक व्यवहार में निर्देशित होते थे।
थोसर्टीन बेव्लेन द्वारा बतायी गयी मानव विकास की ‘लूटपाट की अवस्था’, कहने को तो बीते दिनों की ऐतिहासिक परम्परा है किंतु हम आज भी इससे आगे नहीं बढ़ सके हैं। जिन आर्थिक तथ्यों का हम निरीक्षण कर सकते हैं वे इसी अवस्था के हैं। इसलिए उनसे निकाले गये नियम भी दूसरी अवस्थाओं पर लागू नहीं होते। चूँकि समाजवाद का वास्तविक लक्ष्य सुनिश्चित तौर पर मानव विकास को, इस लूट-पाट की अवस्था को पार करना और उससे आगे बढ़ाना है, इसलिए अपनी मौजूदा स्थिति में आर्थिक विज्ञान भविष्य के समाजवादी समाज पर थोड़ा ही प्रकाश डाल सकता है।
दूसरे, समाजवाद का एक निश्चित सामाजिक और नैतिक लक्ष्य है। विज्ञान न तो लक्ष्यों का निर्माण कर सकता है और न ही उनको इन्सान के अन्दर उतार सकता है। विज्ञान, ज्यादा से ज्यादा, किन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन जुटा सकता है लेकिन खुद ये लक्ष्य उदात्त नैतिक आदर्शों वाले व्यक्तित्वों द्वारा ही तय किये जाते हैं और यदि ये लक्ष्य मुर्दा न होकर जीवन्त और ओजस्वी हैं तो उन बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाये और आगे बढ़ाये जाते हैं जो आधे अचेतन रूप से समाज के मन्थर विकास को निर्धारित करते हैं।
इन कारणों से, मानवीय समस्याओं के प्रश्न पर हमें विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धतियों को आवश्यकता से अधिक करके नहीं आँकना चाहिए और यह भी नहीं मानना चाहिए कि समाज के संगठन को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर अभिव्यक्ति का अधिकार केवल विशेषज्ञों का ही है।
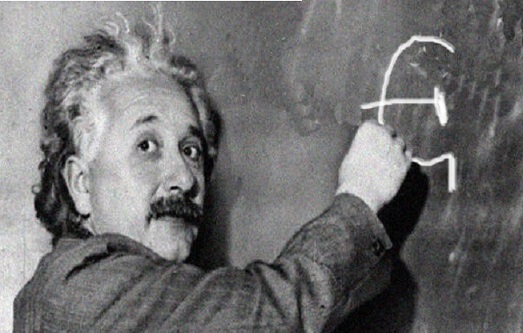
अनगिनत लोग इधर कुछ समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि मानव समाज एक संकट के दौर से गुजर रहा है और इसकी स्थिरता भयंकर रूप से छिन्न-भिन्न हो गई है। यह एक ऐसी स्थिति का लक्षण है, जब लोग उस छोटे या बड़े समूह के प्रति असंपृक्तता या यहाँ तक कि शत्रुतापूर्ण भाव महसूस करने लगते हैं, जिसमें वे रहते हैं। अपनी बात साफ करने के लिए एक निजी अनुभव बताऊँ। हाल ही में मैंने एक प्रबुद्ध सज्जन से एक और युद्ध के खतरे के बारे में बातचीत की जो मेरे विचार से मानवता के अस्तित्व के लिए गंभीर संकट पैदा कर देगा और मैंने कहा कि उस संकट से केवल एक राष्ट्रोपरि या अधिराष्ट्रीय (सुप्रानेशनल) संगठन ही रक्षा कर सकता है। इस पर मेरे अतिथि ने बहुत शांत और ठंढे ढंग से कहा, आप मानव जाति के मिट जाने का इतनी गम्भीरता से क्यों विरोध करते हैं?
मुझे यकीन है कि कम से कम एक शताब्दी पहले किसी ने भी इतने हल्के ढंग से इस किस्म का बयान नहीं दिया होता। यह एक ऐसे आदमी का बयान है जो अपने भीतर सामंजस्य कायम करने का निरर्थक प्रयास करता रहा है और काफी हद तक इसमें सफल होने की उम्मीद खो चुका है। यह एक ऐसे दर्दनाक एकाकीपन और अलगाव की अभिव्यक्ति है जिससे आजकल बहुत से लोग पीड़ित हैं। इसका कारण क्या है? क्या कोई समाधान भी है?
सवाल खड़े करना आसान है मगर किसी भी हद तक भरोसेमन्द जवाब देना कठिन है। फिर भी जहाँ तक हो सकेगा, मैं प्रयास अवश्य करूँगा हालाँकि इस तथ्य के प्रति मैं काफी सचेत हूँ कि हमारी अनुभूतियाँ और हमारे प्रयास अक्सर इतने अन्तर्विरोधी और दुर्बोध होते हैं कि सीधे-सीधे सूत्रों में व्यक्त नहीं किए जा सकते।
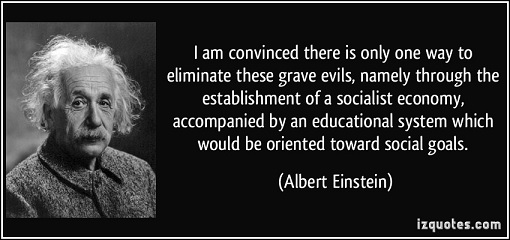 मनुष्य एक ही समय में और एक ही साथ एकाकी प्राणी भी होता है और सामाजिक प्राणी भी। एक एकाकी प्राणी की हैसियत से वह खुद अपने और अपने सबसे ज्यादा करीबी लोगों के अस्तित्व की रक्षा का प्रयास करता है, अपनी निजी इच्छाओं की तृप्ति का प्रयास करता है और अपनी सहज योग्यताओं के विकास का प्रयास करता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वह संगी-साथियों का स्नेह और सम्मान पाना चाहता है, उनकी खुशियों का भागीदार होना चाहता है, उनके दुखों में दिलासा देना और उनकी जिन्दगी को बेहतर बनाना चाहता है।
मनुष्य एक ही समय में और एक ही साथ एकाकी प्राणी भी होता है और सामाजिक प्राणी भी। एक एकाकी प्राणी की हैसियत से वह खुद अपने और अपने सबसे ज्यादा करीबी लोगों के अस्तित्व की रक्षा का प्रयास करता है, अपनी निजी इच्छाओं की तृप्ति का प्रयास करता है और अपनी सहज योग्यताओं के विकास का प्रयास करता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वह संगी-साथियों का स्नेह और सम्मान पाना चाहता है, उनकी खुशियों का भागीदार होना चाहता है, उनके दुखों में दिलासा देना और उनकी जिन्दगी को बेहतर बनाना चाहता है।
किसी मनुष्य के विशिष्ट चरित्र के पीछे केवल इन विविध व बहुधा परस्पर-विरोधी प्रयासों का ही अस्तित्व है और इनका विशिष्ट संयोजन ही उस हद को भी तय करता है जिस हद तक कोई मनुष्य आन्तरिक संतुलन पा सकता है तथा समाज के हित में योगदान कर सकता है। यह बिल्कुल संभव है कि इन दोनों प्रवृत्तियों की सापेक्षिक शक्ति का निर्धारण मुख्यतः वंशानुक्रम द्वारा होता है। किंतु अंतिम रूप से जो व्यक्ति उभर कर सामने आता है उसका निर्धारण मुख्य तौर पर उस समाज के ढाँचे द्वारा जिसमें वह पलता-बढ़ता है, उस समाज की परम्पराओं द्वारा और खास व्यवहारों के प्रति उस समाज के मूल्यांकन द्वारा होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए ‘समाज’ की धारणा का अर्थ अपने समकालीनों और पिछली पीढ़ियों के सभी लोगों के साथ उसके प्रत्यक्ष-परोक्ष संबंधों का कुल योग होता है। व्यक्ति सोचने, महसूस करने, प्रयास करने और कार्य करने में खुद सक्षम है, किंतु वह अपने शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक अस्तित्व के लिए समाज पर इतना अधिक निर्भर है कि समाज के दायरे के बाहर उसके विषय में विचार करना या उसे समझ पाना असंभव है। यह ‘समाज’ ही है जो आदमी को भोजन, वस्त्र, आवास, काम के औजार, भाषा, विचारों के रूप और उनकी अधिकांश अन्तर्वस्तु देता है, उसका जीवन उन लाखों-लाख वर्तमान और विगत लोगों के श्रम और कौशल के ही कारण सम्भव है, जो सब के सब इस छोटे से शब्द। ‘समाज’ के पीछे छिपे हुए हैं।
इसलिए, यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की समाज पर निर्भरता प्रकृति का एक ऐसा तथ्य है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह जैसे कि चींटियों और मक्खियों के मामले में है। लेकिन जहाँ चींटियों और मक्खियों की पूरी जीवन-प्रक्रिया की छोटी से छोटी बात भी सारत: वंशानुगत प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित होती है, वहीं मनुष्य की सामाजिक बनावट और अंतर्सम्बन्ध बदले जा सकते हैं तथा बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। स्मृति, नये संयोजनों के निर्माण की क्षमता व मौखिक संवाद के गुण द्वारा मनुष्य में वे विकास सम्भव हो सके हैं जो जैविक आवश्यकताओं द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। ऐसा विकास परम्पराओं, संस्थाओं व संगठनों में, साहित्य में, वैज्ञानिक व अभियांत्रिक उपलब्धियों में, कलाकृतियों में खुद को अभिव्यक्त करता है। इससे स्पष्ट होता है कि आदमी कैसे एक निश्चित अर्थ में अपने जीवन को खुद अपने व्यवहार से प्रभावित कर सकता है और कैसे इस प्रक्रिया में सचेत चिंतन और जरूरत एक भूमिका अदा कर सकते हैं।
आदमी जन्म से ही आनुवांशिकता द्वारा उन स्वभावगत आवेगों सहित जो मानव जाति की लाक्षणिक विशेषताएँ हैं, एक जैविक संरचना पाता है, जिसे हमें स्थिर व अपरिवर्तनीय मानना चाहिए। इसके साथ ही, अपने जीवन काल के दौरान वह एक सांस्कृतिक संरचना पाता है जिसे वह संवादों और बहुत से दूसरे प्रकार के प्रभावों के जरिए समाज से ग्रहण करता है। यह सांस्कृतिक संरचना ही वह चीज है जो समय के साथ-साथ बदलती रहती है तथा व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों को बहुत ज्यादा हद तक तय करती है। तथाकथित आदिम संस्कृतियों की तुलनात्मक खोज द्वारा आधुनिक नृतत्वशास्त्र हमें बताता है कि मनुष्यों के सामाजिक व्यवहार में काफी अन्तर हो सकता है जो समाज में प्रचलित सांस्कृतिक बनावट और समाज में प्रभावी संगठन के स्वरूप पर निर्भर है। किसी मानव समुदाय की उन्नति के लिए प्रयासरत लोग अपनी आशाएँ इसी पर आधारित कर सकते हैं कि अपनी जैविक संरचना के कारण, एक दूसरे का विनाश करने के लिए या किसी क्रूर व आत्मघाती स्थिति की दया पर बने रहने के लिए मानव जाति अभिशप्त नहीं है।
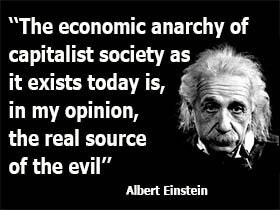 आदि हम खुद से सवाल करें कि मानव जीवन को यथासंभव संतोषजनक बनाने के लिए समाज की संरचना तथा व्यक्ति का सांस्कृतिक दृष्टिकोण कैसे बदला जाय, तो इस तथ्य के बारे में हमें सतत् सचेत रहना होगा कि कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ हैं जिन्हें बदल पाने में हम असमर्थ हैं। जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि व्यावहारिक अर्थों में मनुष्य की जैविक प्रकृति परिवर्तनशील नहीं है और पिछली शताब्दियों के तकनीकी व जनसांख्यिकीय विकास द्वारा निर्मित परिस्थितियाँ भी बनी रहने वाली हैं। अपेक्षतया घनी आबादियों के अस्तित्व की खातिर अपरिहार्य सामग्री की आपूर्ति के लिए एक चरम श्रम-विभाजन तथा अत्यन्त केन्द्रित उत्पादन तंत्र परम आवश्यक है। अतीत की ओर देखने पर वह समय, जो इतना रमणीय लगता था, जबकि व्यक्ति या सापेक्षतया छोटे समूह पूरी तरह आत्मनिर्भर रह सकते थे, सदा के लिए जा चुका है। यह कहना बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि मानव जाति ने अभी ही उत्पादन व उपभोग के एक विश्वव्यापी समुदाय की रचना कर ली है।
आदि हम खुद से सवाल करें कि मानव जीवन को यथासंभव संतोषजनक बनाने के लिए समाज की संरचना तथा व्यक्ति का सांस्कृतिक दृष्टिकोण कैसे बदला जाय, तो इस तथ्य के बारे में हमें सतत् सचेत रहना होगा कि कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ हैं जिन्हें बदल पाने में हम असमर्थ हैं। जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि व्यावहारिक अर्थों में मनुष्य की जैविक प्रकृति परिवर्तनशील नहीं है और पिछली शताब्दियों के तकनीकी व जनसांख्यिकीय विकास द्वारा निर्मित परिस्थितियाँ भी बनी रहने वाली हैं। अपेक्षतया घनी आबादियों के अस्तित्व की खातिर अपरिहार्य सामग्री की आपूर्ति के लिए एक चरम श्रम-विभाजन तथा अत्यन्त केन्द्रित उत्पादन तंत्र परम आवश्यक है। अतीत की ओर देखने पर वह समय, जो इतना रमणीय लगता था, जबकि व्यक्ति या सापेक्षतया छोटे समूह पूरी तरह आत्मनिर्भर रह सकते थे, सदा के लिए जा चुका है। यह कहना बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि मानव जाति ने अभी ही उत्पादन व उपभोग के एक विश्वव्यापी समुदाय की रचना कर ली है।
अब मैं उस बिन्दु पर पहुँच गया हूँ जहाँ से मैं आज के संकट के सारतत्व की ओर थोड़े में इंगित कर सकता हूँ। यह व्यक्ति के समाज के साथ संबंध से ताल्लुक रखता है। आज इंसान समाज के ऊपर अपनी निर्भरता के प्रति हमेशा से अधिक सचेत हो गया है। किन्तु वह इस निर्भरता को एक सकारात्मक गुण के रूप में, एक जीवंत बंधन के रूप में, एक रक्षक शक्ति के रूप में महसूस नहीं करता है। बल्कि इसे अपने प्राकृतिक अधिकारों, यहाँ तक कि अपने आर्थिक अस्तित्व के लिए भी खतरे के रूप में महसूस करता है। इसके अतिरिक्त, समाज में उसकी स्थिति ऐसी है कि उसकी (मानसिक) संरचना में निहित स्वार्थी प्रवृत्तियाँ निरन्तर प्रबल होती जा रही हैं। जबकि उसकी सामाजिक प्रवृत्तियों का, जो स्वभाव से ही कमजोर हैं, क्षरण तेज गति से हो रहा है। सभी लोग चाहे समाज में उनका जो स्थान हो, क्षरण की इस प्रक्रिया के शिकार हैं। अनजाने ही अपने स्वार्थों के कैदी बने हुए हैं, वे स्वयं को अरक्षित, एकाकी तथा जीवन के सहज, सरल व निष्कपट आनन्द से वंचित महसूस कर रहे हैं। आदमी की जिन्दगी छोटी और जोखिम भरी है। इस जीवन में खुद को समाज के प्रति समर्पित करके ही वह सार्थकता पा सकता है।
मेरे ख्याल से बुराई का असली स्रोत वर्तमान पूँजीवादी समाज की वह आर्थिक अराजकता है, जो आज मौजूद है। हमारे सामने विशाल उत्पादक समुदाय है जिसके सदस्य एक दूसरे को सामूहिक श्रम के फल से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वे बल प्रयोग द्वारा नहीं बल्कि कुल मिलाकर कानूनी रूप से कायम नियमों का ईमानदारी से पालन करके ही करते हैं। इस संदर्भ में यह अनुभव करना महत्वपूर्ण है कि उत्पादन के साधन, अर्थात् समस्त उत्पादक क्षमता जो उपभोक्ता सामग्री के साथ-साथ पूँजीगत सामग्री पैदा करने के लिए आवश्यक है, कानूनी तौर पर व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति हो सकते हैं और अधिकतर हैं भी।
आगे की बहस में सरलता की दृष्टि से मैं उन सभी लोगों को मजदूर कहूँगा जिनका उत्पादन के साधनों के मालिकाने में कोई हिस्सा नहीं है। हालाँकि यह इस शब्द के परंपरागत प्रयोग के पूरी तरह अनुरूप नहीं है। उत्पादन के साधनों का मालिक मजदूर की श्रमशक्ति को खरीद सकने की स्थिति में होता है। उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके मजदूर नयी चीजें बनाता है जो पूँजीपति की संपत्ति बन जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु मजदूर द्वारा किये गए वास्तविक उत्पादन और उसे मिले वास्तविक मेहनताने के बीच का सम्बन्ध है। श्रम अनुबंध की ‘स्वतंत्रता’ के कारण मजदूर जो पाता है, वह उसके द्वारा उत्पादित सामग्री के वास्तविक मूल्य से निर्धारित न होकर उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं से और काम की तलाश में होड़ में लगे मजदूरों की संख्या के अनुपात में पूँजीपति को श्रम-शक्ति की जरूरत से निर्धारित होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि सैद्धान्तिक रूप से भी मजदूर का वेतन उसके द्वारा किए गए उत्पादन के मूल्य द्वारा निर्धारित नहीं होता।
अंशत: पूँजीपतियों की आपसी होड़ के कारण और अंशत: तकनीकी विकास के कारण निजी पूँजी कुछ हाथों में केन्द्रित होती जाती है और बढ़ता हुआ श्रम-विभाजन उत्पादन की लघुतर इकाइयों की कीमत पर वृहत्तर इकाइयों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इस विकास का ही परिणाम निजी पूँजी का एक गुटतंत्र (ऑलीगार्की) है; जिसकी अपार शक्ति को जनतांत्रिक ढंग से संगठित एक राजनीतिक समाज द्वारा भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह एक सच्चाई है क्योंकि विधायिका संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा होता है, जो पूँजीपतियों से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं या दूसरे तरीकों से उनके प्रभावों में रहते हैं। ये पूँजीपति व्यावहारिक तौर पर हर तरीके से निर्वाचकों को विधायिका से अलग कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि जनता के प्रतिनिधि आबादी के दलित-शोषित तबकों के हितों की वस्तुत: पर्याप्त रक्षा नहीं करते। इसके अतिरिक्त, वर्तमान परिस्थितियों में निजी पूँजीपति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूचना के प्रमुख स्रोतों (प्रेस, रेडियो, शिक्षा) पर अनिवार्यत: अपने नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार किसी नागरिक के लिए वस्तुगत निष्कर्षों तक पहुँच सकना या अपने राजनीतिक अधिकारों का सटीक प्रयोग कर पाना अत्यन्त कठिन होता है और वास्तव में अधिकांश मामलों में तो एकदम असंभव होता है।
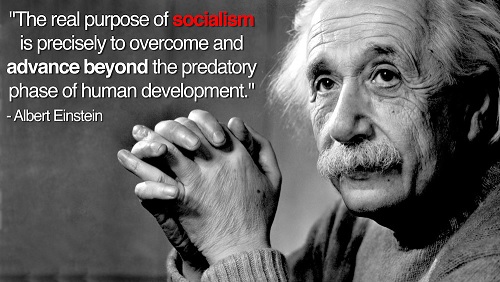
इस प्रकार, सम्पत्ति के निजी मालिकाने पर आधारित अर्थव्यवस्था में मौजूदा स्थिति को दो मुख्य सिद्धान्तों द्वारा स्पष्ट किया जाता है; पहला उत्पादन के साधनों (पूँजी) पर निजी मालिकाना होता है और मालिक जैसे भी ठीक समझें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, श्रम अनुबंध स्वतंत्र होता है। वास्तव में, इस अर्थ में एक शुद्ध पूँजीवादी समाज जैसी कोई चीज नहीं होती। विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि मजदूर लम्बे और तीखे राजनीतिक संघर्षों द्वारा ‘स्वतंत्र श्रम समझौते’ का किंचित सुधारा हुआ रूप, कुछ इस तरह के मजदूरों के लिए पा सकने में सफल हुए हैं, किंतु समग्रता में आज की अर्थव्यवस्था ‘शुद्ध’ पूँजीवाद से बहुत भिन्न नहीं है।
उत्पादन मुनाफे के लिए किया जाता है न कि उपयोग के लिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सक्षम और काम के इच्छुक सभी लोग हमेशा काम पा सकने की हालत में रहें, ‘बेकारों की फौज’ लगभग हमेशा मौजूद रहती है। मजदूर हरदम काम छिन जाने के भय से ग्रस्त रहता है। चूँकि बेकार और बहुत कम वेतन पाने वाले मजदूर एक लाभदायक बाजार नहीं बनाते, इसी से उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन सीमित रहता है, जिसका परिणाम होता है, भयंकर कठिनाई। तकनीकी प्रगति सबके काम का बोझ घटाने के बजाय लगातार और अधिक बेकारी पैदा करती है। पूँजीपतियों के बीच की होड़ के साथ जुड़ा मुनाफे का मकसद ही पूँजी के संचय और उपयोग में अस्थिरता के लिए जिम्मेदार है। यह समाज को उत्तरोत्तर गहन महामंदी की ओर ले जाता है। यह असीमित होड़ श्रम की बड़े पैमाने पर बर्बादी को पैदा करती है और साथ ही व्यक्तियों की सामाजिक चेतना को पंगु बनाती है जिसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूँ।
व्यक्तियों के इस प्रकार पंगु बनाए जाने को मैं पूँजीवाद का सबसे बड़ा अभिशाप मानता हूँ। हमारा सारा शैक्षणिक ढाँचा इस अभिशाप से ग्रस्त है। विद्यार्थी के मन में एक अतिरंजित प्रतियोगी दृष्टिकोण बैठाया जाता है तथा उसे आगामी कैरियर के लिए तैयारी के रूप में धनपिपासु (लोभी) सफलता की पूजा करना सिखाया जाता है।
मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन विकट बुराइयों को समाप्त करने का केवल एक ही रास्ता है, केवल एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है, जिसके साथ-साथ सामाजिक लक्ष्यों से युक्त एक शिक्षा व्यवस्था भी हो। ऐसी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वयं समाज का स्वामित्व होता है और उनका उपयोग नियोजित ढंग से होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन को समायोजित करती है, काम करने में सक्षम लोगों के बीच किये जाने वाले काम को बाँट देती है तथा प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बच्चे को आजीविका की गारण्टी देती है। ऐसे समाज में शिक्षा, व्यक्ति की सहज क्षमता का विकास करने के साथ ही हमारे वर्तमान समाज की सत्ता और सफलता का गुणगान करने की जगह उसके अन्दर अपने जैसे लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने का प्रयास करेगी।
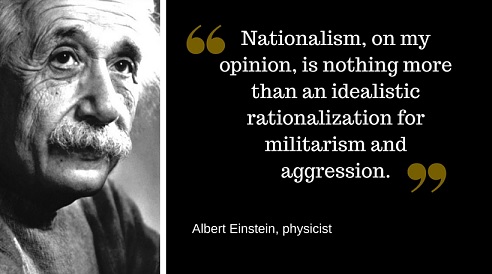
फिर भी, इसे याद रखना जरूरी है कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था ही समाजवाद नहीं होती है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में व्यक्ति पूरी तौर पर गुलाम हो सकता है। समाजवाद की स्थापना कुछ अत्यन्त कठिन सामाजिक-राजनैतिक समस्याओं के समाधान की माँग करती है; राजनैतिक और आर्थिक शक्ति के व्यापक केन्द्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए नौकरशाही को सर्वशक्ति-सम्पन्न व उद्धत होने से कैसे रोका जा सकता है? व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो सकती है और इसके साथ ही नौकरशाही की ताकत को निष्प्रभावी बनाने वाली जनतांत्रिक शक्ति को सुनिश्चित तौर पर कैसे स्थापित किया जा सकता है?
हम संक्रमण के युग से गुजर रहे हैं। समाजवाद के लक्ष्य और समस्याओं के प्रति स्पष्टता इस दौर में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। मौजूदा हालात में इन समस्याओं पर स्वतंत्र और बेरोक-टोक बहस-मुबाहिसे पर सख्त वर्जनाएँ लागू हैं। इसलिए इस पत्रिका की शुरूआत मेरे विचार में एक अहम जन सेवा है।
(महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन का यह लेख 1949 में मंथली रिव्यू पत्रिका के प्रवेशांक में छपा था । )






















