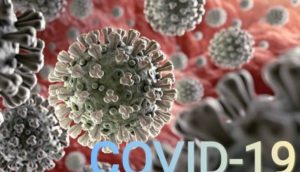सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के महेश व्यास से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि सैलरी पर काम करने वाले 1.8 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। इतनी ही संख्या में छोटे कारोबारियों का कारोबार चौपट हो गया है। दोनों करीब 4 करोड़ होते हैं। आंकड़ा अप्रैल माह का है। इसके अलावा 8 करोड़ वो लोग हैं जो अपने हुनर के दम पर रोज़ कमाते-खाते थे। कांट्रेक्टर पर नौकरी करते थे। कुल मिलाकर संख्या 12 करोड़ होती है। मई में तालाबंदी के क्रमश: नरम पड़ने से इन 12 करोड़ लोगों में 2 करोड़ को फिर से काम मिलने लगा है। यानि तब भी 10 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए। यह संख्या न तो छोटी है और न सामान्य। एक के पीछे अगर आप तीन लोग भी जोड़ लें तो 40 करोड़ लोगों के पास रोज़गार नहीं है।
कितने लोगों की सैलरी आधी हो गई है इसकी गणना उनके पास नहीं थी। लेकिन आप अदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ऐसे 5-6 करोड़ लोग भी होंगे तो कुल 50-60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी चली गई है, जिनमें से कुछ की सैलरी आधी हो गई है औऱ जिनका काम छिन गया है। हमारी आबादी के 60 करोड़ लोगों का उनकी तीन महीने की ज़िंदगी से नाता टूट गया है। मुमकिन है कि तब भी हमें आस-पास में ऐसे लोग न मिलते हों या दिखते हों जिनका काम बंद हो गया है। लेकिन यह तो इस वक्त की सच्चाई है। हमारे आस-पास के लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। कोई पुराना राग-द्वेष हो तो उसे भी भूल जाइये। जब सबका ही चला गया हो तो किस बात का ग़म औऱ किस बात का रंज। किस बात का हिसाब या किस बात का फ़ैसला। माफी मांग लीजिए। माफ कर दीजिए।

एक ऐसे समय और समाज में जब सब कुछ अनिश्चित हो गया हो, स्थगित हो गया है और समाप्त जैसा हो गया हो उस समय और समाज की भाषा क्या होनी चाहिए। मैं लगातार इस सवाल पर सोच रहा हूं। सामाजिक आचार-व्यवहार की भाषा पहले की तरह नहीं हो सकती है। उसे बदलना होगा। हमें नए सिरे से अपने वाक्यों को संयोजित करने की ज़रूरत होगी। हमारा बोला हुआ कुछ भी इस तरह से न हो जिससे ये 60 करोड़ लोग और विस्थापित हो जाएं। उनके मन का अवसाद गहरा हो जाए। क्रोध उग्र होने लगे। तंज और व्यंग्य को लेकर भी अतिरिक्त सावधान रहना होगा। इसके लिए सोच बदलने की ज़रूरत होगी। अपने संबंधियों, मित्रों और परिचितों या फिर किसी अनजान से भी बातचीत करते समय अतिरिक्त रूप से सतर्क रहें। आपकी सह्रदयता, आपका प्यार किसी में जान डाल देगी। मुरझाये पौधे में जैसे खाद डालने के बाद छोटा सा हरा पत्ता निकल आता है।
एक ऐसी भाषा को गढ़ने की आवश्यकता है जो सबको बराबर की जगह दे। सबको सहज रूप में स्वीकार करे। लगे कि कोई अपना रहा है। दुत्कार नहीं रहा है। इस भाषा में सुनने की क्षमता ज़्यादा हो। कहने की थोड़ी कम। शायद कोई चाहता होगा कि इस हालत में कोई बिना कहे समझ सके। उसकी बातों को स्वीकार कर सके। हम सबकी आपस की भाषा कुछ होने का अभिमान या कुछ न होने की हीनता से मुक्त हो। सहारा देती हो। किसी को कंधा देती हो। कोई बहुत क्रोधित है तो सुन लीजिए। कोई बेचैन है तो सुन लीजिए। यह वक्त कम से कम बुरा मानने का है। भाषा सिर्फ ज़ुबान पर बरती जानी वाली चीज़ नहीं है। इसमें आपका पहनना-ओढ़ना भी शामिल है। मैं नहीं कहता कि शोकाकुल माहौल का निर्माण करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि सादगी होनी चाहिए। जिससे किसी को कमतर होने का अहसास न हो और न किसी को बेहतर होने का अहंकार।
पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। पर कई बार लग रहा है कि इस वक्त में हमें नई सार्वजनिक भाषा का निर्माण करना चाहिए। यह ख़्याल आया उन लोगों की तस्वीरों को देख कर जो देश के कोने-कोने में फैले हैं। जिनका कोई नाम नहीं है। जिनके पास अकूत संपत्ति नहीं है। लेकिन वो सड़क पर हैं। लोगों को खाना खिला रहे हैं। पैसे दे रहे हैं। ये कितने शानदार लोग हैं। इन लोगों ने इस वक्त में एक नई भाषा गढ़ी है। समाज के ख़्याल की भाषा। इनके काम में वो ख़्याल था कि कोई भूखा न रहे। भले हमारा बैंक बैलेंस कुछ कम हो जाए। हम कभी इन अनगिनत शानदार लोगों का एहतराम नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया अदा नहीं कर पाएंगे और न किसी हिसाब में दर्ज कर पाएंगे। फिर भी इन लोगों ने काम किया। उनके निस्वार्थ काम की तस्वीरों को देखते हुए लगा कि यही नई भाषा है। इसी नई भाषा में संभावना है। हम सबको सार्वजनिक और व्यक्तिगत रुप से बोले जाने वाली भाषा पर विचार करना चाहिए। यह नई भाषा आलिंगन करने वाली हो, आहत करने वाली न हो।

यह वक्त हमें अवसर दे रहा है। हमने पिछले वर्षों के दौरान भाषा में जिस आक्रामकता को जगह दी है, उसे विदा कर देने का असवर आया है। किसी अच्छे और विनम्र कवि की तरह बोलने की रवायत कायम हो। मैं इन दिनों जब तब कुंवर नारायण की कविता पढ़ने लगता हूं। मालूम नहीं क्यों मुझे लगता है कि यह कवि नई भाषा के दरवाज़े तक ले जा सकता है। विनम्रता का आग्रह और गुमनाम रहने का अभ्यास कराती है इनकी भाषा। काश हमारी राजनीति, समाज सब मिलकर किसी कवि की भाषा को सार्वजनिक रूप से स्थापित करते। कितना बेहतर होता। हमारे आपके पास कम होता मगर हम और आप कमतर महसूस न करते।
न्यूज़ चैनलों ने भाषा की सार्वजनिक मर्यादा को ध्वस्त कर दिया है। पहले यह इल्ज़ाम राजनीति पर आता था। लेकिन चैनलों की भाषा ने भाषा क्षेत्र की सार्वजनिक मर्यादाओं को कुचल दिया है। मैं इसमें किसी को अपवाद नहीं मानता। जब पहली बार कहा था कि टीवी मत देखिए। तो हवा में नहीं कहा था। मैं देख रहा था कि चैनल भाषा को ध्वस्त कर रहे हैं। एक ऐसी भाषा गढ़ रहे हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे वैसी भाषा बोलें। आप भी कितना बदल गए। आप खुद पब्लिक स्पेस में लिखी गई अपनी भाषा को देखिए। इसलिए न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दीजिए। उनमें वैसे भी खबरें नहीं होती हैं। अखाड़ा होता है। वही जो ट्विटर की टाइम लाइन में नहीं होता है।
मैं क्यों इस बात पर बार बार लौट कर आता हूं कि न्यूज़ चैनल न देखें, शायद इसीलिए। चैनलों की पत्रकारिता में अच्छे लोग हैं, मगर चंद अपवादों के सहारे आप शहर के सारे गुंडों को देवता घोषित नहीं कर सकते। यह माध्यम ऐसा ही रहेगा। इसलिए आप इसे छोड़ दें। ये चैनल आपकी भाषा खत्म कर रहे हैं। आपकी सामाजिकता ख़त्म कर रहे हैं। आप खुद मेरी बातों को परखा कीजिए। जब आप टीवी देख रहे होते हैं। मैं नहीं कहता कि बिना जांचे परखे मेरी बात मान लें। अगर आप खुद को, अपने परिवार को दूसरों से बेहतर मानते हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है आपकी उस भाषा का जो अब है नहीं। बेशक उस भाषा में कई प्रकार की जड़ताएं थीं। कहां तो हमें या आपको उन जड़ताओं से भाषा को आजाद कराना था, उल्टा आप उनमें कैद कर दिए गए। आपको लगता होगा कि है लेकिन वो आपकी सोच और आपकी लिखावट से जा चुकी है। आप जब न्यूज़ चैनलों से दूर रहेंगे, व्हाट्स एप की भाषा से दूर रहे होंगे तो यकीन जानिए आपके भीतर कुछ अच्छा घटेगा। आज़मा कर देख लीजिए।

रवीश कुमार जाने-माने टीवी पत्रकार हैं। संप्रति एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर हैं। यह लेख उनके फेसबुक पेज से लिया गया है।