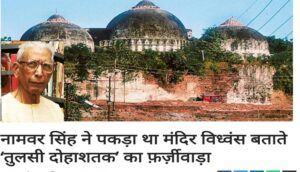पुण्य प्रसून वाजपेयी
खलक खुदा का , मुलुक बादशाह का / हुकुम शहर कोतवाल का / हर खासो-आम को आगाह किया जाता है / कि खबरदार रहें/ और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से /कुंडी चढाकर बंद कर लें / गिरा ले खिड़कियो के परदे/ और बच्चों को सड़क पर न भेजें/ क्योंकि, एक बहत्तर बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कमजोर आवाज में / सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है….
44 बरस पहले 1974 में धर्मवीर भारती ने ‘मुनादी’ नाम से ये कविता तब लिखी जब सत्ता के घमंड में चूर इंदिरा की तानाशाही चरम पर थी और जेपी देश में अलख जगाने निकल पड़े थे। उस वक्त इंदिरा की सत्ता चापलूसों से कुछ इस तरह घिरी हुई थी कि इंदिरा को भ्रष्टाचार में भी ईमानदारी दिखायी देती थी। दमन करने में राष्ट्रीय भावना। और उस वक्त भी विपक्ष की राजनीति शून्य में समायी हुई थी। तब जेपी खड़े हुये थे। और फिर धीरे धीरे कैसे उनके पीछे छात्र-युवा से लेकर राजनीतिक कार्यकत्ता जुडते गये और स्वयंसेवकों की टोली भी जुडने लगी, ये अब इतिहास है।
इतिहास के इन पन्नों को पलटते वक्त जो आहट सुनाई दे रही है, वह ज्यादा क्रूर तरीके और सत्ता की मद में चूर होकर जिस इतिहास रचने की है, वह सिर्फ संकेत भर है कि आने वाले वक्त में हालात और खराब होंगे। इमरजेन्सी की बाजी जनता पार्टी ने पलटी थी और उसी जनता पार्टी से निकले नायक इमरजेन्सी से भी बुरी बाजी चलने से बाज आ नहीं रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में सत्ता का कौन सा चेहरा दिखायी देगा, या वह कितना क्रूर होगा, ये सिर्फ कल्पना की जा सकती है। क्योंकि सभी सत्ता पाने के रास्ते ही सारे दौड़ लगा रहे हैं और जनता एक त्रासदी को भोगते हुये दूसरे त्रासदी को भोगने के लिये खुद को तैयार कर रही है। यानी आजाद भारत में सत्ता की उम्र तले सत्ताधारियों की उम्र ढल जाती है, और नई पीढ़ी विरासत की सोच संभाले सत्ता पाने के लिये दौड़ती नजर आती है। 44 बरस पुराने संघर्ष के नायक आडवाणी आज अकेले अंधेरे में कैद है…. मुरली मनोहर जोशी खामोशी की तरंगों में खोये हुये हैं। जार्ज फर्नाडिंस डिमेन्शिया बीमारी तले सबकुछ भूल चुके हैं। यशंवत सिन्हा सुनसान सड़क पर हंगामा खड़ा करने के मकसद को लगातार टटोल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की खलनायकी से लेकर नायकी तक दांव पर है। कांग्रेसी या क्षत्रपों में इतनी ताकत नहीं नहीं कि सत्ता गंवाने के बाद सत्ता पाने के लिये संघर्ष करते हुये दिखायी देने के अलावे कुछ कर सकें ।
इस फेहरिस्त में नीतीश कुमार नतमस्तक हैं। पासवान अपनी विरासत को अपनी ही पीढियों के बंदोबस्त में डूबे हुये हैं। राजनाथ सिंह से लेकर रविशंकर प्रसाद और अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी में राजनीतिक नैरेटिव सिर्फ अपनी सफलता दिखाने या सत्ता पाने के हर तरीके को अपनाने के आगे जाती नहीं। लकीर महीन पर ये समझने की जरुरत है कि आखिर क्यों किसी नेता में नैतिक बल नहीं है कि वह सड़क पर इस मुनादी के साथ निकल पड़े कि अब राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जरुरत है। यानी 72 की उम्र पार कर चुके पूर्व के नायकों में इतनी जिन्दगी नहीं कि वह कुछ बोल भी सके। और आजादी के बाद जन्म लेने वाली पीढी सत्ता संभाले हुये या सत्ता पाने की होड में मान कर चल रही है कि उसके हाथों नये भारत का सपना जन्म ले ही लेगा। और सत्ता का घमंड इतनी तीक्ष्ण है कि अमित शाह कहने से नहीं चुकते अदालतों को मर्यादा में रहकर फैसले देने चाहिये। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को गठबंधन की सत्ता देश को कमजोर करने वाली और बहुमत की मोदी सत्ता ताकतवर होकर देश को ताकतवर बनाने वाली नजर आती है । तो वित्त मंत्री अरुण जेटली तो चुनी हुये सत्ता को ही देश मान लेते हैं। और इस बोल के पीछे के सच को समझे तो देश के हर संस्था हर संवैधानिक संस्थान। हर अधिकारी, हर कारोबारी और हर प्रभावी व्यक्ति को सत्ता के पक्ष में खडे होने की तमीज होनी चाहिये, समूची व्यवस्था यही बनाने की कोशिश हो रही है। यानी बहस-चर्चा या फिर सवाल उठने नहीं चाहिये। और जनता ने पांच बरस के लिये चुना है तो सत्ता के ही ऐसे किसी फैसले या निर्णय पर अंगुली उठाने का अधिकार किसी को होना नहीं चाहिये, चाहे सत्ता के वो निर्णय संविधान की ही घज्जियां क्यों ना उड़ाता हो ।
तो असल सवाल यहीं से शुरु होता है कि आखिर इस देश में सड़क पर नंगे पांव जेपी की तर्ज पर निकलने वाले भी खत्म क्यों हो गये। युवा तबके का संघर्ष सत्ताधारियों या सत्ता पाने के लिये नारे लगाने में गुम क्यों हो जा रहा है। और किसी भी मुद्दे पर देश एकजूट होकर ये फैसला देने की स्थिति में क्यो नहीं आ पा रहा है कि भविष्य के बेहतर भारत के लिये ही सही पर चंद दिनों तक रोजी-रोटी छोड़ कर सड़क पर ही निकल जाये और पटरी से उतर चुकी राजनीतिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जाये। यानी समाज के भीतर की एकजूटता खत्म कैसे हो गई? किसने कर दी? सारे सवाल सूचना तंत्र के बंटे हुये मंत्रो के आसरे गूंजते तो हैं पर असरकारक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और सारी बहस इसी पर क्यों आ टिकती है कि 2019 में तो आजादी मिल ही जायेगी तो उसी में लग जाया जाये! यानी आजादी ने 71 बरस बाद लोकतंत्र का मतलब सत्ता परिवर्तन से सत्ता हस्तांतरण और एक वोट से एकमुश्त वोट से आगे बढ़ नहीं पाया। और बढ़ा भी तो अंग्रेजों की गुलामी के वातावरण को ही सत्ता के आत्मसात करने वाले हालात विकसित हो गये। यानी कानून सिर्फ आम जनता के लिये और कानून पर राज सत्ता का। यानी संविधान और कानून के राज को ही गुलाम बनाकर लोकतंत्र को जीने का भाव इसलिये विकसित होते चला गया क्योंकि चुनाव जिस तंत्र तले आ खड़ा हो गया वह दबंगई चले बूथ लूट से निकला जरुर। पर धीरे् धीरे वोट को खरीदने और वोटरो को बांटने के सामानांतर सत्ता के ही अपराधी होने पर जा टिका। और सत्ता के लिये अपराधी होने का मतलब यही हो गया कि कानून की नजर में जो भी जायज नहीं है, वह सत्ता के लिये होने वाले चुनाव में जायज होगा ।
लेकिन लोकतंत्र का कवच बरकरार रखना है तो फिर नागरिक और उसके वोट की ताकत को महत्व देना जारी रखा गया। तो सुधार से पहले हालात को समझ लें। अपराधी होना पहले सत्ता से सौदेबाजी करने की ताकत देता है फिर सत्ताधारी बना देता है । भ्रष्ट या लूट के आसरे कालाधान या बेशूमार धन को समेटे व्यक्ति से पहले राउंड में सत्ता सौदेबाजी करती है फिर अपने साथ खड़ा कर लेती है । मुनाफे के इस खेल में जाति भी इसी बिसात को बिछाती है और धर्म भी सियासी बिसात के लिये प्यादा बन जाती है । तो बदलाव लाये कौन और पहल हो कहाँ से? जबकि किसान के नाम पर आंदोलन, महिला सुरक्षा को लेकर गुस्सा, बेरोजगारी को लेकर आक्रोश, छोटे व्यवसायियो के संकट के नाम पर विरोध जारी है। तो संकट में सभी हैं लेकिन सभी मिलकर तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि सत्ता की राजनीति करने वालो को धूल कैसे चटायी जाये। संघर्ष का पैमाना सत्ता को हराने वाले के साथ अलग अलग तरीके से जुडने के अलावे कुछ बच नहीं रहा है। यानी मोदी से आजाद होकर गठबंधन की गुलामी का सुकुन हर कोई पाले हुये है। और लगातार बदलते संभलते हालात संकेत भी दे रहे है कि सत्ता के घमंड को चूर चूर करने की तैयारी में हर तबका है पर खामोश है। और खामोशी के परिणाम बेहद प्रभावी होते हैं, ये इंदिरा समझ नहीं पायी तो मोदी भी कैसे समझेगे! लेकिन लोकतंत्र को ही अगर राजनीतिक इकनामिक माडल में बदला जा चुका है तो इसका दूसरा पहलू यही है कि 2019 के बाद कुछ नये चेहरे होंगे। कुछ नये मोहरे होंगे। कुछ नये रईस होंगे। कुछ नये तबके होंगे। कुछ नये समुदाय होंगे। और अभी की भगवा ब्रिग्रेड को सजा तब जरुर मिलेगी । क्योंकि लोकतंत्र हमेशा खुद को विस्तार देता है तो मोदी का पाठ राहुल गांधी ने पढ़ लिया है । संघ का मोदी राग भी काग्रेस समझ चुकी है। यानी सत्ता बदल रही है पर इस बदलती सत्ता में जनता कहाँ है, और आने वाले वक्त में देश का आम नागरिक कहाँ होगा? ये सवाल क्यो गायब हैं। या फिर कैसे 2013-2014 में जो मनमोहन सिंह खलनायक लगते थे और जो मोदी नायक लग रहे थे, 2018 में वही मोदी खलनायक लगने लगे हैं। पीएम मनमोहन फिर बनेगें नहीं लेकिन देश की आर्थिक नीतियो को लेकर वह नायक लगने लगे हैं।
दरअसल यही से सवाल उठता है कि हमे क्यो नहीं पता है कि हमारी आर्थिक नीतिया कैसी होनी चाहिये। हम क्यों तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के गौरवमयी अतीत को भूल चुके हैं? क्यों गांव पर टिका भारत हम भूलाते जा रहे है और गांव खत्म कर स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में बढ चुके है? क्यों भारत में शारीरिक श्रम को महत्व नहीं और शिक्षा महत्वहीन हो चली है? क्यों परिवार खत्म हो रहे हैं और क्यों सरोकार खत्म कर तकनीक के आसरे देश चलाने की दिशा में देश बढ़ चला है? क्यों रुस का साथ छूटा और अमेरिका के मुरीद हो गये? क्यों चीन के सामने भारत नतमस्तक दिखायी दे रहा है? क्यों हर मुद्दे के पीछे पाकिस्तान को देखकर भावनाओं को उभारा जा रहा है और क्यों सत्ता हिन्दु मुस्लमान में अटक जाती है? क्यों सार्क देशो को 2014 में शपथग्रहण में बुलाकार दोस्ती के विस्तार की बात होती है और 2019 से पहले ही नेपाल, मालदीव, भूटान, श्रीलंका तक भारत से दोस्ती छोड चीन के पाले में खड़े नजर आते हैं?
समझना जरुरी है कि अगर सत्ता सिर्फ सत्ता बनाये रखने के लिये है और राजनीतिक सत्ता की हथेली पर ही देश को नचाने की सोच है तो फिर हर कोई हर दूसरे को अपनी हथेली पर नचाने की निकलेगा। फिर लोकतंत्र का हर पिलर यही काम करेगा। और चौथा स्तम्भ मीडिया भी तो नचायेगा ही …तो फिर सड़क पर कौन सच बोलते हुये निकलेगा? और कैसे विकल्प बनेगा और जो सवाल जीरो बजट की राजनीति का है वह कैसा होगा, ये अगले लेख में।
लेखक वरिष्ठ टीवी पत्रकार हैं।