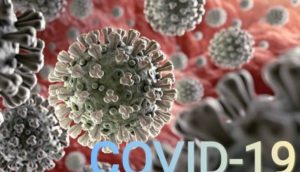निस्संदेह, देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की सबसे ज्यादा कीमत प्रवासी और दिहाड़ी मजदूर ही चुका रहे हैं. लॉकडाउन न सिर्फ उनकी रोजी-रोजगार निगल गया है, बल्कि ‘जहां और जैसे हैं, वहीं और वैसे’ पड़े रहने के लिए जरूरी सिर छुपाने की जगहें भी उनसे छिन गई हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हमदर्दी बरतने की कई अपीलों के बावजूद उनके नियोजकों ने उनसे पूरी तरह मुंह फेर लिया और ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का ‘सिद्धांत’ लागू कर दिया है, जिसके चलते उनके सामने पेट भरने तक के लाले हैं और वे किराया न चुका पाने के कारण मकान मालिकों का कोप झेलने को भी अभिशप्त हैं. दूसरी ओर उन्हें राशन देने व राहत पहुंचाने की सरकारी घोषणाओं का कड़वा सच यह है कि लॉकडाउन के डेढ़ महीने बाद भी उनकी व्यवस्थित घर वापसी तक का इंतजाम नहीं हो पाया है.
उनमें जो थोड़े से ‘सौभाग्यशाली’ हैं, उन्हें स्पेशल ट्रेनों और बसों में भले ही जगह मिल जा रही है, ज्यादातर कई-कई गुना किराया अदाकर मवेशियों की तरह ट्रकों वगैरह में, और नहीं तो जलती सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं. सरकारें उनके लिए सड़कों को भी निरापद नहीं बना पा रहीं और उनमें से कितने ही रास्तों में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हादसों में जानें गंवा रहे हैं. घर पहुंच जाने पर भी उनकी मुसीबतों का अंत नहीं हो रहा. महामारी को लेकर फैलाये गये जिन भयों व भ्रमों ने उन्हें उनके प्रवासस्थलों पर अवांछनीय बना रखा है, अज्ञान के कारण उनसे कुछ ज्यादा ही आतंकित उनके ग्रामीण परिजन भी उनसे आत्मीयता नहीं बरत रहे. तिस पर वहां उनके लिए बनाये गये क्वारंटीन सेंटर कई मायनों में यातनागृहों से भी बदतर हैं.

जो राज्य सरकारें अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत सुधारने के लिए उद्योग-धंधों को फिर से शुरू करने में उनकी अनिवार्य भूमिका के मद्देनजर उनको ‘बेकार’ यात्रा से बचने और वहीं जमे रहने का प्रस्ताव दे रही हैं, वे भी उनकी गुजर-बसर को लेकर रहमदिली से बात करने को तैयार नहीं हैं. इनमें एक नाम कर्नाटक का भी है, जिसने अपने बिल्डरों के हित में मजदूरों को रोके रखने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रद्द कराईं, तो इस सवाल का जवाब देना भी गवारा नहीं किया कि क्या मजदूर संसाधन मात्र हैं? अगर नहीं तो उनकी संवेदनाओं को कुचलकर महाविपदा के वक्त भी अपने परिजनों के बीच जाने की उनकी लालसा को बेकार करार देकर उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह रोके रखना कितना अमानवीय है?
विडम्बना देखिये कि जब इतना सब झेल रहे मजदूरों को थोड़े ढाढ़स और सहानुभूति वगैरह की दरकार थी, सरकारों ने मजदूर विरोधी आर्थिक सुधारों के उस एजेंडे को आगे कर दिया है, जो 24 जुलाई, 1991 को तत्कालीन पीवी नरसिंहराव सरकार द्वारा पूंजी को ब्रह्म और मुनाफे को मोक्ष मानने वाली भूमंडलीकरण की जनविरोधी नीतियों के प्रवर्तन के वक्त ही उनकी अनिवार्य परिणति माने जा रहे थे. लेकिन तब से अब तक आई कई सरकारें उनकी दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने का साहस इसलिए नहीं दिखा पाईं क्योंकि तब वे उन सुधारों के तथाकथित मानवीय चेहरे की बात भी किया करती थीं और निर्लज्जतापूर्वक उसकी ओर पीठ कर लेना उन्हें थोड़ा असुविधाजनक लगता था.
लेकिन अब, जब हमारे सामने कठिन कोरोनाकाल उपस्थित है और सारे तबकों के मिलकर उससे लड़ने की जरूरत जताई जा रही है, देखकर हैरत होती है कि प्रधानमंत्री भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हीं आर्थिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और कई राज्य सरकारों ने उनसे भी ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए मजदूरों को संरक्षण देने वाले कानूनों और प्रावधानों को स्थगित या रद्द करना शुरू कर दिया है.

उनके इन कदमों के बाद उद्योगपति मजदूरों की बेहतरी के ज्यादातर कानूनों के पालन के लिए बाध्य नहीं रह जायेंगे. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में तो भवन व निर्माण श्रमिक कानून, बंधुआ मजदूरी विरोधी कानून और श्रमिक भुगतान कानून की पांचवीं अनुसूची को भी ताक पर रखा जा रहा है. इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिक अनुबंध कानून, औद्योगिक विवाद कानून और इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऐक्ट को निरस्त कर दिया है. गुजरात, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों भी ऐसे मजदूर विरोधी कदमों में पीछे नहीं हैं.
राज्य सरकारों के इन कदमों के बाद उपयुक्त कानूनों के अभाव में काम की जगह या फैक्ट्री में शौचालय, सफाई या वेंटिलेशन न होने पर किसी उद्योगपति पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. किसी मजदूर की तबियत खराब होती है तो फैक्ट्री के मैनेजर को संबंधित अधिकारियों को सूचित नहीं करना होगा. औद्योगिक इकाइयां अपनी सुविधा और शर्तों के हिसाब से मजदूरों को रख और निकाल सकेंगी. बदहाली में काम करने का न तो श्रमिक अदालतें संज्ञान लेंगी और ना ही दूसरी अदालतों में इसको चुनौती दी जा सकेगी. कई राज्यों में अब बदली हुई परिस्थितियों में मजदूरों को 12 घंटे की पाली में काम करना पड़ेगा.
क्या आश्चर्य कि कई मजदूर नेता इसे मजदूरों के जले पर नमक की तरह देख रहे और पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने चौथे संदेश में आपदा को अवसर में बदल देने की जो बात कही, अगर वह सारे अवसर उद्योगपतियों के नाम कर देने की दिशा में बढ़ने की कवायद है तो उससे देश का कितना भला होना है? इस तरह तो उनके भारत की आत्मनिर्भरता के मिशन का अर्थ भी यह हो जायेगा कि सर्वाइवल आफ द बेस्ट की इस व्यवस्था में जरूरतमन्द तबकों को सरकार के भरोसे कतई नहीं रहना चाहिए और खुद पर ही निर्भर करना चाहिए. मजदूर संगठन यहां तक डरे हुए हैं कि अब देश के मजदूरों को औद्योगिक क्रांति से पहले के हालात में काम करना पड़ सकता है.

यहां सरकारों का पक्ष समझें तो चूंकि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही खस्ताहाल है, उम्मीद के अनुरूप विदेशी निवेश आ नहीं रहा और कोरोना द्वारा पैदा की गई कोढ़ में खाज की स्थिति के कारण देशी उद्योगपतियों का रवैया भी ढुलमुल है, वे आगे चलकर भयावह पूंजीसंकट के अंदेशे से डरी हुई हैं. इस डर के ही वशीभूत होकर वे निवेशकों को खुश करने के लिए हमेशा उनकी असुविधा का कारण रहे मजदूर हितैषी कानूनों को समाप्त या स्थगित करने के पक्ष में तर्क दे रही हैं. वे समझती हैं कि इससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा, जिसके बूते अर्थव्यवस्था में नये प्राण फूंके जा सकेंगे.
काश वे समझतीं कि स्थिति का दूसरा पहलू उन्हें नयी उलझनों के हवाले कर सकता है. इन कानूनों के न रहने पर निरंकुश उद्योगपतियों ने श्रमिकों का अंधाधुंध शोषण आरम्भ किया तो कहना मुश्किल है कि उनका असंतोष कौन-सा रूप ले ले और औद्योगिक वातावरण को कैसी अशांति की ओर ले जाये. देश की औद्योगिक राजधानी मुम्बई समेत अनेक महानगरों में उनका रह रहकर फूट रहा गुस्सा अभी से इसका संकेत दे रहा है.

जाहिर है कि वे समझ चुके हैं कि कोरोना का संकट आते ही उनके सामने न घर के और न घाट के वाली जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसके पीछे भूमंडलीकरण की नीतियों के बाद आये उनके विरोधी और उद्योगपति हितैषी ठेका मजदूरी जैसे कानूनी प्रावधान ही हैं. एक दिन वे यह भी समझ ही जायेंगे कि उनकी वास्तविक दुश्मन ये नीतियां ही हैं, जिन्हें विकल्पहीन मानकर देश की प्रायः सभी राजनीतिक पार्टियां और सरकारें उनके समक्ष नतमस्तक हैं. ऐसा नहीं होता तो इन श्रम सुधारों {पढ़िये: बंटाधारों} को लेकर कांग्रेस की राजस्थान व पंजाब सरकारों का रवैया भी उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात की भाजपा सरकारों जैसा ही क्यों होता?
सारी सामाजिक सुरक्षाओं और कल्याणकारी नीतियों की दुश्मन इन्हीं नीतियों के चलते आज मजदूर इतने मजबूर हैं कि न संकट की इस घड़ी में नियोजकों के मुंह फेर लेने का प्रतिकार कर पा रहे हैं, न ही सरकार उनका इतना दबाब महसूस कर रही है कि नियोजकों को अपने उद्यम फिर से संचालित करने के लिए उनके हितों से समझौते की छूट न दे.

कृष्ण प्रताप सिंह – लेखक, वरिष्ठ हिंदी पत्रकार हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रहते हैं।
हमारी ख़बरें Telegram पर पाने के लिए हमारी ब्रॉडकास्ट सूची में, नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए आप शामिल हो सकते हैं। ये एक आसान तरीका है, जिससे आप लगातार अपने मोबाइल पर हमारी ख़बरें पा सकते हैं।