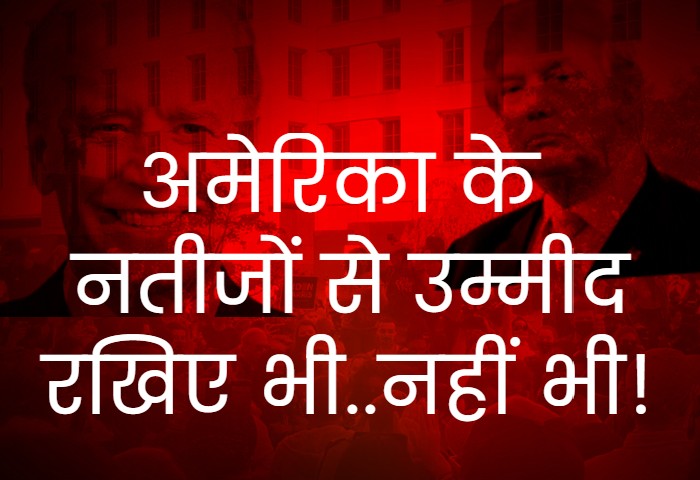तो अन्तः विश्व के शक्तिशाली और चरम पूंजीवादी देश अमेरिका ने अपना फैसला सुना दिया है. वहां के करोड़ों मतदाताओं ने डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को देश का 46वां राष्ट्रपति चुन लिया और छिछोरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ‘व्हाइट हाउस’ (राष्ट्रपति निवास) से बाहर कर दिया है. यह दो व्यक्तियों की हार-जीत नहीं है बल्कि पूंजीवादी निज़ाम के भीतर दो प्रवृतियों के बीच हुई जंग का फैसला है. बाइडेन और ट्रम्प, दोनों ही पूंजीपति हैं और पूंजीवाद के समर्थक हैं…निरंकुश पूंजीवाद और उदार पूंजीवाद के बीच भी द्वंद्व रहता आया है. इन चुनाव परिणामों के राजनीतिक -आर्थिक प्रभाव सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेंगे, शेष विश्व पर भी पड़े बगैर नहीं रहेंगे.
पिछले कुछ वर्षों से चरम पूंजीवाद की गरम हवाएं चल रही हैं. कॉर्पोरेट पूंजीवाद ने निरंकुशता, अधिनायकवाद, नस्लवाद, आतंकवाद, धार्मिक-मज़हबी कट्टरता, सैन्य उपासना, युद्धोन्माद, उग्र राष्ट्रवाद, आत्मग्रस्तता, हठधर्मिता, छिछोरपन, जन के प्रति राज्य -संवेदनहीनता, नागरिक अधिकारों का हनन, उत्तर सत्य राजनीति व मीडिया, वैधानिक व लोकतान्त्रिक संस्थाओं का छिछलाकरण जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है. अमेरिका के अलावा, रूस, चीन, फ्रांस, टर्की और कतिपय दक्षिण अमेरिकी व अफ़्रीकी देशों में ऐसी प्रवृतियों के ध्वजावाहकों को राष्ट्रपतियों-प्रधानमंत्रियों के रूप में देखा जा सकता है. ऐसे शासक जनता को इन प्रवृतियों के मायाजाल में फंसा कर संवैधानिक सीढ़ियों से चढ़ कर सत्तासीन होते रहे हैं; हिटलर व मुसोलिनी सबसे बड़े उदाहरण हैं. जब भी विरोधी हवाएं चलने लगती हैं, विदेशी संकट, ज्ञात -अज्ञात दुश्मन, चरम सांस्कृतिक व धार्मिक राष्ट्रवाद का नारा उछाल देते हैं. अमेरिका के पांचवें दशक में ‘मैकार्थीवाद‘ चलाया और ‘रूसी आ रहे हैं‘ का नारा लगा दिया. यहाँ तक कि फ़िल्में भी बनीं. हमारे यहाँ भी यही हुआ. पिछले छः सालों में जंग व आतंकवाद पर बनी फिल्मों से राज्य समर्थक नैरेटिव तैयार किया गया. प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात-नई दिल्ली यात्रा का अफसाना अलग तो नहीं है. ट्रम्प की मेलो-ड्रामा कहानी सर्वविदित है. चीन व रूस के शिखर नेताओं की यात्रा कथा भी तो यही है. मार्क्सवाद ने कब कहा है कि ताउम्र राष्ट्रपति रहें? दोनों देशों के नेता साम्यवादी विरासत के वारिस माने जाते हैं. बेलारूस में वहां के राष्ट्रपति के विरुद्ध अब भी जन-आंदोलन जारी हैं..
वास्तव में ट्रम्प सहित अन्य नेताओं ने ‘चरमवाद और छिछोरपन‘ का लगातार सहारा लिया है और सत्ता में स्वयं को जमाये रखा. कोई मोदी जी से पूछे कि उन्होंने अमेरिका में ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार‘ का नारा लगवा कर क्या अपने छिछोरेपन का परिचय नहीं दिया है? क्या दूसरे देश में जाकर ऐसा प्रचार करना प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पतनीकरण करना नहीं है? क्या इससे ‘राजनयिक शिष्टाचार‘ भंग नहीं हुआ है? कल को दिल्ली आ कर बाइडेन भी किसी विपक्षी नेता के लिए प्रचार करना शुरू करें तब कैसा रहेगा? ट्रम्प ने भी भारत में आ कर यही किया. दोनों नेताओं ने सर्वसम्प्रभुता संपन्न राष्ट्रों की राजनयिक मर्यादाओं को तोड़ा.
कॉर्पोरेट पूंजीवाद के समर्थक नेताओं को यह समझना चाहिए कि ‘चरमवाद व उग्रवाद‘ जनता का स्थाईभाव नहीं होता है, दूध में उबाल की भांति ज़रूर होता है, और वह भी शासक वर्ग द्वारा गढ़े गए नैरेटिव से अनुकूलित होता रहता है. क्या आज के जर्मनी व इटली में फासीवादी-नाजीवादी हिटलर व मुसोलिनी के लिए 1935 -45 जैसा प्यार का तूफ़ान उमड़ेगा? इन देशों की कई यात्राओं में हुए अनुभवों के आधार पर यह लेखक इस सोच की तस्दीक कर सकता है..
अमेरिकी चुनाव परिणामों से यह भी साफ़ हो गया कि देशी-विदेशी नारा भी बेरंग हो गया है. भारतीय मूल की कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद पर चुना जाना, इस बात का सबूत है कि दुनिया अब अधिक समय तक नस्ल, रंग, धर्म, एकल संस्कृति से चिपके रहने से इंकार करती है. यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने 2004 में ज़िद्द की थी कि यदि सोनिया गाँधी प्रधानमंत्री बनी तो वे अपना केश मुड़वा कर रहेंगी क्योंकि विदेशी मूल का व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? यदि अमेरिका का बहुसंख्यक श्वेत समाज कहने लगे कि कमला भारतीय मूल की हैं. वे हमारी उपराष्ट्रपति कैसे हो सकती हैं? तब क्या होगा? जब पूँजी का भूमंडलीकरण हो सकता है तो मूल वंश-नस्ल-धर्म-संस्कृति का क्यों नहीं हो सकता? एक नए प्रकार की राजनीतिक सभ्यता जन्म लेने के लिए मचल रही है. प्रोद्योगकी व सूचना क्रांति ने दुनिया को सिकोड़ दिया है, एक विराट परिवार का भाव पैदा होने लगा है. भारत में लोगों ने अमेरिकी चुनावों को बेहद दिलचस्पी से देखा है. इस हार-जीत में स्वयं के उतार-चढ़ावों को भी देखा है. क्यों इस हार-जीत में उत्सव-शोक के भाव घुले रहे हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ प्रभावित होती हैं. क्यों हम विभिन्न देशों में होने वाले राजनीतिक घटनाओं- आन्दोलनों से प्रभावित होते हैं? क्योंकि अब दुनिया एकलवादी नहीं हो सकती है. अब सांस्कृतिक -धार्मिक सनकों व हठधर्मिता के आधार पर किसी भी देश को लम्बे समय तक हांका नहीं जा सकेगा.
यह सही है, इस हार-जीत से अमेरिका का मूल पूंजीवादी -वर्चस्ववादी चरित्र यथावत रहेगा. अलबत्ता इसमें सतही या दिखावटी परिवर्तन आ सकता है. लेकिन इतना तय है कि इससे उदारवादी वातावरण के निर्माण में सहायता मिलेगी. उन शासकों के हौसले पस्त होंगे जो दीर्घ काल तक भारत को हांकने का ख़्वाब देख रहे हैं. धार्मिक राष्ट्र में इसे तब्दील करना चाहते हैं. लेकिन, अमेरिकी सत्ता परिवर्तन से संवैधानिक शक्तियां मज़बूत हो सकती हैं. मानवाधिकारों को बल मिल सकता है. सारांश में, राज्य की लोकतान्त्रिक संवेदनशीलता पुनर्जीवित हो सकती है. पूंजीवाद का मानवीय चेहरा (capitalism with humane face) दिखाई दे सकता है. फिलहाल इससे अधिक की आशा नहीं करनी चाहिए .
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और राजेंद्र माथुर राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान समेत गणेशशंकर विद्यार्थी सम्मान से सम्मानित हैं।