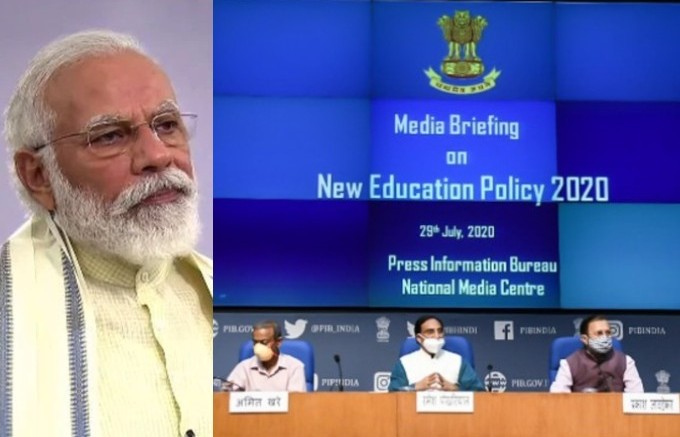हमारे देश में नीति-निर्माण की विडंबना यह है कि उससे प्रभावित होने वाले समूह की उसमें कोई भूमिका नहीं होती, उनसे राय-मशविरा कम ही किया जाता है। कोई भी सेक्टर इससे अछूता नहीं है, तो फिर शिक्षा-व्यवस्था भी अपवाद क्यों होगा? केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसके लिए दो लाख से भी अधिक लोगों से फीडबैक लिया गया है। लेकिन ये दो लाख से अधिक लोग कौन थे? क्या इस शिक्षा नीति को आकार देने वाले समूह ने देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघों या वहाँ के सांविधिक इकाइयों, यथा- एकेडमिक कौंसिल, एक्जीक्यूटिव कौंसिल आदि के निर्वाचित प्रतिनिधियों से कोई विचार-विमर्श किया? उत्तर नहीं में है, क्योंकि मशविरा के लिए एक विशेष संगठन के लोगों को ही बुलाया गया? क्या सत्ताधारी पार्टी से जुड़े शिक्षक और छात्र संगठन के लोग ही ‘स्टेक होल्डर’ होते हैं? अन्य संगठनों ने बिना मांगे अपने विचार और सुझाव भेजे, लेकिन उसका संज्ञान इस समूह ने लिया होगा, इस पर संदेह ही है।
केंद्र सरकार शिक्षा-व्यवस्था में व्यापक सुधार के नाम पर इस आपदा-काल में आनन-फानन में निर्णय लेकर देश पर थोप रही है, उससे किस प्रकार का बुनियादी बदलाव आयेगा, यह समझ से परे है। इस शिक्षा-नीति में उच्च शिक्षा से जुड़े बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यह साफ तौर पार निजीकरण को प्रभावी रूप से लागू करने का दस्तावेज दिखाई देता है। उच्च शिक्षा के निजीकरण की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, लेकिन सरकार ने अब इसे पूरी तरह से बाजार के हवाले करने का निर्णय सुना दिया है।
नई शिक्षा नीति पहले से मौजूद निजी विश्वविद्यालय के कुनबे में बड़े-बड़े कॉरपोरेट खिलाड़ियों के उतरने का रास्ता साफ करेगा। वैसे इसका संकेत उस समय ही मिल गया था, जब सरकार ने ‘इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस’ की घोषणा की थी। उस समय जिस ‘जियो विश्वविद्यालय’ को शामिल किया गया था और जिसकी रूपरेखा अभी तक कागजों पर बन रही थी, अब उसे अमलीजामा पहनाना आसान हो जायेगा। सरकारी शिक्षण संस्थानों को अब खरीदा-बेचा जा सकेगा, उन्हें बंद किया जाना भी सुविधाजनक हो जायेगा। आगे चलकर, वित्तीय रूप से संकटग्रस्त किसी सरकारी कॉलेज का अधिग्रहण कर उसे ‘निजी विश्वविद्यालय’ के रूप में बदलना सरल हो जायेगा।
नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि प्रत्येक संस्थान वित्तीय, अकादमिक और प्रशासनिक रूप से स्वायत्त होंगे। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अगले 15 वर्षों में, सन् 2035 तक विश्वविद्यालय से कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करने का प्रावधान है और इनको स्वायत्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार पहले से ही कॉलेजों को स्वायत्त करने की योजना पर चल रही थी; लेकिन अभी तक, विशेष रुप में दिल्ली विश्वविद्यालय में, शिक्षक संगठनों के विरोध के कारण तथा कॉलेज के विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के कारण यह योजना सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत यह सब आसान हो जायेगा। इस तरह के कॉलेज ऑटोनोमस डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज के रूप में मान्य होंगे। लेकिन इस तथाकथित स्वायत्तता की कीमत विद्यार्थियों से वसूल की जायेगी। ये प्रावधान स्पष्ट तौर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली सरकारी आवंटन में भारी वित्तीय कटौती की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसा करके सरकार अपने वित्तीय दायित्व से मुक्त होने की मंशा स्पष्ट कर रही है।
स्वायत्त होने के बाद सभी शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों को अपने वित्तीय प्रबंधन के लिए‘आत्मनिर्भर’ बनना पड़ेगा तथा वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो ‘हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (हेफा)’ से लोन लेना होगा अथवा अन्य तरीकों से आर्थिक संसाधन जुटाने पड़ेंगे। दोनों ही स्थितियों में आर्थिक बोझ विद्यार्थियों पर पड़ेगा। इसलिए निश्चित तौर पर फीस में भारी वृद्धि होगी, जिसका भार उठाना आर्थिक रुप से कमजोर किसी भी समुदाय के परिवार के लिए कठिन होगा। लेकिन इससे सबसे अधिक नुकसान दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को होगा। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग और अन्य धार्मिक समुदाय भी इससे प्रभावित होगा।
जिस उच्च शिक्षा की वजह से समाज की सोच और ढाँचे में परिवर्तन संभव हो पाया है, यह नई शिक्षा नीति इस तबके को उसी से वंचित कर देगी। कुछ समर्थक यह तर्क दे सकते हैं कि इसमें ‘स्कॉलरशिप’ का प्रावधान किया गया है। लेकिन क्या यह सभी जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध हो पायेगा? आज भी ‘स्कॉलरशिप’ मौजूद है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। वर्तमान समय में अपेक्षाकृत कम फीस की वजह से यह तबका किसी तरीके से उच्च शिक्षा की ओर देखने का साहस जुटा लेता है और संघर्षों का सामना करते हुए बहुत सारे स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण कर भी लेते हैं। लेकिन, आने वाले समय में शायद हाशिए पर खड़ा वर्ग उच्च शिक्षा का सपना देखना भी छोड़ दे!
नई शिक्षा नीति में सरकार का दावा है कि वह शिक्षण संस्थानों को अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता देगी। यह स्वायत्तता तो विश्वविद्यालयों में पहले से मौजूद थी, इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि विश्वविद्यालयों की अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता में सबसे अधिक हस्तक्षेप वर्तमान सरकार ने ही किया है। चाहे सिलेबस के निर्माण का मामला हो या शोध के लिए विषय तय करने का मुद्दा; विश्वविद्यालय में इस संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत इकाईयों- रिसर्च कौंसिल, एकेडमिक कौंसिल, एक्जीक्यूटिव कौंसिल आदि को दरकिनार कर सरकार के आदेश पर निर्णय लिए गए। सन् 2015 के सत्र से लागू किए गए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के लिए सिलेबस बनाने का काम यूजीसी ने किया था, जबकि उसकी भूमिका केवल अनुदान देने तक सीमित थी। जबकि सिलेबस निर्माण का काम विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग, संकाय और अकेडमिक कौंसिल सिलेबस करते थे।यह स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वायत्तता पर हमला था।
इस शिक्षा नीति में एक निश्चित अवधि के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की बात की गई है, जाहिर है कि यह शिक्षकों के भीतर भविष्य को लेकर अनिश्चितता-बोध भर देगा। आज पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार तदर्थ या कॉन्ट्रैक्ट (संविदा) पर काम कर रहे हैं, लेकिन खाली पड़े पदों को स्थायी रूप से भरने के लिए आवश्यक ठोस कदम नहीं उठाये गए। आज जो लोग अस्थायी या तदर्थ रूप में काम कर भी रहे हैं, वे भविष्य को लेकर दवाब और तनाव से ग्रसित हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित और अग्रणी विश्वविद्यालय में 50 फीसदी से अधिक तदर्थ और अतिथि प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि राज्य के विश्वविद्यालयों की स्थिति तो और भी अधिक खराब है। परिणामस्वरूप प्रतिभाशाली लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अध्ययन-अध्यापन और शोध का प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्तर में गिरावट और गुणवत्तापूर्ण शोध के अभाव का यह एक महत्वपूर्ण कारण है।
शिक्षकों को स्थायी करने के लिए जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया जायेगा, तो फिर उच्च शिक्षा की तस्वीर कैसे बदलेगी? दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षक दो दशक से भी अधिक समय से तदर्थ रूप में ही पढ़ा रहे हैं, जबकि हजारों शिक्षक कई-कई सालों से साक्षात्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक-एक कॉलेज में उसी पद के लिए तीन-चार बार फॉर्म भरे गये हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं हुए हैं। नई शिक्षा नीति इस समस्या का समाधान करने की बजाए इसे बढ़ा ही रही है।
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत चार साल के स्नातक पाठ्यक्रम को भी सरकार की अग्रिम सोच कई रूप में रेखांकित करने वाले भी कई लोग होंगे। लेकिन यह भी कोई नई योजना नहीं है। वर्ष 2013 में तत्कालीन कुलपति प्रो. दिनेश सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय में इसे लागू किया था और बिल्कुल इसी ढाँचे के साथ उसमें भी बाहर निकलने की स्थिति में अलग-अलग उपाधि देने का प्रावधान रखा गया था। इस पाठ्यक्रम को सत्ता में आने के बाद बीजेपी की सरकार ने रद्द की। आज उसी पाठ्यक्रम को उसी ढाँचे में लाकर सरकार अपनी गलती सुधारना चाहती है या गलती दोहराना! अगर वर्ष 2014 में वह पाठ्यक्रम गलत था और उसे रद्द किया गया तो अब वही पाठ्यक्रम सही कैसे हो सकता है? यदि वर्ष 2014का वह स्नातक पाठ्यक्रम सही था, तो उसे रद्द करके क्या सरकार ने गलती नहीं की? और क्या इस कदम से हमारी शिक्षा-व्यवस्था इन वर्षों में शैक्षणिक रूप से तो कहीं पीछे नहीं हो गई?इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए।
भारत जैसे विभिन्नता और विविधता वाले विशाल देश के लिए जहाँ बड़े पैमाने पर गरीबी है, आर्थिक असमानता है, कई प्रकार के धार्मिक-जातिगत भेदभाव और असंतुलन हैं तथा बहुत बड़ी आबादी अभी भी उच्च शिक्षा के दायरे से बाहर है, वहाँ उच्च शिक्षा को स्वायत्तता के नाम पर बाजार के हवाले कर देना, वंचित तबके को इस दायरे से बाहर रखने का षड्यंत्र ही कहा जा सकता है। जिस तरह से रेलवे, एलआईसी, भारत पेट्रोलियम तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों आदि क्षेत्रों में विदेशी और निजी निवेश की अनुमति देकर एवं उसकी सीमा को बढाकर वर्तमान सरकार ने उदारीकरण और मुक्त अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है, उसी तरीके से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है।
चरमराता आधारभूत ढांचा, सरकारी अनुदान में कटौती, बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षण संस्थाओं की समाप्त होती स्वायत्तता, वर्षों से रिक्त पड़े पद, शिक्षकों की भारी कमी, बहुत बड़ी संख्या में तदर्थ या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते शिक्षक आदि समस्याएँ मिलकर भारत के विश्वविद्यालयों की नींव को खोखला कर रहे हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों की स्थिति तो पहले से ही जर्जर थी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी उसी रास्ते पर अग्रसर हैं। उच्च शिक्षा में बुनियादी बदलाव के लिए जिस समग्र सोच और दृष्टिकोण की स्पष्टता की जरूरत है, उसका इस नई शिक्षा नीति में अभाव है। इस नई शिक्षा नीति से निजीकरण को बल मिलेगा, जबकि वंचित तबके के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो जायेगा।
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, श्यामलाल कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय), पूर्व सदस्य, अकेडमिक कौंसिल, दिल्ली विश्वविद्यालय.