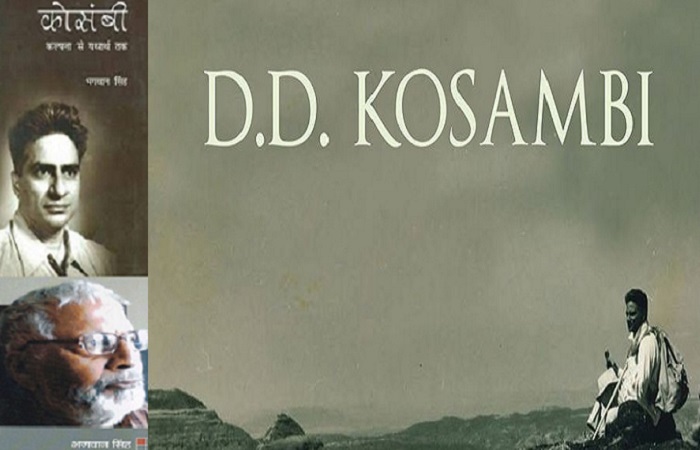मित्रो, प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा की पुण्यतिथि (20 अगस्त) के अवसर पर हमने भगवान सिंह की पुस्तक कोसंबी: कल्पना से यथार्थ तक पर लिखी वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप कुमार की समीक्षा प्रकाशित की थी। आशय यह बताना था कि आरएसएस के प्रोजेक्ट हिंदुत्व को मिली सफलता किस तरह ज्ञान-विज्ञान के परिसर को दूषित कर रही है और इतिहास को ख़ासतौर पर अपनी राजनीतिक विचारधारा की ज़रूरतों के अनुकूल बनाने की कोशिश हो रही है। हास्यास्पद तर्कों से सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी लिपि भी अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, को आर्यों की सभ्यता साबित करने में जुटे लेखक भगवान सिंह इसी खेल के मोहरे हैं जिन्होंने इस पुस्तक के ज़रिये हिंदुत्ववादी घृणा प्रोजेक्ट की राह में बढ़ी बाधा की तरह तैनात डी.डी कोसंबी के ऐतिहासिक अवदान पर सफ़ेदा पोतने की कोशिश की है। प्रो.सियाराम शर्मा ने भी कुछ वर्ष पहले इस पुस्तक की सुसंगत पड़ताल करते हुए एक लेख लिखा था जो मशहूर लेखक प्रियंवद के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका अकार में छपा था। हम इस बहस को आगे बढ़ाने के क्रम में साभार सहित इस लेख प्रकाशित कर रहे हैं- संपादक
तुम्हीं कहो कि यह अन्दाज-ए-गुफ्तुगू क्या है
सियाराम शर्मा
इतिहास राष्ट्रवादी या नृजातीय या पुनरूत्थानवादी विचारधाराओं के लिए उसी तरह कच्चा माल होता है जैसे हेरोइन के नशेडि़यों के लिए अफीम। इन विचारधाराओं के लिए शायद इतिहास सबसे जरूरी चीज होता है। अगर अतीत अनुकूल नहीं होता है तो उसे अपने अनुकूल गढ़ लिया जाता है।1
-एरिक हॉब्सबाम-
भगवान सिंह घृणा की हद तक मार्क्सवाद और मार्क्सवादी इतिहासकारों के प्रति पूर्वावग्रही हैं। कोसंबी: कल्पना से यथार्थ तक पुस्तक की मूल योजना कोसंबी के साथ-साथ मार्क्सवादी इतिहास लेखन की समृद्ध परंपरा को खारिज करने की है। इसके लिए लेखक ने कोसंबी के बाद के मार्क्सवादी इतिहासकारों का नाम लिये बिना हवा में तलवारबाजी की है। उनका आरोप यह है कि बाद के मार्क्सवादी इतिहासकारों ने उनका नाम जपने के सिवा कुछ भी मौलिक नहीं किया और उन्हीं की गलतियों को दुहराते रहे। सबसे पहले वे कोसंबी पर ईसाई मिशनरियों के एजेन्डे पर पश्चिमी आकाओं के लिए इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने और विकृत करने का आरोप लगाते हैं। वे फतवा देते हैं कि उनमें ’इतिहास को समझने की आकांक्षा नहीं है, इसे ध्वस्त करने का उन्माद अवश्य है।’ उनका तो यह भी आरोप है कि आगे चलकर भारत के प्राचीन इतिहास लेखन में डी.डी. कोसंबी की जो मूर्ति गढ़ी गयी वह पूरी तरह प्रायोजित है। गोया उन्हें जो महत्व दिया गया, वे उसके योग्य नहीं थे। लेखकीय शालीनता की परवाह किये बिना वे एक कर्मठ और प्रतिभाशाली लेखक के समस्त ऐतिहासिक कर्म पर सफेदा पोतते हुए अपने विसर्जनवादी नजरिये का परिचय कुछ इस प्रकार देते हैं- “हम वैदिक समाज और संस्कृति को समझने के लिए कोसंबी को नहीं पढ़ सकते। सभ्यता की विकास प्रक्रिया को समझने के लिए कोसंबी को नहीं पढ़ सकते। परन्तु अपने समय की सबसे जीवंत और ओजस्वी संस्कृति को नष्ट कैसे किया जा सकता है, इसके लिए वह बहुत उपयोगी इतिहासकार हैं। जिन प्रमाणों से अपने इरादों के विपरीत निष्कर्ष निकलते हों, उन्हें देखते ही कैसे आँखें बंद कर ली जाएँ यह कोसंबी से सीखा जा सकता है। इतिहासकार के रूप में उनकी प्रासांगिकता मात्र इतनी ही है।” 2
कोसंबी उन परिवर्तनकामी बुद्धिजीवियों में थे जो ’इतिहास लिखने की बजाय बदलना कही अधिक महत्वपूर्ण’ समझते थे। लेकिन इतिहास बदलने के लिए भी इतिहास की समझ जरूरी है। इसीलिए हर वह पीढ़ी जो इतिहास बदलना चाहती है, उसे नये सिरे से इतिहास लिखने की जरूरत महसूस होती है। इसी आवश्यकता के तहत वे इतिहास लेखन की ओर आकर्षित हुए। कोसंबी के पूर्व तक का इतिहास व्यक्तियों, राजवंशों और उससे जुड़ी घटनाओं का इतिहास था। उन्होने उसे उत्पादन के साधनों और सम्बंधों की जटिल अन्तक्र्रिया के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार-“उत्पादन के साधनों और संबंधों में हाने वाले क्रमिक परिवर्तनों का कालक्रम से प्रस्तुत किया गया विवरण ही इतिहास है।”3 इतिहास की इस परिभाषा में मार्क्स के उस मशहूर कथन की अनुगूँज है कि “भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली जीवन की आम सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है।”4 यह सच है कि उत्पादन के साधनों का प्रभाव संबंधों पर पड़ता है। लेकिन ये संबंध निर्धारणवादी नहीं होते। इन पर बिम्ब-प्रतिबिम्ब सिद्धांत लागू नहीं होता। इसीलिए कोसंबी ने कहा था-“हमारा दृष्टिकोण यांत्रिक नियतिवाद से बहुत हटकर होना चाहिए, विशेषतः भारत पर विचार करते समय। क्योंकि भारत में बाह्य रूप को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और अन्तर्वस्तु की उपेक्षा की जाती है। आर्थिक नियतितवाद भी किसी काम का नहीं है। यह अनिवार्य नहीं, सत्य भी नहीं, कि एक निश्चित मात्रा की धनराशि से एक निश्चित प्रकार का विकास अवश्य होगा। जिस सम्पूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया में समाज के स्वरूप का विकास होता है, उसका भी विशिष्ट महत्व है।”5
अपने दयनीय और अधकचरे मार्क्सवादी ज्ञान के बल पर भगवान सिंह कोसंबी के मार्क्सवादी होने पर सवाल उठाते हैं। “कोसंबी मार्क्सवादी होने का दावा करते हैं या सचमुच मार्क्सवादी हैं, और यदि मार्क्सवाद वही है, जिसे वह चरितार्थ करते हैं, तो मार्क्सवाद क्या है, यह एक शोध का विषय है।”6 डी.डी.कोसंबी के समस्त इतिहास लेखन की सबसे बड़ी ताकत उसके पीछे सक्रिय उनकी मार्क्सवादी दृष्टि ही है। यही उन्हें वह विश्लेषणात्मक औजार मुहैया करवाती है, जिससे वे सभ्यता, संस्कृति की वस्तुपरक, तार्किक और तलस्पर्शी व्याख्याएँ कर पाते हैं। इसके लिए उन्हें किसी पुनरूत्थानवादी, हिन्दुत्ववादी गद्य लेखकों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। असल में कोसंबी के प्रति भगवान सिंह की घृणा का मूल कारण उनका मार्क्सवादी होना भी है। घोषित रूप से या अपरोक्ष बिना मार्क्सवादी नजरिये के एक सच्चे इतिहास का लिखा जाना संभव भी नहीं है। अर्नेस्ट गेलनर ने ठीक ही कहा है-“लोग मार्क्सवादी योजना में सकारात्मक ढंग से यकीन करें या नहीं। लेकिन कोई और सुसंगत, सुप्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी ढाँचा उभरा नहीं है। न तो पश्चिम में और न पूरब में। लेकिन लोगों को किसी किस्म का टट्र चाहिए होता है जिसके खिलाफ वे सोच-विचार कर सकें। इसलिए इतिहास के मार्क्सवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करने वाले भी इसके विचारों का सहारा लेते हैं जब वे कहना चाहते हैं कि किस चीज पर वे सकारात्मक ढंग से भरोसा करते हैं।”7
कोसंबी अपने लेखन में मार्क्स के ऋण को स्वीकार करते हैं। मार्क्सवाद उनके लिए कोई जड़ सूत्र या बंद सिद्धांत नहीं है, उन्होंने अत्यन्त खुलेपन के साथ मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की पद्धति का उपयोग अपने इतिहास लेखन में किया है। यही उचित तरीका है। हॉब्सबाम ने भी इसका समर्थन किया है – “मैं तो इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा को हरगिज नहीं छोड़ना चाहता । लेकिन मार्क्सवादी इतिहास के सबसे फलदायक स्वरूप वे हैं जिनमें आज उनकी रचनाओं पर टिप्पणी करने से ज्यादा उनकी पद्धतियों का इस्तेमाल होता है।”8 कोसंबी आधार और अधिरचना की द्वन्द्वात्मकता और उसके अन्योनाश्रय संबंध को तो स्वीकार करते हैं पर आर्थिक निर्धारणवाद को खारिज करते हैं। ऊपरी ढाँचे की सापेक्ष स्वायत्तता को उन्होंने महत्व दिया है। प्राचीन इतिहास पर लिखते हुए उनके समक्ष स्पष्ट आर्थिक आधार उपलब्ध नहीं था। अतः उन्होंने बची-खुची अधिरचनाओं से आधार तक की यात्रा तय की। इसलिए कुछ लोगों ने उन पर ’सांस्कृतिक निर्धारणवादी’ होने का आरोप लगाया। अपनी मार्क्सवादी दृष्टि के खुलेपन के कारण ही वे मार्क्स के ’एशियाई उत्पादन पद्धति’ जैसे सूत्रीकरण के विरोध का साहस जुटा पाये और श्रीपाद अमृत डांगे की पुस्तक – ’इंडिया फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टु स्लेवरी’ की निर्मम आलोचना कर सके। मार्क्सवादी अन्तर्दृष्टि के साथ इतिहास लेखन में वे ’कम्बाईन्ड मेथड’ के पुरस्कर्ता थे। जहाँ जैसी भी आवश्यकता पड़ी, उन्होंने पुरातत्व, नृतत्व, सिक्काशास्त्र, साहित्य और भाषा जैसे विविध अनुशासनों का सार्थक इस्तेमाल किया।
मार्क्स के ’एशियाई उत्पादन पद्धति’ वाले गाँव एक ऐसे गाँव हैं जो अपने-आप में स्वतंत्र आर्थिक इकाईयों की तरह हैं, जहाँ उत्पादन सिर्फ गाँव की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है, न कि बाहरी विनिमय के लिए। इसने एशियाई गाँवों के परिवर्तन और विकास को बाधित करने का कार्य किया। कोसंबी इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि भारतीय गाँव अनंत काल से इसी तरह चले आते हुए गाँव नहीं है। लोहे के फाल के उपयोग और व्यापक पैमाने पर कृषि की शुरूआत ने इन गाँवों में परिवर्तन लाया। साथ ही इन गाँवों में नमक और धातुओं का उत्पादन नहीं होता था। अतः इसके लिए वे गाँव से बाहर के विनिमय पर निर्भर रहते थे।
कोसंबी का यह भी मानना था कि प्रचलित मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार भारत के इतिहास को आदिम साम्यवाद,-दासप्रथा,-सामंतवाद और पूँजीवाद के खाँचों में फिट नहीं किया जा सकता क्योंकि यूनान और रोम की तरह भारत में दासप्रथा लगभग नहीं था। यहाँ दासों की प्रायः खरीद-बिक्री नहीं होती थी और न ही श्रम आपूर्ति में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका थी। दासों की भूमिका हमारे समाज में सबसे निम्न वर्ण के शूद्र लोगों ने निभायी। लेकिन उनकी स्थिति दासों से भिन्न थी। अपनी इस समझ के आधार पर उन्होंने डांगे की उपर्युक्त पुस्तक की आलोचना की। सामंतवाद के यूरोपीय मॉडल को भी उन्होंने ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार सामंतवाद के प्रथम चरण में “सम्राट या शक्तिशाली राजा अपने अधीनस्थों से उगाही करता था जो स्वयं शासक थे और जब तक सर्वोच्च शासक को भुगतान करते थे, अपने-अपने राज्य में मनमानी करते थे। ये अधीनस्थ शासक कबीलाई सरदार भी हो सकते थे और लगता है कि बगैर वर्ग की मध्यस्थता के जो कि असल में भूमि स्वामी संस्तर था, सीधे प्रशासन द्वारा इलाके पर शासन करते थे। नीचे से सामंतवाद का अर्थ है अगला चरण जहाँ गाँव में राज्य और कृषक वर्ग के बीच भूस्वामियों का एक वर्ग विकसित हो जाता है, जो स्थानीय जनता के ऊपर सशस्त्र बल रखता था।”9 मार्क्स एंगेल्स के यहाँ इस तरह ऊपर और नीचे से सामंतवाद के दो स्तरों की कोई अवधारणा नहीं है। यह दामोदर धर्मानंद कोसंबी की भारतीय परिपे्रक्ष्य में की गयी नयी व्याख्या थी। हलाँकि आगे चलकर रामशरण शर्मा जैसे इतिहासकारों ने अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर इस मॉडल से अपनी असहमति जतायी।
प्राचीन भारतीय समाज के विश्लेषण के लिए उत्संस्करण (एकल्चरेशन) की अवधारणा भी कोसंबी की मौलिक अवधारणा है इसके आधार पर कबीलाई या जनजातीय समूहों का कृषक समाज में बिना हिंसा के विलयन किया जा सका। इसके लिए एक तरफ ब्राह्मणों के द्वारा आदिवासी देवी -देवताओं और मिथकों का आत्मसातीकरण किया गया तो दूसरी ओर कबीले के कुछ सरदारों को वर्ण व्यवस्था में ऊँचा दर्जा दिलाकर उन्हें शासक वर्ग में शामिल कर लिया गया। शेष कबीले के लोगों को निचली जाति के किसानों के रूप में मान्यता देकर मिला लिया गया । एक तरह से यह उत्संस्करण बिना किसी हिंसा के जनजातीय या कबीलाई समूह को वर्गीय समाज का हिस्सा बना लेने की प्रक्रिया थी। इस प्रकार कोसंबी द्वारा की गयी एशियाई उत्पादन पद्धति की आलोचना, भारत में दास प्रथा का अभाव, ऊपर और नीचे से सामंतवाद तथा उत्संस्करण की अवधारणा का शास्त्रीय मार्क्सवाद से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये उनकी मौलिक अवधारणाएँ हैं। प्राचीन भारतीय समाज के विश्लेषण में सहायक सिद्ध होती हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मार्क्सवाद के सिद्धान्तों को उन्हांेने आँख मूँदकर भारतीय समाज पर यंत्रवत् लागू नहीं किया।
असहिष्णुता फैलाने वाली विचारधाराएँ झूठी और आधारहीन कथाओं पर निर्भर होती हैं।
इस पुस्तक में डी.डी. कोसंबी की मान्यताओं को पूरी तरह निरस्त करने के लिए जिस आक्रामकता के साथ घृणा का प्रचार-प्रसार किया गया है, उसके पीछे भगवान सिंह की मूल मकसद वही है जो वर्षों से पुनरूत्थानवादियों और हिन्दुत्ववादियों की रही है। कोसंबी खुद इन प्रवृत्तियों से अपरिचित नहीं थे। वे कहते हैं-“कुछ लेखक अब भी यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जनक आर्य लोग थे। इस मत का कारण यह पूर्वग्रह है कि भारतीय संस्कृति की प्रत्येक उच्च उपलब्धि आर्याे की ही देन हो सकती है‘‘। 10 भगवान सिंह के अनुसार भी ’हड़प्पा सभ्यता वस्तुतः वैदिक सभ्यता ही थी’, हड़प्पा के साहित्य का अवशेष ऋग्वेद ही है।’ भगवान सिंह की कोसंबी से नाराजगी इसलिए है कि वे हड़प्पा सभ्यता का यह कहकर अवमूल्यन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कृषि क्षेत्र नदी घाटी तक ही सिमटा था। उनकी खेती का तरीका उन्नत नहीं था। वे हल का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका अतिरिक्त उत्पादन मेसोपोटामिया और मिस्र से कम था। वे कोसंबी को मूलतः हड़प्पा और वैदिक सभ्यता में कालगत और दायगत विच्छिन्नता के लिए दोषी मानते हैं। भगवान सिंह के अनुसार हड़प्पा वासियों ने अरायुक्त पहिये और रथ का आविष्कार किया था। वहाँ के कारीगर दूर-दूर तक खनिज संपदा का दोहन कर उससे सुन्दर और उपयोगी पण्य वस्तुएँ तैयार कर मेसोपोटामिया और पश्चिमी बाजारों में दूर-दूर तक बेच रहे थे। उनका व्यापार अत्यन्त उन्नत था। भगवान सिंह के शब्दों में – “मेसोपोटामिया के नगर भारतीय माल के बाजार थे। हड़प्पा के कारीगर दूर-दूर तक खनिज संपदा का दोहन कर रहे थे। उनसे अविश्वसनीय रूप में सुन्दर पण्य वस्तुएँ तैयार कर रहे थे। अपना माल सीधे और पश्चिमी बाजारों के माध्यम से दूर-दूर तक बेच रहे थे। उन्होंने अरायुक्त पहिये और रथ, गाड़ी (अनस) और छकड़े (शकटी) का आविष्कार करके परिवहन और मालवहन में एक नया अध्याय जोड़ा था। तकनीकी दृष्टि से भारत अपनी समकालीन सभ्यताओं से आगे था। इसकी भाषा के सुदूर क्षेत्रों तक प्रसार के पीछे उनका माल, उनकी तकनीकी और सांस्कृतिक अग्रता थी और थे इसके व्यापारिक उपकेन्द्र।”11
भगवान सिंह आर्यों के आव्रजन और उनके आक्रमणकारी होने के सिद्धांत से अपनी असहमति जताते हैं। वे उन्हें बर्बर, लुटेरा और घुम्मकड़ कहे जाने का भी प्रतिवाद करते हैं। वे आर्यों को यहाँ का मूल निवासी मानते हैं तथा आर्यों और यूरोपीय भाषाओं का प्रसार वे भारत से मध्य एशिया की ओर दिखाने का प्रयत्न करते हैं। वे उन्हें लौह तकनीक तथा कृषि की दृष्टि से भी उन्नत अवस्था में पाते हैं। इन सब के पीछे उनका उद्देश्य अतीत में भारत की महानता सिद्ध करना है। पुनरूत्थानवाद की यह प्रवृत्ति प्रायः वर्तमान की दुरावस्था की हताशा और कुंठा से पैदा होती है। आज हम अमेरिकी और यूरोपीय देशों के नेतृत्व में जारी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में उनके पिछलग्गू हैं। हमारा बाजार उनके मालों से पटा है। नव धनाढ़्य वर्ग,और मध्य वर्ग के बड़े हिस्से ने उनकी भाषाई और सांस्कृतिक वर्चस्व को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में आज हम अपने विस्तारवादी और प्रसारवादी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते, तो चलें स्वर्णिम अतीत का ही स्वप्न रचें। इन पुनरूत्थानवादी और विस्तारवादी संकीर्ण मानसिकता के समक्ष डी.डी. कोसंबी सबसे बड़ी चुनौती हैं। अतः इस पुस्तक में बार-बार उन्हें निशाना बनाया गया है। भगवान सिंह इस सबके पीछे अपने विस्तारवादी एजेन्डे को छिपा भी नहीं पाते। सच सामने आ ही जाता है-“भारत को भारोपीय का उत्स देश मानते ही न केवल भाषा और संस्कृति अपितु विज्ञान और दर्शन का भी प्रेरक भारत सिद्ध हो जाता और यूनान के जिस शिखर पर हीगेल और मार्क्स दोनों का अनन्य विश्वास था वह भी भारत से प्रेरित सिद्ध हो जाता ।….. हीगेल यदि सचमुच प्राच्यविदों के लेखन से परिचित थे, तो उन्हें विलियम जोन्स के उस कथन का ज्ञान रहा होगा, कि ’पाइथागोरस और प्लेटो ने अपने सिद्धांत उसी स्रोत से लिये होंगे जिससे भारतीय ऋषियों ने (जिसे वैदिक और ग्रीक काल रेखा पर ध्यान दें तो पता चल जायेगा किसने किससे लिया होगा), कि यूरोप कलाओं और विज्ञानों’ में एशिया की सभ्यताओं के योगदान के लिए उनका आभारी है और यह कि ‘सभ्यता का जन्म एशिया में हुआ‘। शून्य की अवधारणा, दाशमिक अंक प्रणाली, रसायन, भौतिकी और ज्यामिति के सिद्धांत भारत से अरब खलीफाओं के माध्यम से यूरोप तो पहुँचे ही हैं।”12 यह पुनरूत्थानवादी, विस्तारवादी आकांक्षा एक इतिहासकार की नहीं, अतीत ग्रस्त व्यक्ति की है। इस तरह मनमाना इतिहास नहीं लिखा जाता ।
भगवान सिंह डी.डी. कोसंबी को हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को अलगाने का दोषी मानते हुए हड़प्पा सभ्यता को ही वस्तुतः वैदिक सभ्यता मानते हैं और हड़प्पा सभ्यता के साहित्यिक अवशेष के रूप में ’ऋग्वेद’ को देखते हैं। अगर यह सही है तो हड़प्पावासियों और ’ऋग्वेद’ की भाषा और लिपि भिन्न क्यों है ? उसे आज तक पढ़ा क्यों नहीं जा सका? प्राचीन भारत की प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता की एकता के दावे को सिरे से खारिज करती हैं। उनके अनुसार “वैदिक वांगमय में मिलने वाले वर्णन से हड़प्पा सभ्यता का समीकरण बिठा सकना कठिन है। कारण सिर्फ यही नहीं है कि वह कालक्रम में पहले आती है, बल्कि दोनों भिन्न-भिन्न संस्कृतियों की नुमाइंदा हैं। यह बात खास तौर पर ध्यान खींचती हैं-इस अर्थ में भौगोलिक दृष्टि से दक्षिणी पंजाब में एक साझा क्षेत्र ऐसा है जो संबंध दिखा सकता था, बशर्ते कि कोई संबंध रहा होता। वैदिक ग्रंथों में वर्णित समाज पशुपालक और खेतिहर है जबकि हड़प्पा के जीवन में नगरीय केन्द्र व्यापक पैमाने पर चलने वाले व्यापार के केन्द्रीय तत्व थे। एक राज्य जैसी सत्ता से नियंत्रित बड़े-बड़े बखारों और बड़े पैमाने की भंडार-प्रणालियों के जो साक्ष्य खुदाइयों से मिले हैं, उनका कोई हवाला वैदिक साहित्य में नहीं मिलता । इन ग्रंथों में दस्तकारों के उत्पादन का शायद ही कोई जिक्र हो जबकि यही हड़प्पाई नगरों की सुस्थापित विशेषता थी। मुहरें हड़प्पावासियों के प्रयोग में थी, जबकि इन ग्रंथों में नजर नहीं आतीं। वैदिक वांगमय में लेखनकला का कोई ज्ञान दिखायी नहीं देता। हड़प्पावासियों के पास एक लिपि थी, जिसे पढ़ा जाना अभी बाकी है। …….. हड़़प्पाई स्थलों पर रथ और पहिये पूरी तरह और घोड़े लगभग पूरी तरह गायब हैं। घोड़े का अभाव यहाँ उल्लेखनीय है क्योंकि वेदों में वर्णित उत्सवों और अनुष्ठानों, दोनों में ही इसकी केन्द्र्रीय भूमिका होती थी। ……. वेद कर्मकांडों के ग्रंथ हैं और इसलिए अगर हड़प्पाई नगर भी उसी संस्कृति के रहे होते तो वहाँ के अनुष्ठानों से जुड़ी विशेषताएँ भी वेदों में जरूर प्रतिबिम्बित हुई होती।”13
डी.डी. कोसंबी नागर सिंधु संस्कृति का काल 3000 ई.पूर्व से 2000 ई.पूर्व तक मानते हैं। 1750 ई.पूर्व के आस-पास वे इसका अंत मानते हैं। इस काल निर्धारण के लिए भी भगवान सिंह ने उनकी आलोचना की। रामशरण शर्मा और रोमिला थापर भी हड़प्पा संस्कृति का समय 2500 ई. पूर्व से 1700 ई.पूर्व तक को स्वीकृति प्रदान कर एक तरह से कोसंबी को ही सही सिद्ध करते हैं। रामशरण शर्मा के अनुसार आर्यों की टोलियाँ 2000 ई.पूर्व के आस-पास भारत आना शुरू हुई। अतः आर्य सिन्धु घाटी सभ्यता के निर्माता नहीं हो सकते और न ही ’ऋग्वेद’ हड़प्पा के साहित्य का अवशेष हो सकता है। रामशरण शर्मा भगवान सिंह जैसे लोगों की इस धारणा का भी खण्डन करते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी और हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। “यदि हम विदेशी विद्वानों को छोड़ भी दें तो हमारे अपने देश के मूर्धन्य विद्वानों का यह मत नहीं है। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति का सहारा लेकर राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया पर संस्कृत के विद्वान के नाते अपने शोध के आधार पर उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। उनकी सुविख्यात पुस्तक ’आर्कटिक होम आॅफ दि वेदाज’ में बतलाया गया है कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र में था। यद्यपि अधिकांश विद्वान लोकमान्य तिलक के इस सिद्धांत से सहमत नहीं हैं, तो भी इसमें कोई संदेह नहीं कि तिलक के अनुसार आर्यों का मूल स्थान भारतवर्ष के बाहर था। इसी प्रकार रमेशचन्द्र मजुमदार और के.ए.नीलकंठ शास्त्री, देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर जैसे प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडितों के अनुसार आर्य भारत में बाहर से आये थे। ……. तिलक के समय में तो हड़प्पा अथवा सैंधव सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, लेकिन राखालदास बनर्जी और माधोस्वरूप वत्स जैसे विद्वान पुरातत्वविदों ने जब इसे खोजकर निकाला तो उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। चोटी के इतिहासकारों का भी यही मत है। मजुमदार, भाण्डारकर, नीलकंठ शास्त्री, रामचैधुरी, महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे, वामन विष्णु मिराशी, अनन्त सदाशिव अल्तेकर, दिनेश चन्द्र सरकार की कोटि के किसी शोध समर्पित भारतविद् या इतिहासकार ने हड़प्पा अथवा सैंधव सभ्यता को आर्यों की कृति नहीं माना है। ध्यान रहे ये सारे विद्वान भारतीय संस्कृति के पोषक और कट्टर समर्थक थे।”14
स्पष्ट है आर्यों के बाहर से आगमन और हड़प्पा तथा वैदिक सभ्यता को अलगाने के लिए भगवान सिंह डी.डी. कोसंबी को पानी पी-पीकर कोसते हैं। उन पर औपनिवेशिक शासकों के स्वामीभक्त सिपहसालार होने का आरोप मढ़ते हैं। लेकिन कोसंबी की जमात में मार्क्सवादी इतिहासकार ही नहीं, देश के जाने-माने राष्ट्रवादी इतिहासकारों का भी बड़ा हिस्सा शामिल है। यह मुद्दा विचारणीय है कि भगवान सिंह जैसे हिन्दुत्ववादी और पुनरूत्थानवादी विचारक आर्यों के बाहरी होने के विचार से इतने बौखला क्यों जाते हैं ? उनकी बौखलाहट का कारण क्या है ? असल में हिन्दुत्व के समर्थक और धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले लोग हर बाहर से आने वाले लोगों और धार्मिक समूहों को देश से बाहर निकालने का राग आलापते हैं और उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक घोषित करते हैं। आर्य बाहर से आये थे, यह सिद्ध होते ही वे खुद बाहरी साबित होते हैं और उनकी घृणा की राजनीति की पूरी तर्क श्रृंखला गड़बड़ा जाती है। इस तथ्य को रामशरण शर्मा ने बहुत अच्छी तरह व्याख्यायित किया है। वे कहते हैं “हिन्दू सम्प्रदायवादी प्रचार करते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे और यहाँ से वे विश्व के दूसरे भागों में फैले। वे यह प्रचार किसी ठोस शोध या अध्ययन के आधार पर नहीं करते हैं बल्कि राजनीतिक और आक्रामक भावनाओं से अभिभूत होकर ऐतिहासिक तथ्यों की तोड़-मरोड़ करते हैं। प्रचारक सोचते हैं कि यदि आर्यों का मूल वासस्थान भारत से बाहर माना जायेगा तो वे विदेशी समझे जायेगें और आर्य उसी कोटि में रखे जायेंगे जिस कोटि में वे स्वयं मुसलमानों और ईसाइयों को रखते हैं।”15
भगवान सिंह की रूचि का क्षेत्र तुलनात्मक भाषा शास्त्र है। ’ऋग्वेद’ में आये शब्दों के आधार पर वे भी हिन्दुत्ववादी निष्कर्षो पर पहुँचते हैं। हिन्दुत्ववादियों की तरह उनका भी मत है कि “मूल भारोपीय भाषा का विकास भारत में ही हुआ दिखायी देता है। …….वैदिक भाषा से जिस सभ्यता का पूर्वानुमान होता है, वह पूरे भारोपीय क्षेत्र में केवल भारत और वह भी हड़प्पा सभ्यता में ही दिखायी देती है। …… जो भी हो, भारत में बाहर से वैदिक या आर्य भाषा के आने का कोई प्रमाण दिखायी नहीं देता, जबकि हड़प्पा के व्यापारियों के साथ इस प्रभाव के बाहर फैलने की संभावना दिखायी देती है।”16 यह दिलचस्प है कि भगवान सिंह डी.डी. कोसंबी पर पश्चिमवादी नजरिये से इतिहास को विकृत करने का आरोप लगाते हैं पर वे खुद अंधराष्ट्रवादी, विस्तारवादी नजरिये के तहत् भारोपीय भाषा का उत्स भारत में मानकर पश्चिम एशिया और यूरोप में उसके प्रभाव की वकालत करने लगते हैं। रोमिला थापर ने ठीक ही कहा है “देशी पर विदेशी को केवल आरोपित करके इनकी व्याख्या करना ऐतिहासिक व्याख्या का एक बेहद लचर तरीका है। इस तर्क को पलटकर यह दावा करना भी कि विदेशी वास्तव में देसी है, उतना ही सरलतावादी है।”17
सिर्फ कुछ शब्दों के आधार पर सभ्यता के विकास की दिशा तय नहीं की जा सकती। रोमिला थापर के अनुसार ऋग्वेद ज्यादा से ज्यादा 1500 ई.पूर्व या इससे थोड़ा बहुत बाद की रचना है। इसके आधार पर यह कैसे कहा जा सकता है कि 2000 ई.पूर्व विनष्ट सभ्यता और भाषा का प्रसार पश्चिम एशिया और यूरोप में हुआ। ’ऋग्वेद’ कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। वह कर्मकांडों का रहस्यवादी विवरण है। अतः इस आधार पर इतिहास की पुनर्रचना कैसे की जा सकती है? साहित्यिक और भाषाई तथ्यों के साथ-साथ पुरातात्विक तथ्यों का ताल-मेल बैठाकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। इसीलिए कोसंबी समन्वित पद्धति पर बल देते है । रामशरण शर्मा भगवान सिंह जैसे लोगों के प्रयासों को खारिज करते हुए कहते हैं- “भाषागत साक्ष्यों की जाँच पुरातात्विक सामग्री के द्वारा की जा सकती है। यह ध्यान देने का विषय है कि पुरातात्विक सामग्री अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही साथ यह भी बतलाना आवश्यक है कि केवल विभिन्न हिन्दयूरोपीय (भारोपीय) भाषाओं में पाये गये सजात शब्दों के अध्ययन को ही आद्य हिन्द-यूरोपीय संस्कृति के पुनर्निर्माण का स्रोत नहीं बनाया जा सकता है।”18
यह पुस्तक साम्प्रदायिक फासीवादियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखी गयी है। ये नयी बातें नहीं है पर भारत में साम्प्रदायिक फासीवाद के वर्तमान उभार ने उसे नया परिपे्रक्ष्य प्रदान किया है। अतः आवाज में बल, आक्रोश और आक्रामकता पूर्व से कहीं ज्यादा है। इसमें न तो कोसंबी को समझने की कोशिश है, न ही वर्तमान संदर्भों में उन्हें सच्चे ढंग से मूल्यांकित करने की। इसमें अपने पूर्वग्रहों को थोपने और एक बड़े इतिहासकार को खारिज करने का उन्माद ज्यादा है। मार्क ब्लाख ने ठीक ही कहा था “दुर्भाग्य की बात है कि फैसला सुनाने की आदत व्याख्या करने की रूचि ही खत्म कर देती है। जब अतीत के आवेग वर्तमान के पूर्वग्रहों से गुँथ जाते हैं, तो मानवीय यथार्थ एक श्वेत श्याम चित्र बनकर रह जाता है। इस संदर्भ में मोंतैंन्य ने हमें खतरे से आगाह किया है, ‘जब कभी निर्णय एक ओर झुक जाता है तो हम वर्णन को उसी दिशा में मोड़ने और विकृत करने से नहीं बच सकते‘।”19
भगवान सिंह के द्वारा सचेत ढंग से की गयी यह कोशिश कि आर्य देशी थे। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता एक ही है तथा भारोपीय भाषा का प्रसार पश्चिम एशिया और यूरोप में भारत से ही हुआ, दरअसल कोई इतिहास लेखन न होकर एक गल्प रचने का प्रयास है। उन्हें इतिहास लेखन छोड़कर गल्प में ही और हाथ आजमाना चाहिए। ’अपने-अपने राम’ इसका उदाहरण है। यह मात्र संयोग नहीं है कि ’हड़प्पा और वैदिक साहित्य’ के आमुख में उन्हें गल्प और इतिहास बहुत करीब नजर आता है। ऐसे में जब एक सभ्यता पूरी तरह विनष्ट हो गयी हो, ऋग्वेद के अलावे कोई और प्रामाणिक ग्रन्थ उपलब्ध न हो, पुरातत्व में रूचि न हो और इतिहास को मनमाने तरीके से गढ़ना हो तो इसकी संभावना और बढ़ जाती है। झूठे गल्प रचने के ऐसे ही प्रयासों पर एरिक हॉब्सबाम ने कहा था- “आजकल उपन्यासकार अपनी कथावस्तु का आधार कल्पित तथ्यों के बजाय दस्तावेजी इतिहास को बनाने लगे हैं। इसके कारण ऐतिहासिक तथ्य और कथा के बीच की सीमारेखा धुँधली होती जा रही है। ……. असहिष्णुता फैलाने वाली कुछ विचारधाराएँ पूरी तरह झूठी और आधारहीन कथाओं पर निर्भर होती है। इतिहास की जगह पर मिथक या गढ़े हुए झूठ ला बिठाने की ऐसी ही तमाम कोशिशें बदतरीन बौद्धिक मजाक ही नहीं है। वे ही तो तय करते हैं कि स्कूली किताबो में क्या होना चाहिए।”20
इतिहासकार कोई चिड़चिड़ा दंडाधिकारी नहीं है।
ज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तित्वों के बीच तर्क-वितर्क, बहस-मुबाहिसा, खण्डन-मण्डन तथा आपसी स्वस्थ संवाद की हमेशा गुंजाइश रहती है। नये तथ्यों, प्रमाणों, विश्लेषणों और खोजों के आधार पर नयी अवधारणाएँ सामने आती है। लेकिन इस क्रम में पूर्व पक्ष के प्रति हमेशा संयत, शालीन और विनम्र भाषा और व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। प्रथम दौर के इतिहासकार में बहुत सी सीमाएँ और कमजोरियाँ नजर आ सकती हैं। वह वाजिब भी है। उनका उल्लेख किया जाना चाहिए। कोसंबी के इतिहास लेखन की भी सीमाएँ हैं। उनका लेखन पूरी तरह अन्तर्विरोध रहित नहीं है। उनकी सीमाओं और अन्तर्विरोधों पर भी अँगुली रखी जानी चाहिए। इससे कोसंबी का महत्व कम नहीं हो जाता। वे अपनी सीमाओं और अन्तर्विरोधों के साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सामंतवाद के उनके दो स्तरों के सिद्धांत, बौद्ध धर्म की अवनति के कारण, कौटिल्य के ’अर्थशास्त्र’ का काल निर्धारण, उर्वशी-पुरूरवा प्रसंग की टोटम मूलक व्याख्याओं से कई मार्क्सवादी इतिहासकार भी सहमत नहीं हैं पर उनका रवैया शत्रुतापूर्ण नहीं है। मुख्य सवाल नीयत का है। कोई दोष दर्शन में इतना मशगूल हो जाये कि किसी व्यक्ति का अवदान नजर ही न आये तो इस दृष्टि दोष का क्या किया जाये। आप यथार्थ और सत्य के प्रति किसी हद तक निर्मम और कटु हो सकते हैं पर किसी के व्यक्तित्व और चरित्र हनन का प्रयास निंदनीय है। समीक्ष्य पुस्तक में जगह-जगह डी.डी. कोसंबी के व्यक्तित्व पर लेखक ने जो असंयत, अभद्र और अर्नगल टिप्पणियाँ की हैं, वह अत्यंत आपत्तिजनक है। खुद मुख्तार बनकर जगह-जगह कोसंबी के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने जो फैसले सुनाये हैं, उनमें से कुछ को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाये तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है।
“उनका विवेचन प्रायः अन्तर्विरोधी और यांत्रिक हो जाता है‘ । ‘यांत्रिकता बल प्रयोग के सीमा तक बढ़ जाती है । वह तथ्यों को अपने अनुमान से तोड़ और बदलकर एक काल्पनिक यथार्थ रचते हैं। ’संस्कृत में उपलब्ध सामग्री का कोसंबी ने बहुत अधकचरे रूप में और बहुत कम इस्तेमाल किया है।’ ’जिस अटपटेपन पर हँसी रोकने का प्रयत्न करना होता है, उनको ही कोसंबी का अपूर्व योगदान मानकर प्रशस्तियाँ की जाती रही।’ ’सभी को इतना कुपढ़ और अंधानुरागी पाठक वर्ग नहीं मिलता, जितना उन्हें भारतीय इतिहास के आपातिक मोड़ पर मिल गया।’ ’वह अल्पज्ञात से सुविदित को, संदिग्ध से विश्वसनीय को, एकांगी से सर्वांगीण को निरस्त करते हुए एक नया और विचित्र इतिहास रचते हैं।’ ’कोसंबी एक इतिहासकार से अधिक इतिहास की लाठी हैं और इस लाठी का प्रयोग उन पर किया जाता रहा है, जो इतिहास को समझना चाहते हैं।’ ’कोसंबी अधिक से अधिक औपनिवेशिक काल के शासकों के स्वामीभक्त सिपहसलार हो सकते थे, उनसे पुरस्कृत हो सकते थे, उन्हीं के द्वारा उन्हें भारत का तेजस्वी इतिहासकार के रूप में पेश भी किया जा सकता था, परन्तु वह स्वतंत्र भारत के इतिहासकार नहीं हो सकते थे।’ ’अपनी युग दृष्टि और वस्तुदृष्टि का विस्तार तक नहीं किया।’ ’अपने से वरिष्ठ और अनुभवी आचार्यों को भी वह तुच्छ समझते थे।’ ’वह अपने को अपने ज्ञान प्रदर्शन से रोक नहीं पाते।’ ’यशोलिप्सा उनमें बहुत प्रबल थी।’ ’संस्कृत का अच्छा ज्ञान होते हुए भी वैदिक साहित्य ही नहीं, साहित्य मात्र की समझ नहीं थी।’ ’कोसंबी जालसाजी की हद तक जाकर अर्थ का अनर्थ करते हैं।’ ’कोसंबी की सोच में नस्लवाद उनके अवचेतन में समाया हुआ था।’ ’कोसंबी की मुख्य समस्या रंगभेद की है’।”
इन टिप्पणियों में अन्तर्निहित निर्णयों और फैसलों से अस्तित्ववादियों के ’दूसरे नरक हैं’ की बू आती है। दूसरों की ऐसी ही उपेक्षा और तिरस्कार से आहत हो गालिब ने पूछा होगा – “हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है/तुम्हीं कहो कि यह अन्दाज-ए-गुफ्तुगू क्या है।” उपर्युक्त उद्धरणो से स्पष्ट है कि दामोदर धर्मानंद कोसंबी भगवान सिंह की नजरों में धैर्यहीन, दंभी, औपनिवेशिक शासकों के स्वामीभक्त सिपहसलार, यशोलिप्सा से भरे, दुराग्रही, जालसाज, नस्लवादी, रंगभेदी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्तित्व थे। उन्हें खलनायक सिद्ध करने के लिए या उनके प्रति अपनी घृणा को प्रदर्शित करने के लिए जैसे उपर्युक्त विशेषण भी कम पड़ रहे थे। अतः वे उनके व्यक्तित्व और चरित्र हत्या पर उतर आते हैं। उनके निजी जीवन में ताक-झाँक करने लगते हैं। पश्चिमी विद्वानों के प्रति मोहग्रस्तता के लिए कोसंबी को कटघरे में खड़ा करने वाले भगवान सिंह उन्हें नीचा दिखाने के लिए एक अमेरिकी पूँजीपति गवाह को भी ढूँढ लाते हैं-“कोसंबी अपनी यशोलिप्सा के लिए इतिहास लेखन कर रहे थे, इतिहास में न तो स्वतः उनकी रूचि थी, न इतिहास की समझ। प्रदर्शनप्रियता इतनी अधिक थी कि अपने सीमित आर्थिक साधनों के बाद भी वह रेल के फस्र्ट क्लास में सफर करते थे, जिस पर व्यंग्य करते हुए इंगैल्स ने लिखा था कि वह स्वयं एक अमेरिकी पूँजीवादी होते हुए भी भारत में दूसरे दर्जें के ऊपर यात्रा नहीं कर पाया पर मार्क्सवादी कोसंबी ने उसे डकन क्वीन में पहले दर्जे में यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया । इसमें यह भी जोड़ा जा सकता है कि वह आत्मरति के शिकार थे, उन्हें अपने सिवाय किसी से प्रेम न था, न अपने देश से, न समाज से, न भाषा से, न परिवार से। उनका कुत्ता अवश्य अपवाद रहा हो सकता है। इसीलिए लोग उनसे डरते भले रहे हों, उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। उनके अपने छात्र, पत्नी और बच्चे तक नहीं। वह मार्क्सवादी से अधिक अस्तित्ववादी थे और थे आत्मनिर्वासन के शिकार।”21
इस तरह के एकतरफा फैसले वैयक्तिक घृणा की पराकष्ठा है। ये वही लोग कर सकते हैं जो देश और समाज में घृणा फैलाने के कार्य को ही अपनी देशभक्ति का प्रमाण मानते हैं। किसी साहित्य और साहित्यिक कृति का लेखक के व्यक्तित्व से गहरा संबंध होता है परन्तु किसी इतिहासकार के व्यक्तित्व और निजी जीवन से इतिहास का क्या संबंध होता है, यह पुस्तक उसका घटिया उदाहरण पेश करता है। भगवान सिंह ने अपनी समस्त साहित्यिक प्रतिभा का इस्तेमाल कोसंबी को खलनायक के रूप में गढ़ने के लिए किया है। मार्क ब्लाख ने कहा था-“इतिहासकार कोई चिड़चिड़ा जाँचकत्र्ता दंडाधिकारी नहीं है।” लेकिन भगवान सिंह पूरी किताब में चिड़चिड़े दंडाधिकारी की भूमिका में ही नजर आते हैं।
एक टेक्स्टबुक फासिस्ट की बजबजाती घृणा
’एक टेक्स्टबुक फासिस्ट’ की तरह भगवान सिंह में मुस्लिमों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों के प्रति तीव्र बजबजाती घृणा का भाव है। अपनी मुस्लिम कुंठा का इजहार वे आर्यों को स्वदेशी कहकर करते हैं। कम्युनिस्ट घृणा कोसंबी के प्रति घृणा मे तब्दील हो जाती है। ईसाई घृणा के कारण वे कोसंबी पर पश्चिम परस्त और प्राच्यवादी होने का आरोप लगाते हैं। वे उन्हें ईसाईयत से प्रभावित एवं ईसाई मिशनरियों के एजेन्डे पर कार्य करने वाले इतिहासकार के रूप में देखते हैं। शुरूआत वे उनके युवावस्था से करते हैं-“हावर्ड में साहित्य, भारतीय समाज, हिन्दू धर्म ओर विशेषतः ब्राह्मणवाद के विषय में मिशनरियों के विचारों को आप्तता दी जा रही थी, उससे युवक कोसंबी का अप्रभावित रह जाना असंभव था।” “उन्होंने मिशनरियों के अनुवादों, विचारों और उपनिवेशवादियों के मंतव्यों को आँख मूँदकर स्वीकार कर लिया।” “मिशनरी और औपनिवेशिक रूझान रखने वाले और घोषित रूप से रंगभेद और संकीर्ण राष्ट्रवाद से ग्रस्त पाश्चात्य विद्वानों की पुस्तकें पढ़ते-पढ़ते, उनकी वकालत को वस्तुपरक अध्ययन मानकर चलते रहने के कारण अकेले कोसंबी ही नहीं, अधिकांश महत्वाकांक्षी विद्वान मुग्धता की स्थिति में पहुँच चुके थे और यह समझ खो चुके थे कि इन दोनों को सावधानी से पढ़ा और समझा जाना चाहिए।” “कोसंबी के इतिहास लेखन में मिल की दृष्टि को अपनाया गया है और मिल ने अपना इतिहास मिशनरियों की भारत संबंधी रपटों के आधार पर लिखा था।” “वह सोच रहे थे या इस प्रचार के कायल हो गये थे कि ब्राह्मणवाद, जातिवाद और सम्प्रदायवाद की विकृतियों से यदि भारत को कोई बचा सकता है तो वह ईसाईयत ही है।”22 इन उद्धरणो में भगवान सिंह की ईसाई घृणा सतह पर आ गयी है। यह देश और समाज की तरह ज्ञान के भी साम्प्रदायीकरण की कोशिश है। यह धार्मिक घृणा ग्राहम स्टेंस के हत्यारों और गुजरात के दंगाईयों से कितनी मेल खाती है! उन्हें भरपूर खाद-पानी मुहैया करवाती है।
इस पुस्तक के अनुसार कोसंबी पश्चिम और ईसाईयत के वर्चस्ववादी एजेंडे पर कार्य करने वाले इतिहासकार नजर आते हैं। प्रच्छन्न तौर पर उन्हें हिन्दू विरोधी और राष्ट्रविरोधी तक साबित करने की कोशिश दिखायी पड़ती है। भगवान सिंह कोसंबी पर आरोप लगाते हैं कि वे भारतीय सभ्यता की प्रकृति को समझने को तैयार नहीं थे। वे प्राच्यवादी रूग्णाताओं से ग्रस्त थे। भारत को पश्चिमी नजरिये से देखते थे। भारत की जिन उपलब्धियों पर उन्हें गर्व होना चाहिए, उसकी वे खिल्ली उड़ाते हैं। वे कोसंबी के सभ्यता विमर्श को पश्चिम से विशेषतः जर्मन नस्लवादी चिंतन से प्रभावित मानते हैं। भगवान सिंह का आरोप यह भी है कि कोसंबी पश्चिमी बौद्धिक जगत् में अपनी स्वीकृति के लिए भारत की हेयता और पश्चिम की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं। जब भी किसी भारतीय लेखक की विशिष्टता को प्रतिपादित करना होता है तो उन्हें यूरोपीय लेखक याद आते हैं। उन्हीे के बीच रखकर वे उनका मूल्यांकन करते हैं। कोसंबी की पश्चिम परस्ती की आलोचना करते हुए वे तल्ख लहजे में कहते हैं – “कोसंबी की सबसे बड़ी समस्या पश्चिम की लादी को पूर्व की पीठ पर लादने की है, जिसके प्रतिनिधि वह स्वयं बनकर उसे अपनी पीठ पर ले लेते हैं। दूसरी समस्या उसे निष्ठापूर्वक गंतव्य तक पहुँचाने की है। लादी अपने असंतुलन से ही सरकने लगती है। वह वस्तुपरक होते तो उसे उसके अपने ही असंतुलन या अन्तर्विरोध से गिरने को छोड़ देते और भारवाही की कोटि से मुक्त हो जाते । परन्तु वह उस सरकती हुई लादी को संभालने के लिए अपनी रीढ़ टेढ़ी कर लेते हैं और अकादमिक विकलांगता के शिकार हो जाते हैं।”23
पश्चिम की समस्त ज्ञान परंपरा को नकारना भगवान सिंह के लिए देशप्रेम का उदाहरण हो सकता है। कोसंबी के लिए नहीं था। कोसंबी क्या करते जब भारत में इतिहास लेखन की परंपरा थी ही नहीं। अतः भारत पर जिन पश्चिमी विचारकों ने लिखा उनसे संवाद कायम करना प्राच्यवाद की हिमायत करना नहीं है। कोसंबी के लेखन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जब वे खुले मन से भारत के महत्व को स्वीकार करते हैं। क्या कोसंबी की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर भी भगवान सिंह उनके प्राच्यवादी होने के आरोप पर कायम रहेंगे? कोसंबी ने लिखा है – “जिस समय मकदूनिया का सिकंदर हिन्द के कल्पित वैभव और जादुई नाम को सुनकर पूर्व की ओर आकर्षित हुआ था, उस समय इंगलैण्ड और फ्रांस अभी-अभी लौह युग में कदम रख रहे थे। भारत के लिए नये व्यापारिक मार्ग के खोजने के प्रयास में ही अमरीका की खोज हुई है। यही वजह है कि अमरीका के मूल निवासियों को अब भी ’इंडियन’ कहा जाता है। अरब लोग जिस समय बौद्धिक दृष्टि से संसार में सबसे प्रगतिशील और सक्रिय थे, उस समय उन्होंने अपने चिकित्सा ग्रंथ और काफी हद तक गणित के ग्रन्थ भी, भारतीय स्रोतों के आधार पर तैयार किये। एशियाई संस्कृति और सभ्यता के दो प्राथमिक स्रोत चीन और भारत ही हैं। …….. भारत की ओर से किसी प्रकार के बल प्रयोग के बिना ही भारतीय धर्म-दर्शन का चीन और जापान में स्वागत हुआ, जबकि शायद ही कोई भारतीय पर्यटक इन देशों में पहुँचा हो या किसी भारतीय ने इन देशों के साथ व्यापार किया हो। इंदोनेशिया, विएतनाम, थाई देश, बर्मा और श्रीलंका के सांस्कृतिक इतिहास पर भारत का काफी अधिक प्रभाव पड़ा है, यद्यपि ये देश कभी भी भारतीय आधिपत्य में नहीं रहे।”24
भगवान सिंह का कोसंबी पर एक आरोप यह भी है कि वे ब्राह्मणवाद विरोधी हैं। उनमें ब्राह्मण वर्ण के प्रति उग्र क्षोभ और आक्रोश दिखाई देता है। यहाँ तक कि उनके अतिमानवीयकरण तथा ’आइकन’ बनाये जाने के पीछे भी वे मूल कारण उनका ब्राहम्णवाद विरोध ही देखते हैं। भगवान सिंह का कहना कि वे क्षत्रियों और वैश्यों को तो आर्य मानते हैं पर ब्राह्मणों और शूद्रों को मुख्यतः हैवानियत की अवस्था में जीने वाले आदिम समाज से उत्पन्न बताते हैं। ऐसा उन्होंने ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए किया। इसके पीछे मूल कारण था मदन-मोहन मालवीय द्वारा उन्हें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से निकाला जाना । हद तो तब हो जाती है जब वे यह सिद्ध करने का बेतूका प्रयास करते हैं कि इस अपमान का बदला लेने के लिए ही वे इतिहास लेखन कर रहे थे। खुद भगवान सिंह के शब्दों में ही क्लासिकल विधेयवादियों को भी शर्मिदा कर देने वाली उनकी विधेयवादी व्याख्या का यह नमूना प्रस्तुत है-“वह इतिहास लेखन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से निकाले जाने के अपमान का बदला लेने के लिए कर रहे थे। …….. कोसंबी का जैसा स्वभाव था, वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए तड़पते रहे होंगे और बदले के तरीके पर ऊहापोह में लगे रहे होंगे। अतः इतिहास में घुसकर मदनमोहन मालवीय और उनके ब्राह्मणत्व और हिन्दुत्व से बदला लेने पर अमल कुछ विलम्ब से आरंभ हुआ।”25 लगे हाथ वे यह भी जोड़ देते हैं कि वे ब्राह्मणवाद के महत्व को समझ नहीं सके।
भगवान सिंह के इस निम्न श्रेणी के आरोप पर कुछ भी कहने से बेहतर है कि ब्राह्मण वर्ण के बारे में कोसंबी के विचारों को जान लिया जाये। ’प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता’ नामक पुस्तक में वे इस वर्ण के प्रति अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं-“प्राचीन भारतीय समाज में ब्राह्मण वर्ग ही एक ऐसा समुदाय था जिसके लिए विधिवत् शिक्षा अनिवार्य थी और उसकी अपनी एक बौद्धिक परंपरा रही। वेद, व्याकरण तथा कर्मकाण्ड पर अधिकार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि शिष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी एकांत आश्रम में बारह साल तक किसी ब्राह्मण गुरू की सेवा में रहे। पवित्र ग्रंथों को, एक भी अक्षर की, एक भी स्वराघात की भूल किये बिना, कंठस्थ करना पड़ता था; फिर भी वेदों को लिपिबद्ध नहीं किया गया था। सीजर के गॉल प्रदेश के द्रुइद भी इसी प्रकार रटते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे, पर भारतीय वेदाभ्यासियों की बौद्धिक उपलब्धि का स्तर अधिक ऊँचा था। असोक तथा उसके उत्तराधिकारियों ने अपने समय के अग्रगण्य ब्राह्मणों का आदर-सत्कार किया तो इसका कारण यह था कि जाति व्यवस्था शिक्षा व संस्कृति के क्षेत्र में, समाज में वर्ग व्यवस्था बनाये रखने में, मूलतः परस्पर विरोधी समूहों के एकीकरण एवं विलयन में और सर्वसामान्यतः खेतिहर समाज के विस्तार में योग देकर अपने नये महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने में जुटी हुई थी।”26
डी.डी. कोसंबी जैन धर्म, उर्वशी-पुरूरवा प्रसंग, ‘श्रीमद्भगवद गीता‘, भर्तृहरि के ’शतकत्रयी’ और ’अर्थशास्त्र’ जैसी भारतीय संस्कृति की आधारभूत कृतियों पर जैसी विश्वसनीय और दृष्टि सम्पन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत की, वैसा आगे के मार्क्सवादी इतिहासकारों के यहाँ प्रायः नही है। कुछ हद तक रोमिला थापर ने समय-समय की शकुन्तला तथा ’संन्यास और प्रति संस्कृति की रचना’ जैसे निबन्धों में इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अधिकांश इतिहासकारों का ध्यान आर्थिक पक्ष पर ही केन्द्रित रहा। धर्म और संस्कृति का हरा-भरा चारागाह साम्प्रदायिक फासिस्टों के कुपाठ के लिए स्वतंत्र और खुला छोड़ दिया गया। वर्तमान साम्प्रदायिक फासीवाद के उभार के कई कारणों में से एक कारण यह भी है। कोसंबी का लेखन आज भी इस क्षेत्र में दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करता है। यह दुर्भाग्यजनक है कि अपनी सोची-समझी राणनीति के तहत् इस क्षेत्र में कोसंबी के उल्लेखनीय अवदान के बारे में भगवान सिंह अपराधिक चुप्पी साध लेते हैं। दृष्टि के अंधत्व और बौद्धिक बेईमानी का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि कोई लेखक तीन सौ पृष्ठों की पुस्तक किसी इतिहासकार पर लिखे और उसके इन महत्वपूर्ण पक्षों पर पूरी तरह सफेदा पोत दे। इसी मानसिकता के कारण हिटलर का एक नाम ’पुतैया’ भी था।
यह पुस्तक स्कूली पाठ्यक्रमों, शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों, मुस्लिमों, ईसाईयों और कम्युनिस्टों पर बढ़ते हमलों की एक कड़ी है। पहले इन्हें ध्वस्त करो और फिर इन पर कब्जा करो की रणनीति के तहत मार्क्सवादी इतिहास लेखन के सबसे बड़े आधार स्तंभ को निशाना बनाया गया है। ऐसे असभ्य और बर्बर हमले भविष्य में और तेज होंगे। इतिहास और संस्कृति को नष्ट करने की ये कोशिश इराक पर अमेरिकी बमबारी से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ही विनाशक आक्रामकता पर हॉब्सबाम ने कहा था – “मुझे लगता था कि आण्विक भौतिकी के विपरीत इतिहास कम से कम कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब मैं जानता हूँ कि ऐसा हो सकता है। हमारे अध्ययनों को उसी तरह बम के कारखानों में बदला जा सकता है, जिस तरह आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (आई.आर.ए.) ने रसायनिक फर्टिलाइजर को विस्फोटक में बदलना सीख लिया था।…… आम तौर पर हमें ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर जिम्मेदार होना होगा और खास तौर पर इतिहास के दुरूपयोग की आलोचना करनी होगी।”27
भगवान सिंह ने जिस फैसलाकुन अंदाज में कोसंबी पर लिखा है, उस तरह मैं यह फरमान जारी नहीं कर सकता कि कोसंबी को समझने के लिए इस पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पुस्तक को इसलिए पढ़ा जाना चाहिए ताकि हम समझ सकें किस तरह पुनरूत्थानवादी शक्तियाँ, कितनी आक्रामकता के साथ हमारे ज्ञान और चिंतन की समृद्ध विरासत को मटियामेट करने पर तुली है। कैसे घृणा की राजनीति, वैयक्तिक विद्वेष और फासिस्ट मनोवृत्ति एक लेखक की भाषा को शोहदों की भाषा के स्तर पर उतार देता है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे उसके व्यक्तित्व और चरित्र की हत्या की परियोजना में बदल दिया जाता है। कैसे अपनी आस्थाओं, विश्वासों और भ्रमों के सहारे तथ्यों को गल्प में ढालकर इतिहास को निरस्त कर दिया जाता है। हमें ऐसे संगठित और अब तो सत्तापोषित प्रयासों से डटकर, मुकाबला करते हुए मार्क्सवाद और मार्क्सवादी विरासत की रक्षा करनी होगी। इसी क्रम में हम इतिहास की भी रक्षा कर पायेंगे और कोसंबी के ऐतिहासिक कर्म की भी।
(कोसंबी: कल्पना से यथार्थ तक/भगवान सिंह/राजकमल पेपर बैक्स/ संस्करण-2014/मूल्य – 250रू.)
संदर्भ:
(1) एरिक हॉब्सबाम/‘इतिहासकार की चिंता‘/ग्रंथ शिल्पी/प्रथम हिन्दी संस्करण 2007 /पृ. – 21.
(2) भगवान सिंह/‘कोसंबीःकल्पना से यथार्थ तक‘/राजकमल पेपर बैक्स/प्रथम संस्करण – 2014/पृ. – 220.
(3) दामोदर धर्मानंद कोसंबी/‘प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता‘/राजकमल प्रकाशन/तीसरा संशोधित संस्करण 1990/पृ. – 21.
(4) कार्ल मार्क्स/रानीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा का एक प्रयास/ संकलित रचनाएँ/खण्ड – 1, भाग – 2, प्रगति प्रकाशन मास्को/संस्करण – 1978/ पृ.- 267.
(5) दामोदर धर्मानंद कोसंबी/‘प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता‘/वही.पृ – 23.
(6) भगवान सिंह/वही.,पृ. – 12.
(7) अर्नेस्ट गेलनर/स्रोत – एरिक हॉब्सबाम/‘इतिहासकार की चिंता‘/वही.पृ. – 50.
(8) एरिक हॉब्सबाम/वही.,पृ. – 203,204.
(9) दामोदर धर्मानंद कोसंबी/स्रोत – डी.एन. झा/ दामोदर धर्मानन्द कोसाम्बीः एक अद्भुत विद्वान/सहमत मुक्तनाद/अंक – 41/जुलाई – दिसम्बर 2009/ पृ. – 32.
(10) दामोदर धर्मानंद कोसंबी/‘प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता‘/वही.,पृ- 98.
(11) भगवान सिंह/वही.,पृ. – 244.
(12) भगवान सिंह/वही.,पृ. – 140,41.
(13) रोमिला थापर/‘आर्यःमिथक और यथार्थ‘/सहमत/1995/पृ. – 61.
(14) रामशरण शर्मा/ ‘आर्य संस्कृति की खोज‘/सारांश प्रकाशन/पहला संस्करण 1995/पृ. – 81,82.
(15) रामशरण शर्मा/वही., पृ. – 80.
(16) भगवान सिंह/‘हड़प्पा सभ्यता ओर वैदिक साहित्य‘/राधाकृष्ण प्रकाशन/ दूसरा संशोधित संस्करण – 2011/पृ. – 175.
(17) रोमिला थापर/वही., पृ. – 67.
(18) रामशरण शर्मा/वही., पृ. – 19.
(19) मार्क ब्लाख/इतिहासकार का शिल्प/ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन/प्रथम हिन्दी संस्करण 2005/ पृ. – 130.
(20) एरिक हॉब्सबाम/वही., पृ. – 22,23.
(21) भगवान सिंह/‘कोसंबीः कल्पना से यथार्थ तक‘/वही., पृ. – 100.
(22) भगवान सिंह/वही., पृ. – 17,18,19,20,24,37.
(23) भगवान सिंह/वही., पृ. – 64.
(24) दामोदर धर्मानंद कोसंबी/‘प्राचीन भारत की संस्कृति और सम्भ्यता‘/वही., पृ. – 19,20.
(25) भगवान सिंह/वही., पृ – 100.
(26) दामोदर धर्मानंद कोसंबी/वही., पृ. – 208.
(27) एरिक हॉब्सबाम/वही., पृ. – 21,22.
संपर्क: सियाराम शर्मा, 7/35, इस्पात नगर, रिसाली, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़), पिन कोड- 490006, मो0 – 9329511024, e-mail – prof.siyaramsharma@gmail.com
साभार- अकार