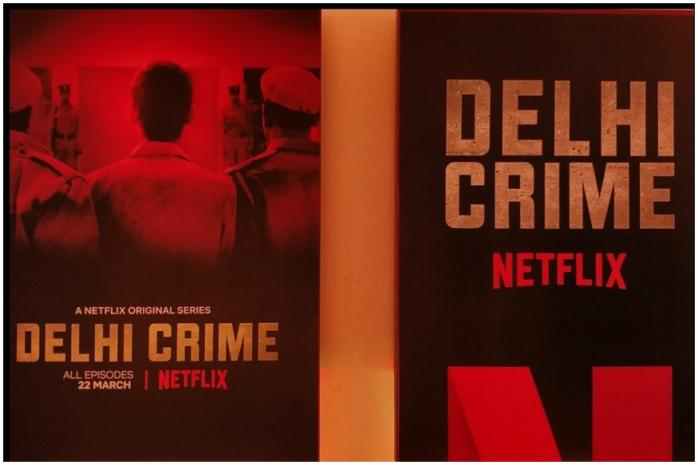साल 2012 में 16 दिसंबर को दिल्ली में हुई बर्बरता ने समूचे देश को झकझोर दिया था. कई हफ़्तों तक आंदोलन का माहौल रहा था तथा वारदात से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात देशभर की मीडिया और लोगों के मन में दर्ज हो रही थी. इस घटना को हुए ज़्यादा वक़्त भी नहीं बीता है. ऐसे में रिची मेहता की सिरिज़ ‘दिल्ली क्राइम’ को बहस के दायरे में आना ही था. यह सिरीज़ नेटफ़्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.
समीक्षाओं में दो बातें बार-बार आ रही हैं- एक, सिरीज़ में कई तथ्यों को नज़रअंदाज़ किया गया है या उन्हें तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, दूसरी, इसे पूरी तरह से पुलिस के नज़रिये से दिखाया गया है. मेरी राय में इन दोनों आलोचनाओं की पड़ताल ज़रूरी है, किंतु मेरा यह भी आग्रह है कि इसे एक अपराध कथा की तरह देखा जाये और इसके आधार पर फ़िल्म की समीक्षा हो.
कथानक में किये गये कुछ बदलाव बहुत मायने नहीं रखते हैं और उनसे कहानी पर असर नहीं पड़ता है. उदाहरण के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का पुरुष होना. कुछ दृश्य न सिर्फ़ बेमतलब हैं, बल्कि वे कहानी को ही कमज़ोर करते हैं. जैसे, अस्पताल में मौत से जूझ रही लड़की का महिला पुलिस अधिकारी से यह कहना कि उसे ख़ुशी है कि मामला उनके हाथ में है. चूंकि यह फ़िल्म दिल्ली पुलिस के नज़रिये से बनायी गयी है, इसलिए ऐसा दृश्य उसे कमज़ोर ही करता है. इस फ़िल्म को बनाने में तत्कालीन पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने निर्देशक रिची मेहता को बड़ी मदद की है और मामले से जुड़े अधिकारियों से संपर्क कराने के साथ दस्तावेज़ों को भी उन्हें उपलब्ध कराया है. इसमें कोई बड़ी आलोचना की बात नहीं है कि कहानी किसी एक नज़रिये से कही गयी है. दिक्कत तब होती है, जब फ़िल्म अपना यही तर्क कुछ जगहों पर छोड़ देती है. उदाहरण के रूप में, मुख्यमंत्री के बेटे के साथ किसी प्रभावशाली आदमी की बातचीत, जो पुलिस आयुक्त के पीछे पड़ा हुआ है. उस दौरान हुए कई प्रकरणों से परिचित होने के नाते यह मैं दावे से कह सकता हूं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त के बीच तनातनी का माहौल था. यह भी हुआ था कि इस तनाव का एक आयाम दोनों की क्षेत्रीय पहचान का अलग-अलग होना भी था. कुछ अन्य ग़लतियों में उच्च न्यायालय में दिल्ली पुलिस से जवाब-तलब के मामले का चित्रण है. ऐसा किसी स्वयंसेवी संस्था की याचिका पर नहीं हुआ था, अदालत ने ख़ुद ही मामले का संज्ञान लिया था और जांच के बारे में जानकारी मांगी थी.
पॉपुलर कल्चर और पब्लिक स्फेयर में अपराध कथाओं की एक ख़ास जगह है. इसमें पाठक या दर्शक सिर्फ़ भावनात्मक तौर पर ही प्रतिक्रिया नहीं देता है, बल्कि वह एक गवाह, खोजी और जज की भूमिका में भी होता है. भले ही कहानी किसी या कुछ किरदारों के नज़रिये से कही जा रही हो, पर उसे पढ़ने, सुनने और देखने वाला घटनाक्रम के पड़ताल की अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है. अपराध आधारित कहानियां भी उसकी इस भूमिका के लिए उसे उकसाती हैं, उसे चुनौती देती हैं. ऐसा अन्य तरह की कथाओं में भी हो सकता है, होता भी है, लेकिन अपराध कथा का रोमांच (थ्रिल) बिना पाठक या दर्शक की अपनी भागीदारी के पैदा ही नहीं हो सकता है. इसलिए हर एक गतिविधि पर नज़रें जमाना ज़रूरी होता है. अक्सर ऐसा होता है कि यदि आपसे किसी ऐसी कहानी का शुरुआती हिस्सा छूट गया, तो बाद का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है. ऐसी कथाओं का अंत बहुत अहम नहीं होता और वह अक्सर बहुत क्षणिक होता है. वह उत्तेजना पैदा करता है, पर पिछले लम्हों के रोमांच का ही नतीज़ा होता है. साहित्य एवं रंगमंच की तुलना में हालांकि फ़िल्मों और टेलीविज़न पर उनका चित्रण ज़्यादा असरदार होता है.
अब इसे ‘दिल्ली क्राइम’ की कमी कहें या फिर पुलिस के नज़रिये से कथा कहने में उसकी कामयाबी कि इस सिरिज़ में हमारे लिए दर्शक के रूप में सबसे सुरक्षित जगह थाना या डीसीपी का कक्ष हो जाता है. जब पुलिसवाले बाहर कहीं होते हैं, तो वो भी हमें सुरक्षित लगता है. लेकिन सीएम और सिविल सोसाइटी के साथ पुलिस कमिश्नर की बैठक हमारे भीतर विलगाव भरती है. वहां नेता और सिविल सोसायटी के लोग अपने नहीं लगते, बल्कि अपराध से जूझती हमारी अपनी पुलिस के ख़िलाफ़ खड़े हुए लगते हैं. जुलूस और प्रदर्शन किसी और समूह का है, हमारा नहीं. यहां तक कि डीसीपी की बेटी भी कोई अन्य ही लगती है.
यह कमाल है निर्देशक का. ख़ामियों के बावजूद वह न सिर्फ़ पुलिस के पक्ष से हमें मुतमईन कर देता है, बल्कि हमें पुलिस के भरोसे रहने का भाव भी भरता है. यहां पुलिस मानवीय तो है, पर वह पुलिस ही है. समाज की आलोचना और अपराधियों के अपराधी होने के विभिन्न कारण भी पुलिस के जरिये ही हम तक पहुंचते हैं. राजनीति, मीडिया, प्रदर्शनकारी की आलोचना भी पुलिस ही करती है. कोई और पक्ष है ही नहीं. मज़े की बात यह है कि यह सब हम स्वीकार करते जाते हैं. इस कोशिश में फ़िल्मकार ग़लतबयानी भी करता है. जिस बस में यह वारदात हुई थी, उसमें युवती और उसके दोस्त के सवार होने से पहले जो मिस्त्री चढ़ा था, उसका प्रकरण ठीक नहीं दिखाया गया है. उसे जब अपराधियों ने लूटने के बाद उतार दिया था, तो उसने मोबाइल चौकसी कर रहे पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना दी थी. उन्होंने उसकी मदद भी नहीं की और वारदात की जांच भी नहीं की. बाद में उन्हें निलंबित किया गया था. कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी हटाये गये थे. सिरिज़ में इसकी चर्चा नहीं है.
चूंकि मैं ख़ुद पहले दिन से प्रदर्शनों में था, तो यह दावे से कह सकता हूं कि प्रदर्शनकारियों से थाने पर, अस्पताल के बाहर और इंडिया गेट पर पुलिस के साथ लगातार संवाद होता रहता था. इस बात को सिरिज़ नहीं बताती है. ऊपर से एक दृश्य में एक जांच अधिकारी थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे एक युवक से पूछता है कि तुम्हारा इरादा क्या है. इस पर वह कहता है कि अपराधियों को हम मार देंगे. इसी तरह से अस्पताल के बाहर नारेबाज़ी के दृश्य भी सही नहीं हैं. वहां हमेशा मौन प्रदर्शन हुए थे.
बहरहाल, अपराध कथाओं की एक बड़ी ख़ासियत यह भी है कि वे हमारे समाज और शासन के ताने-बाने के छिन्न-भिन्न होते जाने की सूचना भी देती हैं, भले ही कथानक का ऐसा इरादा हो या नहीं. आम तौर पर ऐसी कथाएं भी मेलोड्रामा की संरचना में ही होती हैं और उनमें अच्छे-बुरे के बीच लकीर साफ़ खींची होती है. हमारी व्यवस्था में व्यक्ति के या व्यक्ति के समूहों के क्षत-विक्षत होने को ‘दिल्ली क्राइम’ भी रेखांकित करती है. वह पूंजीवादी तंत्र को भी अपराधी ठहराती है. भले ही फ़िल्म अंत में अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने में सफल हो जाती है, लेकिन किरदारों के भीतर एक बेचैनी होने का अहसास भी दिला जाती है. पूरी फ़िल्म में शीर्ष के अधिकारी कुछ ज़्यादा इत्मीनान से रहते हैं, जबकि निचले स्तर के लोग निजी और पेशेवर स्तर पर बहुत परेशान हैं. मुझे लगता है कि यह फ़िल्मकार की वजह से नहीं, अपराध कथा के चरित्र के कारण है.
बहरहाल, इन्हीं दिनों नेटफ़्लिक्स पर ही एक ऐसी ही अपराध फ़िल्म ‘हाइवेमेन’ स्ट्रीम हो रही है. उसमें भी एक डाकू और उसकी संगिनी का पीछा कर मारने की कहानी है. उसमें अपराधी बिल्कुल ही अनुपस्थित है और उसका हवाला पुलिस के जरिये ही मिलता है. ‘हाइवेमेन’ और ‘दिल्ली क्राइम’ में अपराधियों के लिए भी जगह होती, तो कहानी का दायरा व्यापक हो जाता. ऐसी कथाओं की जटिलता बरक़रार रखी जानी चाहिए, अन्यथा केरीकेचर बन जाने का ख़तरा रहता है. यही ‘हाइवेमेन’ और ‘दिल्ली क्राइम’के साथ हुआ है. ख़ैर, इन्हें एक दफ़ा तो देखा ही जाना चाहिए. कई बार सिनेमा पूरे कथानक में नहीं, दृश्यों में भी मिलता है.