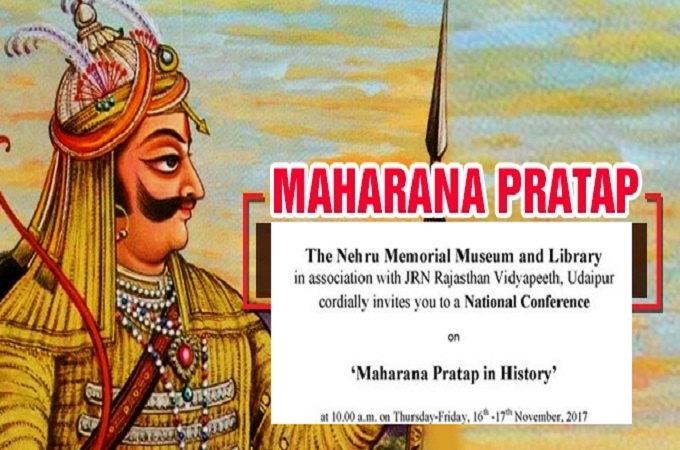पंकज श्रीवास्तव
इतिहास जड़ नहीं होता। नए तथ्यों के आधार पर इतिहास में सुधार की प्रक्रिया चलती ही रहती है। जिस दिन हड़प्पा संस्कृति की लिपि पढ़ने में क़ामयाबी मिल जाएगी, बहुत सी किताबों को नए सिरे से लिखना पड़ सकता है। आधुनिक इतिहास लेखन की यही प्रक्रिया है। किसी काल विशेष में उपलब्ध ज्ञान ही इतिहास का आधार होता है।
लेकिन जिस तरह से 1576 में हुई हल्दीघाटी के युदध में महाराणा प्रताप को ‘विजयी’ बताने की कोशिशें हो रही हैं, वह किसी नए ऐतिहासिक तथ्य के आलोक में न होकर राजनीतिक अभियान का हिस्सा हैं। इसके तहत राणा प्रताप को एक ‘हिंदू आयकन’ के रूप मे स्थापित करने पर ज़ोर है जो मौजूदा हिंदुत्ववादी राजनीति की मुस्लिम विरोधी राजनीति में काम आए। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक में इस मुहिम ने हाल में काफ़ी ज़ोर पकड़ा है जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं।
16 और 17 नवंबर दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी में जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर के सहयोग से ‘इतिहास में महाराणा प्रताप’ विषय पर दो दिन की राष्ट्रीय कान्फ्रेंस हुई। लेकिन इतिहासकारों के लिए यह कहना संभव नहीं हुआ कि राणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया था। अधिक से अधिक यही कहा जा सका कि हल्दीघाटी युद्ध से पलायन कर जाना राणा प्रताप की रणनीतिक कार्रवाई थी जैसा कि गुरिल्ला युद्ध में होता है।
इस पर बात करने से पहले आइए देखते हैं कि कवि नरोत्तम ने ‘मानचरित्र रासो’ में इस युद्ध के बारे में क्या लिखा है। हल्दीघाटी का युद्ध राणा प्रताप के सामने अकबर नहीं उनके सेनापति राजा मानसिंह थे।
कवि नरोत्तम लिखते हैं–
परिय लोथि तिहिं खेत नांउ तिनि कोउ न जानइ ।
इतहि उतहि बहु जोध क्रोध करि भीरहि भानइ ।।
राउत राजा राउ सूर चौडरा जि केउव ।
कहत न आवहि पारु औरु चंधरया ति तेउव ।।
भिरि स्वाँम काँम संग्राम महि, लगी लोह सब लाज जिहि
जीत्यौ जु माँन नीसाँन हनि, खस्यौ खेत परताप तिहि।।
अर्थात- “जंग इतना ख़ौफ़नाक थी कि लाशों पर लाशें गिरने लगीं, इतनी कि उनका नाम तक कोई नहीं जानता था ; दोनों तरफ़ के योद्धाओं ने ग़ुस्से में एक-दूसरे से लोहा लिया ; राजा, रावत, घुड़सवार की क्या गिनती करे, झंडे लेकर चलने वाले भी अपने मालिक की इज़्ज़त के लिए लड़े ; राजा मान सिंह डंके की चोट पर विजयी हुए और महाराणा प्रताप सिंह युद्ध क्षेत्र से खिसक गए। ”
कह सकते हैं कि कवि नरोत्तम मानसिंह के दरबारी थे। तारीफ़ तो करेंगे ही। लेकिन यदि राणा युद्ध ‘जीते’ तो फिर हुआ क्या ? उसके बाद हमारे पास राणा के घास की रोटी खाकर लड़ते रहने की कहानियाँ हैं, जो बस इतना बताती हैं कि राणा प्रताप किसी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे जैसा कि दूसरे राजपूत राजाओं ने किया था। लेकिन वे 1567 में हार चुके चित्तौड़ का क़िला जीत पाए, ऐसा नहीं हुआ। निश्चित ही वे अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहे जिसकी प्रशंसा ही की जा सकती है।
लेकिन 441 साल बाद राणा की हार को अपनी राजनीतिक जीत के लिए इस्तेमाल करने वाले राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। जबकि अकबर की ओर से सेनापति मानसिंह थे और राणा प्रताप के सिपहसालार का नाम हक़ीम खाँ सूर था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राणा प्रताप को समर्पित कर दिया था उनकी बहादुरी लोककथाओं में दर्ज है।
सच्चाई यह है कि इस लड़ाई का धर्म से कोई लेना-देना नहीं था। राणा प्रताप के कुछ बेहद निकट लोग भी अकबर के साथ थे। इसकी वजह मेवाड़ की गद्दी को लेकर चला विवाद था। दरअसल, राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने 18 शादियाँ की थीं जिससे उनके 24 बेटे और 20 बेटियाँ हुईं। प्रताप बड़े बेटे थे, लेकिन उदय सिहं अपने वारिस बतौर जगमल को राजगद्दी दे गए जो वारिसों में नवें नंबर पर थे। प्रताप सिंह के समर्थकों ने उदय सिंह की मृत्यु के बाद इसका विरोध किया और राणा प्रताप गद्दी पर बैठे। नाराज़ जगमल अकबर के साथ चला गया जिसे जहाजपुर का परगना मिल गया।
देखा जाए तो राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई केंद्रीय और स्थानीय सत्ता की लड़ाई थी, हिंदू-मुस्लिम की नही जैसा कि आज बताने की कोशिश हो रही है। अकबर राजपूतों को अपने साथ करके भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। जो साथ नहीं आए, उन्हें युद्ध में जीतना एकमात्र रास्ता था।
राणा प्रताप के बाद उनका बेटा अमर सिंह मुगल दरबार में पाँच हज़ारी मनसबदार हुआ। इसलिए यह कहना ग़लत है कि सिसौदिया हमेशा मुगलों से लड़ते ही रहे।
राणा प्रताप की महानता असंदिग्ध है,इसके लिए उन्हें 441 साल बाद किसी युद्ध मे किसी तरह ‘जितवाने’ की ज़रूरत नहीं है। हार कर भी प्रेरणा देने वाले नायकों से इतिहास भरा पड़ा है। एक प्रेरणा तो यही है कि राणा प्रताप हिंदू-मुस्लिम भेद नहीं रखते थे वरना उनके सर्वाधिक विश्वासपात्र सेनापति का नाम हक़ीम खाँ सूर न होता।
( इस लेख में कवि नरोत्तम सहित कई विवरणों के लिए वरिष्ठ पत्रकार शाज़ी ज़माँ के हाल में प्रकाशित उपन्यास ‘अकबर ‘को स्रोत बतौर इस्तेमाल किया गया है। उपन्यास में प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है। )